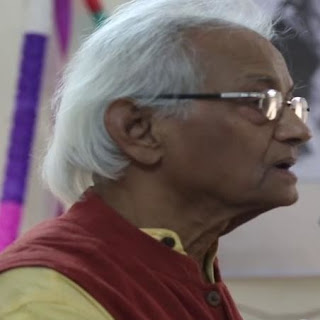हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हो गए हैं। साथी-संघाती खूब तालियां बजा रहे हैं..भूरि-भूरि प्रशंसाएं। कभी बैंकिंग सेक्टर छोड़कर पत्रकारिता में दाखिला, फिर सियासत की चाल-कुचाल उन्हे राजसत्ता के सिरहाने तक ले जा चुकी है। पत्रकार जब राजनेता हो जाए, वैसे ही तमाम बातें समझ में आ जाती हैं, फिर भी, कहा जाता है कि एमजे अकबर, अरुण शौरी आदि की तरह हरिवंश के लिए भी पत्रकारिता सेटिंग-गेटिंग का खेल रही है। एक वक्त में जब निर्मल बाबा के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहा था, हरिवंश दूसरे बाबाओं के महिमा गान पर अपने 'प्रभात खबर' अखबार में आधा-आधा पेज रंग रहे थे। ख्यात न्यायाधीश मार्कंडेय काट्जू ने जब बिहार में मीडिया पर नकेल कसने की बात कही तो 'प्रभात खबर' में संपादक हरिवंश ने पूरे दो पेज की काउंटर रिपोर्ट लिखी। लेख में नीतीश कुमार की भूरि-भूरि प्रशंसा थी और काट्जू की लानत-मलानत। 'प्रभात ख़बर' की मदर कंपनी ऊषा मार्टिन का नाम कोलगेट घोटाले में आने पर हरिवंश बार-बार तत्कालीन कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल से मिलने गए तो तरह-तरह के सवाल उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सपा नेता मुलायम सिंह यादव, बसपा लीडर मायावती जैसे राजनेता जिस भी पत्रकार नुमा प्राणी की भूरि-भूरि प्रशंसा करें, जान लीजिए कि 'दाल में काला' नहीं, पूरी दाल काली होगी! वैसे तो हमारे देश में बारहो मास और भी तमाम धुरंधर पत्रकार, साहित्यकार सियासी पद-पुरस्कारों की मलाई सोखने के लिए दर-दर लुलुआते रहते हैं।
Friday 10 August 2018
Wednesday 8 August 2018
हिंदी साहित्य में वीरबालकवाद / मनोहर श्याम जोशी
09 अगस्त जन्मदिन पर विशेष
वीरबालकवाद क्या होता है? यह प्रश्न आपके उर में विह्वलता भरने लगे उससे पहले यह समझ लें कि वीरबालकवाद वह होता है जो समझदार वीरबालकों द्वारा किया जाता है और समझदार वीरबालक वे होते हैं जो अपने को वीरगति को प्राप्त नहीं होने देते। अब पूछिए कि समझदार वीरबालकों द्वारा क्या किया जाता है? और समझ लीजिए अपने को जमाया और और दूसरों को उखाड़ा जाता है। और हाँ, हर बात का श्रेय स्वयं ले लिया जाता है। तो इस लेख के आरंभ में ही स्वयं वीरबालकवाद का अच्छा नमूना पेश करते हुए मैं 'वीरबालक' और 'वीरबालकवाद' दोनों फिकरे चलाने का श्रेय लेते हुए विषय-निरूपण के नाम पर संस्मरण सुनाऊँगा और आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि सभी वीरबालक विषय-निरूपण के नाम पर संस्मरण अवश्य सुनाते हैं क्योंकि आखिर ऐसा हो क्या हो सकता है जिससे वह व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए न रह हों?
तो साहब हुआ यह कि मैं जब साठ के दशक में मुंबई आया तब शुरू में अपने मित्र उमेश माथुर के यहाँ रहा। बंबइया इंडस्ट्री में किस्मत आजमाते हुए संघर्षरत लड़कों के लिए मैंने वीरबालक संबोधन प्रस्तावित किया और उमेश जी ने उसे अनुमोदित कर दिया। उन्हीं दिनों देवानंद के एक सहायक अमरजीत को जुहू में में टायर पंचर लगाते हुआ एक किशोर मिला जो बहैसियत लेखक बंबइया फिल्मों में किस्मत आजमाने अपने घर से भागकर आया था। उस वीरबालक को उमेश जी ने समझाया कि अभी तुम्हारी पढ़ने-लिखने की उम्र है इसलिए पहले पढ़ाई पूरी करो फिर बंबई आओ। उस वीरबालक की वापसी के लिए चंदा इकट्ठा करके हमने उसे बंबई से विदा किया। लगभग सात वर्ष बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक नौजवान पत्रकार मुझसे मिलने आया और उसे देखते ही मेरे मुँह से निकला, 'कहो वीरबालक तुम यहाँ कैसे?'
रामशरण जोशी जयपुर में अपनी पढ़ाई पूरी करके बहैसियत फिल्म-लेखक बंबई में किस्मत आजमाने आ गए थे। मैंने उस वीरबालक का स्वागत किया और उसकी सारगर्भित पत्रकारिता के कई नमूने छापे। शुरू में रामशरण जनसंघियों की न्यूज एजेंसी 'हिंदुस्तान समाचार' से जुड़े हुए थे। फिर वह एक नक्सलवादी के रूप में प्रकट हुए। उनकी बातचीत और पत्रकारिता से यह संकेत मिलने लगा कि संघर्ष है जहाँ, वीरबालक है वहाँ। इसके साथ ही नेताओं के बारे में उनकी व्यक्तिगत जानकारी में बड़ी तेजी से इजाफा होता चला गया। सत्ता-प्रतिष्ठान के पत्रों के लिए लिख तो पहले से ही रहे थे फिर वह उनमें से एक में अच्छे पद पर नियुक्ति भी पा गए। और इसके साथ ही उनका संघर्षरत क्रांतिकारी वाला स्वरूप ज्यादा जोर पकड़ने लगा।
तो फिर मैंने एक फिकरा गढ़ा - वीरबालकवाद। वीरबालकवादी का जीवन बगैर क्रांति की क्रांतिकारिता को, बगैर संघर्ष के संघर्ष को और बगैर जोखिम के जोखिम को समर्पित रहता है। कलम का सिपाही होने के नाते वह सारी लड़ाई शब्दों में लड़ता है अर्थात उसकी वीरता वाचा के आयाम तक सीमित रहती है। मनसा और कर्मणा वह सयाना बनता चला जाता है और जितना सयाना होता जाता है उतना ही बोलने और दिखने में वीरता को प्राप्त होता है। इसी के चलते आज हिंदी में सारी सत्ता वयोवृद्ध वीरबालकों के हाथ में है और उनकी छत्रछाया में तरुण वीरबालक तेजी से पनप रहे हैं। वह समझ गए हैं कि वाचा ही वीरबालक बनना चाहिए। और अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरे वीरबालकों का कद घटाना चाहिए। दस रीत को अपनाकर 'करियरिस्ट' और 'क्रांतिकारी' दोनों एक साथ हुआ जा सकता है।
अगर आप मनसा और कर्मणा भी वीरबालक बने रहें तो आप झगड़ालू, सिरफिरे औ सिनिकल समझ लिए जाएँगे। शैलेश मटियानी की तरह किसी भी गुट में फिट नहीं हो पाएँगे और सभी के हाथों पीटे जाएँगे। आपको अपने जीते जी किसी तरह की कोई मान्यता, पद-प्रतिष्ठा, पुरस्कार-पुरस्कार राशि और सुख सुविधा कभी नहीं मिल सकेगी। मरने के बाद मिलेगी इस भरोसे भी आप तभी मर सकेंगे जब आपको यह विश्वास हो कि दो-चार वीरबालकवादी आपकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कर-करके अतिरिक्त प्रतिष्ठा अर्जित करने को लालयित होंगे। मनसा और कर्मणा वीरता को आप जितना ही छोड़ते जाएँ उतनी ही 'वाचा' के स्तर पर अपनी वीरता को उद्घोष शुरू कर दें। ऐसा न करने पर आप अपनी नजरों में भी गिर जाएँगे, दूसरों की नजरों में तो खैर आप गिरे हुए होंगे ही।
कारण सच्चा वीरबालक उसे ही माना जाता है जो भौतिक सुखों को जूते की नोक पर रखने वाला ऋषि और लेनिन के पद-चिह्नों पर चलने वाला रिवोल्युशनरी दोनों हो। इस कसौटी पर खरा उतर सकने वाला साहित्यकार मिल सकना कहीं भी कठिन है और हमारे अर्द्धसामंती समाज में तो असंभवप्राय है। अपने इस इतने लंबे साहित्यिक जीवन में मैंने अब तक कुल एक ऐसा लेखक देखा है जो अच्छी खासी नौकरी छोड़कर नक्सलवादी बनने चला गया। वह था दिनमान में मेरे साथ काम कर चुका रामधनी। लेकिन अभी पिछले दिनों में कोई बात रहा था कि वह भी अब मुख्यधारा में शामिल हो गया है। अपने मित्र मुद्राराक्षस को छोड़ मैंने किसी और लेखक को नहीं देखा जिसने किसान या मजदूर मोर्चे पर काम किया हो। और तो और स्वतंत्र लेखन कर सकने और अपनी बात बेरोक-टोक कहने की खातिर नौकरी छोड़ने वाले पंकज बिष्ट जैसे लोग भी गिने-चुने ही मिल पाएँगे। लुत्फ ये है कि सभी वीरबालक अपने बायोडाटा में एक इंदराज संप्रति अवश्य रखते हैं। यथा - संप्रति - गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अध्यापनरत। मानो इससे पूर्व एवरेस्ट अभियान में रत थे और इसके बाद पेरू के जंगलों में छापामारों के कंधे से कंधा मिलाकर युद्धरत हो जाएँगे।
तो जहाँ सभी अपनी ही मान्यताओं के अनुसार छोंगी, कायर और पतित तीनों ही हों, वहाँ सारा खेल इस बात तक सीमित रह जाता है कि साहित्यिक राजनीति की आवश्यकता और अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए कब किसको कितना ज्यादा गिरा हुआ बताना है अथवा मन की बात मन में ही रखते हुए कब कितना उठा देना है? हर समझदार वीरबालक इस बात को समझता है कि अगर मैं कुछ दूसरों को गिरा कुछ दूसरों को उठा हुआ बताऊँगा तो कुछ नासमझ तीसरे मुझे इसलिए उठा हुआ मान लेंगे कि ऊँचाई पर बैठा हुआ इनसान ही इस तरह के प्रमाण पत्र बाँट सकता है, यही नहीं, जिन वीरबालकों को मैंने उठा हुआ बताया है वे सब मुझे हाथोंहाथ उठा लेंगे। कुछ नादान पाठक शंका कर सकते हैं कि क्या दूसरों को पतित बताने वाला वीरबालक यह जोखिम उठा रहा होता है कि वे पलटकर उस पर वार कर देंगे?
इन शंकालुओं को यह समझना चाहिए कि हर वीरबालक जहाँ तक हो सके हेड आफ डिपाट कटगरी के किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता जो पलटकर उसका कोई नुकसान कर सकता हो। अगर वह ऐसे व्यक्ति पर प्रहार करता भी है तो किसी अन्य हेड आफ डिपाट के आशीर्वाद और कृपादृष्टि आश्वासन ले लेने के बाद ही। रीडर और लेक्चरर कटगरी के वीरबालकों पर प्रहार करना निरापद ही नहीं, आवश्यक भी समझा गया है। नई पीढ़ी के वीरबालक पुरानी पीढ़ी के अब वयोवृद्ध हो चले ऐसे नामवर वीरबालकों पर निर्भय होकर प्रहार करने लगे हैं जिनके पास अब कोई खास सत्ता रह न गई हो। लेकिन पुरानी पीढ़ी के वीरबालक इतने सयाने हैं कि टाप पोजिशन पर रह चुके किसी अन्य वृद्ध वीरबालक पर तब तक वार नहीं करते जब तक उसकी तेरहवीं क्या, बरसी न हो गई हो।
कुछ पाठकों को शंका हो सकती है कि जब वो वाले 'सर' सत्तावान अथवा प्राणवान अथवा दोनों ही थे तब वीरबालकों ने जाकर उनसे यह नम्र निवदेन क्यों नहीं किया कि 'सर' अन्यथा न लें लेकिन हमारी समझ से आप रिएक्शनरी और डिकाडेंट दूनों हैं। वीरबालक रिवोल्युशनरी के साथ-साथ ऋषि भी होता है और ऋषियों को बड़ों का निरादर करना शोभा नहीं देता। अब शंकालु यह पूछ सकता है कि क्या ऋषियों को गाली-गलौज करना शोभा देता है? अरे ऋषियों को न देता हो रिवोल्युशनरियों को तो देता है ना। इस तरह की क्रांतिकारी कार्रवाई ही तो वीरबालक-बिरादरी के जाग्रतावस्था में पहुँची है वर्ना उसमें तो ऊँघते रहने की महामारी व्याप्त है। वीरबालकों की आँखें तभी खुलती हैं जब कान में गालियों की आवाज पड़े या काकटेल्स के लिए पुकार।
रीडर कटगरी के वीरबालकों के लिए यह भी निरापद समझा जाता है कि वह परोक्ष प्रहार करें अर्थात कोई ऐसी कहानी या कविता लिख दें जिसमें कुछ वीरबालक विशेष या एक वीरबालक विशेष नितांत घृणित किस्म का पात्र बना दिया गया/दिए गए हों। ऐसी हर रचना की बहुत चर्चा होती है और सभी वीरबालक उसके विषय में एक-दूसरे को फुनियाते हैं। इस तरह का प्रच्छन्न प्रहार इसलिए निरापद माना गया है कि जिस किसी पर प्रहार किया गया हो वह तो मानेगा ही नहीं कि इस रचना का निशाना मैं हूँ। स्वयं रचनाकार को भी यह सुविधा मिल जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने निशाने से कह दें कि सर आपके शत्रु इतने घृणित हैं कि मेरे और आपके संबंध बिगाड़ने के लिए कहते डोल रहे हैं कि अपनी रचना में मैंने उनका नहीं, आपका पर्दाफाश किया है।
समझदार वीरबालक एक समय में एक से ज्यादा हेड आफ डिपाट को नहीं जुतियाता। और उसे जुतियाने से पहले भी किसी अन्य हेड आफ डिपाट से वचन ले लेता है कि आप हमको एक जोड़ा नया जूता तो दिलवा दीजिएगा ना? सभी सरों के सिर पर ताबड़तोड़ जूते बरसाने में दो खतरे पेश आते हैं। पहला यह कि आप पागल समझ लिए जाएँगे। दूसरा यह कि आपका जूता टूट जाएगा और आप जानिए नंगे पाँव चलने वाले का वीरबालकों के साहित्य में भले ही अनन्य स्थान हो, वीरबालकों की बिरादरी में वे नगण्य समझे जाते हैं। उनके बारे में यह तक नहीं माना जाता कि वे वे मकबूल फिदा हुसैन मार्का बेहतरीन स्टंटबाज हैं। सीरियस वीरबालक बिरादरी में स्टंटबाजी नहीं चलती तो सुजान वीरबालक किसी सर के सिर पर जूता तभी बरसाता है जब किन्हीं अन्य सर की वरद हथेली उसके अपने सिर पर टिकी हुई हो। ज्ञातव्य है कि हिंदी में जूनियर वीरबालक डाक्साब और सीनियर वीरबालक सर कहकर संबोधित किए जाते हैं। जौत्यकर्म के विषय में विधान यह है कि इसे दो अवस्थाओं में ही अधिक करना उचित है। या तो तब जब आप करियर बनाने के लिए हाथ-पाँव मार रहे हों या फिर जब आप हेड आफ डिपाट बन चुके हों। करियर की तलाश में लगभग घिस चुका फटा-पुराना जूता धड़ाधड़ प्रतिष्ठितों के सिर पर बरसाएँगे तभी वयोवृद्ध वीरबालकों की नोटिस में आएँगे। उनमें से हर हेड आफ डिपाट ललचाएगा कि क्यों नहीं इस बलिष्ठ-बाहु को फैलोशिप दिलवाकर पटा लूँ कि यह मेरे दिए जूते से मेरे प्रतिद्वंद्वियों को तसल्लीबख्श ढंग से गंजा करता रहे। फैलोशिप मिल जाने के कुछ ही समय बाद गुरुजनों की संगत में तरुण वीरबालक को यह बात समझ में आती है कि राजनीति की तरह साहित्य में भी स्थायी दोस्त दुश्मन-जैसी कोई चीज नहीं होती। शत्रुता का एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण मैच चलता रहता है। सौदेबाजी चलती रहती है और समीकरण बदलते रहते हैं। इसलिए आपसी गाली-गलौज को बहुत सिर-यसली में नहीं टेक किया जाता।
सच तो यह है कि जौत्यकर्म को मनोरंजक रूप से उत्तेजक और उत्तेजक रूप से मनोरंजक विधा का दर्जा दिया जाता है। 70 के दशक से उस मुक्तमंडी का वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ जिसकी संस्कृति ओर राजनीति दोनों में ही इस तरह के उत्तेजक-मनोरंजक जौत्यकर्म का अच्छा भाव लगता है। मुझे याद है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना के अवसर पर साहू जैनों द्वारा आयोजित महासम्मेलन में बहैसियत तरुण वीरबालक मैं थोड़ा गरजा-बरसा और मेरे बाद श्रीकांत ने तो उसी हैसियत से सत्ता-प्रतिष्ठान और उससे जुड़े साहित्यकारों पर इतना जोरदार प्रहार किया कि बोलते हुए उसकी कमजोर काया अपने दुस्साहस पर स्वयं ही काँपती रही। वह तब हैरान हो गया जब बाद में श्रीमती रमा जैन ने उसे बुलवाया और बहुत प्यार से समझाया कि जोश बहुत अच्छी चीज है लेकिन थोड़ा संयम भी जरूरी होता है। कुछ ही समय बाद श्रीकांत भी मेरे साथ साहू जैनों के दिनमान में काम करता नजर आया।
अगर मैं भूला नहीं होऊँ तो लगभग उन्हीं दिनों पेरिस में पी.ई.एन. के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए अमरीकी नाटककार आर्थर मिलर ने ने इस विडंबना की ओर ध्यान दिलाया था कि लोकतंत्र वाले देशों में सत्ता प्रतिष्ठान को मुँह बिराते संस्कृतकर्मी अब जेलों में नहीं, भव्य दफ्तरों में कैद किए जा रहे हैं। उनकी हैसियत खतरनाक क्रांतिकारियों की नहीं, मनोरंजक उछल-कूद करने वाले बंदरों की रह गई है इसलिए वे जितना ही ज्यादा गाली-गलौच करते हैं उन्हें उतना ही ज्यादा प्यार से गले लगाया जाता है। उन्हें अपनाकर सत्ता प्रतिष्ठान अपनी छवि सुधार लेता है और साथ ही स्वयं उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान का ही एक हिस्सा बना देता है। कृपया ध्यान दें कि मिलर ने यह बात विचारधारा की समाप्ति और मुक्तमंडी की विश्वविजय के मौजूदा दौर से कई दशक पहले कही थी।
आज तो पूँजीवादी मीडिया हर कहीं वामपंथी वीरबालकों को वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर सर्वहारा की पैरवी और मुक्तमंडी की भर्त्सना करने के लिए तगड़ा वेतन और हर तरह की सुख-सुविधा दे रहा है। लोकतंत्र और मुक्तमंडी के अंतर्गत स्वयं राजनीति भी कुल मिलाकर वीरबालकवादी हो चली है इसलिए आज भारत जैसे असामंती देश तक यह संभव है कि आप किसी सेठ की या सरकार की नौकरी करते हुए भी अपने को सत्ता-प्रतिष्ठान-विरोधी क्रांतिकारी मान और मनवा सकें। कभी कम्युनिस्ट होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, आज विचारधारा की समाप्ति के बाद यह आलम है कि पूँजीपति मीडिया में काम करने वाले पत्रकार और आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारी भी अपने को कम्युनिस्ट बता रहे हैं। बहरहाल वीरबालक बिरादरी सेठाश्रय और राजाश्रय का मुक्तकंठ से विरोध करती पाई जाती है उसमें एक-दूसरे पर सेठाश्रय या राजाश्रय लेने का आरोप लगाने का रिवाज है।
हर समझदार वीरबालक यह जानता है कि प्रतिरक्षा का श्रेष्ठ उपाय प्रहार है। इसीलिए वह 'जो पहले मारे सो मीर' के सिद्धांत पर पूरी आस्था रखता है। पहले हमला करने वाला अपने पर जवाबी हमला करने वाले को लचर सफाई देने वाला ठहराते हुए पूछ सकता है कि अगर आपको मैं पतित और प्रतिक्रियावादी लग रहा था तो आप अब तक चुप्पी काहे साधे थे? इस पर सफाई देने वाला यदि अतिरिक्त सफाई देते हुए यह कहे कि मैं तो शालीनतावश चुप था तो कोई बात बनती नहीं। कारण, वीरबालक बिरादरी में 'शालीनता' की तो होती है लेकिन शालीनता की नहीं। शालीनता अर्थात अपनी समस्त प्रगतिशीलता के बावजूद सरस्वती-वंदना सुनने और शंख-ध्वनि के बीच शाल, श्रीफल, प्रतिमा और चेक लेने की स्वीकृति। मैं बराबर इस प्रतीक्षा में रहा हूँ कि कोई वीरबालक 'शालीनता' पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक आपत्ति उठाएगा। व्यावहारिक यह कि जब हम न शाल ओढ़ते हैं और न हमें नारियल गिरी की बर्फी पसंद है तब आप शाल-श्रीफल ही क्यों दिए चले जाते हैं? सूट लेंथ और स्काच नहीं दे सकते क्या? सैद्धांतिक यह कि हम क्रांतिकारियों को इस तरह की भारतीयता अर्थात प्रतिक्रियावाद से जुड़ी चीजें क्यों दी और सुनाई जा रही हैं।
यहाँ उल्लेखनीय है कि वीरबालक बिरादरी के लिए 'भारतीयता' खासी गड़बड़ सी चीज रही है। किसी के पतित ठहरा देने का अचूक तरीका वीरबालकों में यही माना जाता रहा है कि उसे पुरातनपंथियों या हिंदुत्ववादियों से जोड़ दिया जाए। जब से भाजपा भी सत्ता की भागीदारी होने लगी है तब से वीरबालकों के लिए उससे जुड़ने का लालच और उससे जोड़ दिए जाने का खतरा दोनों ही बहुत बढ़ गए हैं। एक संस्मरण ठोकने की अनुमति चाहता हूँ। मुझे व्यंग्य लेखन के लिए पुरस्कार दिया जाना था। आयोजकों ने कहा कि अपनी पसंद का कोई वक्ता बता दीजिए। मैंने ऐसे अधेड़ वीरबालक का नाम सुझाया जिसकी रचनाएँ मैं बहुत पसंद करता हूँ। आयोजन से हफ्ता भर पहले उसका मेरे पास फोन आया कि जोशी जी मैं दो रात से सो नहीं सका हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ?
मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, पूछा, 'क्या हुआ भाई?' पता चला कि पुरस्कार देने अटल जी आ रहे हैं। और उनके वयोवृद्ध बालकों ने कहा है कि संघ परिवार से जुड़े पी.एम. के साथ मंच शेयर करना ठीक नहीं रहेगा। मैंने उनसे न यह पूछा कि सी.पी.एम. के नेता संघियों के साथ क्यों पर्लियामेंट शेयर कर रहे हैं और न यह कि वयोवृद्ध वीरबालक संघीय पी.एम. की सरकार द्यारा गठित समितियों और आयोजित गोष्ठियों में क्यों चले जा रहे हैं? मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि परेशान क्यों होते हो मना कर दो। इस पर उसने राहत और हैरानी दोनों एक साथ व्यक्त की। वीरबालकवादियों के लिए सही मंत्रों का जाप करना और राजनीतिक छुआछूत बरतना बहुत आवश्यक माना गया है। इसके अभाव में आपकी वीरता संदिग्ध हो जाएगी क्योंकि वीरता दिखाने के लिए कोई और अवसर न प्रस्तुत हुआ है और मुक्तमंडी ने चाहा तो आगे भी प्रस्तुत नहीं होगा। परम प्रसन्नता का विषय है कि स्वाधीनता के बाद से अब तक हिंदी भाषी प्रदेश में कुल एक बार ऐसा अवसर आया जब वीरता के प्रदर्शन से कष्ट में पड़ने का कोई खतरा पैदा हो सकता था।
वह था आपातकाल। लेकिन उसके दौरान वीरबालकों ने कोई खास वीरता प्रदर्शित की नहीं। शायद इसलिए कि वे जेल नहीं जाना चाहते थे या शायद इसलिए कि वे इंदिरा गांधी को वामपंथी समझते थे। खैर जो हो, उसके वर्षों बाद कुछ वीरबालक आपातकाल के संदर्भ में भी वीरता और कायरता के प्रमाण पत्र बाँटते रहे। मेरी कायरता असंदिग्ध है क्योंकि मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी। लेकिन यह भी असंदिग्ध है कि उस दौर में वीरबालक बिरादरी में कुर्सी छोड़ देने की कोई प्रतियोगिता नहीं चली हुई थी। मेरे मित्र साहित्यकारों में केवल कमलेश ही ऐसे थे जो इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ कर दिखाने के लिए निकले थे। प्रसंगवश बाद में कमलेश वीरबालक बिरादरी के लिए समर्थ कवि और प्रकांड विद्वान से ज्यादा इस रूप में सांय स्मरणीय हुए कि समर्थ मेजबान हैं। मेरे दोस्तों में कुल निर्मल वर्मा ने ही 'जोशी हाउ कैन यू...' वाली शैली में लताड़ते हुए तब कायर संपादक कहा था। औरों को तो यह इलहाम इंदिरा गांधी के हार बल्कि मर जाने के बाद हुआ।
वीरबालक कुर्सी छोड़ना नहीं, कुर्सी पाना चाहते हैं। औसत वीरबालक ने ज्यादा नहीं तो इतना समझने लायक मार्क्सवाद तो पढ़ ही रखा होता है कि हम एक अर्द्धसामंती समाज में जी रहे हैं जिसमें कलम से कहीं ज्यादा महिमा कुर्सी की है। रुतबा, रौब, रुपया, कुर्सी पर बैठने के बाद ही मिलता है। कुर्सी ही जमाने और उखाड़ने के लिए अधिकार दिलाती है, जो भक्तों को आकर्षित शत्रुओं को आतंकित करती है। वीरबालक भयंकर रूप से सत्ता-ग्रंथि का मारा हुआ होता है क्योंकि हिंदीभाषी क्षेत्र में साहित्य और साहित्यकार की अपनी अलग से कोई सत्ता बची ही नहीं है। मुझे अपने दोस्त श्रीकांत का एक सवाल याद आता है जो उसने मुझसे एक दिन दिनमान कार्यालय में पूछा था, यह बताओ जोशी कि ज्यादा पावर किस में होती है - पोस्ट में कि पालिटिशियन में? अगर मैं अपने कसबे बिलासपुर में पावरफुल पोस्ट होकर लौटूँ तो मुझे ज्यादा सम्मान मिलेगा कि पावरफुल मिनिस्टर बनकर लौटने में?
श्रीकांत मिनिस्टर तो नहीं बाद में एम.पी. जरूर बन गया और खुद यह देख सका कि जहाँ तक वीरबालकों का सवाल है उनके लिए संसद की सत्ता साहित्यकार की सत्ता से कहीं ज्यादा बड़ी है। श्रीकांत एक बढ़िया कवि के रूप में हमेशा याद किया जाएगा लेकिन उस दौर में वह पी एम के निकट होने और बड़ी दरियादिली से स्काच पिलाने के लिए याद किया जाता था। उसे भाव-विह्वल श्रद्धांजलि देते हुए एक वीरबालक ने कहा था, 'अब श्रीकांत जैसा स्काच पिलाने वाला कहाँ मिलेगा।' खैर तो वीरबालक एक-दूसरे पर प्रहार करते हुए यह मानकर चलते हैं कि राजनेता सर्वशक्तिशाली हैं और कुर्सियाँ उनकी कृपा से ही मिलती हैं और जब हमसे छिनती हैं तो राजनेताओं के कोप के कारण ही। बिरादरी में किसी को घटिया साबित करने का सबसे बढ़िया उपाय यह समझा जाता है कि उसे राजनेता की चापलूसी करके कुर्सी पाने और बचाने वाला सिद्ध कर दिया जाए।
अब जैसा रामशरण जोशी ने मुझे आपातकाल में कायरता दिखाने का प्रमाण पत्र देने के साथ-साथ यह भी बताया है कि इंदिरा गांधी के हार जाने के बाद अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए मैंने अटल जी की कुंडलियाँ छापनी शुरू कर दीं। सफाई देना इसलिए व्यर्थ नहीं है कि किस्सा खासा दिलचस्प है। हुआ यह कि जेल से अटल जी ने एक कुंडली संपादक के नाम पत्र के रूप में भेजी जिसमें मारीशस में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन पर कटाक्ष किया गया था। पत्र जेल-सेंसर से पास हो कर आया था इसलिए मैंने छाप दिया लेकिन इसके छापे जाने पर सूचना मंत्रालय के सेंसर ने मुझे फटकार सुनाई। फिर विदेशमंत्री बन जाने के बाद अटल जी ने अपने कुछ गीत प्रकाशनार्थ भेजे जिन्हें मैंने तुरंत नहीं छापा। इस पर उन्होंने संपादक पर व्यंग्य करते हुए एक कुंडली भेजी। फिर मैंने उनके गीत छापे और उनकी भेजी कुंडली और जवाबी संपादकीय कुंडली भी साथ ही साथ छाप दिए। संपादकीय कुंडली में कहा गया था कि मंत्री पद पा जाने पर कवि हो जाना सहज संभाव्य है।
मुझे सचमुच बहुत अफसोस है कि मुझे अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे घटिया काम करने पड़े। जहाँ तक रामशरण जोशी का सवाल है मेरे लिए यह अपार संतोष का विषय है कि उन्हें अपने नक्सलवादी विचारों के कारण माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कार्यकारी निर्देशक का पद मिल गया है और इसे पाने या बचाने के लिए उन्हें कभी किसी कांग्रेसी सी.एम.,पी.एम. की चाटुकारिता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। खैर शत्रुतापूर्ण मैत्री और मैत्रीपूर्ण शत्रुता में विश्वास करने वाले वीरबालकों में एक-दूसरे के बारे में झूठ बोल देने से परहेज उतना ही कम किया जाता है जितना कि अपने बारे में सच्चाई स्वीकार करने से। दूसरों के बारे में कहीं से कोई गड़ा मुर्दा उखाड़कर ले आया जाता है तो अपने बारे में यह तक भुला दिया जाता है कि अभी कल ही हम कहीं और क्या कह अथवा कर चुके हैं। अरे परिपक्वता आने के साथ-साथ आदमी का विचार बदलता है कि नहीं? कुछ वयोवृद्ध वीरबालक तो इस मामले में इतने भुलक्कड़ हैं कि एक ही गोष्ठी में बोलते-बोलते परिपक्व हुए चले जाते हैं। वीरबालक बिरादरी में कुर्सी इसलिए भी बहुत जरूरी समझी जाती है कि यद्यपि हर वीरबालक अपने को कलम का मजदूर कहता है तथापि वह लिखकर पैसा कमाने को कलम बेच देने का पर्याय मानता है। इसलिए कभी वीरबालकों को पत्रकारिता से भी परहेज था। अब उससे तो नहीं लेकिन फिल्म और टीवी के लिए लिखने से है। खैर पत्रकार या लेखक के रूप में मीडिया से जुड़ने वाला हर वीरबालक यह कहते रहने जरूरी समझता है कि मैंने अपनी कलम बेची नहीं है और सरकार या सेठ से किसी तरह का समझौता नहीं किया है। पूँजीपतियों से जोड़े जाने के कलंक से बचने के लिए कुछ सयाने वीरबालकों ने किसी ऐसे छोटे-मोटे सेठ को पकड़ लेने की युक्ति अपनाई है जो साहित्य का मारा हुआ हो और बुद्धिजीवियों की सोहबत करा देने की एवज में सारे खर्चे-पानी का जुगाड़ खुशी-खुशी कर देता हो।
जो वीरबालक बड़े सेठों के लिए काम करते हैं वे इस बात को छिपा जाते हैं कि मालिक को नौकर की वैचारिक क्रांतिकारिता से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो केवल जी-हजूरी और हितरक्षा चाहता है। जब तक आप विज्ञापन से आय बढ़वाते और सत्तावान लोगों से संबंध सुधरवाते रहेंगे तब तक सेठ आपको सांस्कृतिक पृष्ठों पर कुछ भी लिखने-छापने की पूरी छूट देता रहेगा। दूसरे वीरबालक आपकी शिकायत करें तो वह अनसुनी कर देगा। जी हाँ, सेठ से यह शिकायत की जाती थी कि आपका संपादक कम्युनिस्ट है और पश्चिमी रंग में रंगा हुआ है। अब यह शिकायत की जाती है कि आपका संपादक पोंगापंथी हिंदी वाला है जो भूमंडलीकरण के तकाजों से अनजान है।
कभी मेरे द्वारा साप्ताहिक हिंदुस्तान कि आवरण पर कांगड़ा-शैली के श्री राधा जी के चित्र के बारे में कृष्ण कुमार जी से यह शिकायत की गई कि पश्चिमी रंग में रंगे कम्युनिस्ट संपादक ने राधा का नग्न चित्र छापकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। कृष्ण कुमार जी ने मुझे बुलाकर कहा था, कांगड़ा शैली का है वह तो मैं समझ गया लेकिन भई देखो अपन ऐसे फोटो निकालें ही क्यों की लोग नाराज होवें और सर्कुलेशन घटे। मैं समझता हूँ कि अब नई पीढ़ी के सेठ भी नई पीढ़ी के संपादक जी को बुलाकर कुछ यों कहते होंगे, पोर्नोग्राफी के लिए कौन कह रहा है भई लेकिन अपने प्रोडक्ट की अपमार्केट इमेज तो बनानी ही चाहिए। हिंग्लिश यूज करके और लुगाइयों के सेमीन्यूड फोटो निकालकर। नहीं तो अपनी तो एड-रेवेन्यु निल रह जाएगी। जिसे पुराना सेठ अपसंस्कृति की जननी समझता था उसे नया सेठ अपमार्केट की मदर बताता है।
किसी छोटे या बड़े नेता, किसी छोटे या बड़े सेठ की कृपा से किसी गद्दी पर आसीन साहित्यिक सामंत वीरबालक का जलवा देखना हो तो उसके साथ कभी दौरे पर निकलिए। जहाँ जाइएगा स्टेशन या हवाईअड्डे पर स्थानिक वीरबालकों की सलामी गारद अटेंशन में पाइएगा। उसका स्थानिक मन-सबदार उसे हार पहनाएगा और वेरी इंपोर्टेंट वयोवृद्ध वीरबालक वी.आई.वी.वी. की चरण रज अपने माथे लगाएगा। फिर अपने यहाँ के सबसे बड़े नेता, सेठ या अधिकारी की कार में वी.आई.वी.वी. को अपने यहाँ के सबसे बढ़िया होटल या सरकारी विश्राम गृह में ले जाइएगा जहाँ कार-दाता एक और सलामी-गारद, एक और हार के साथ प्रस्तुत होगा। सलामी की रस्म पूरी हो जाने के बाद कारदात अपना स्काचदाता रूप दिखाते हुए एक बोतल सेवा में प्रस्तुत करेगा। जो सभा होगी उसमें वी.आई.वी.वी. अपनी वीरता और शत्रुओं की कायरता का बखान करके स्थानीय वीरबालकों की दाद पाएगा और स्थानीक साहित्यकारों के वीरबालकवादी तेवरों पर स्वयं दाद देगा। साहित्य चर्चा अंतर्गत इतना ही होगा कि स्थानिक वीरबालक वी.आई.वी.वी. को अपनी कोई पुस्तक थमाते जाएँगे कि सर पढ़कर दो शब्द लिखने की कृपा करें। सर प्रोत्साहन के दो शब्द वहीं बगैर पढ़े कह डालेंगे और दिनभर में मिली कई किलो रद्दी स्थानिक मनसबदार के लिए छोड़ आएँगे।
वी.आई.वी.वी. तरुण वीरबालकों को यह नेक सीख दे जाता है कि अच्छा साहित्यकार होने के लिए अच्छा वीरबालक होना जरूरी है, कुछ अच्छा पढ़ना या लिखना नहीं। जहाँ तक हो सके लिखो ही मत। लिखो तो अच्छा मत लिखो क्योंकि रूपवादी समझ लिए जाओगे। और देखो तुम्हें लिखने के जिद ही हो तो ऐसी छोटी-मोटी कविताएँ लिखो जिनकी तारीफ में मित्र आलोचक जितना भी कहें वो कम हो लेकिन जिनके बारे में इतना कहना ही काफी हो कि याद न रखी जा सकने के मामले में ये सर्वथा यादगार है। ऐसी कविताएँ लिखने में समय कम लगता है और संग्रह जल्दी तैयार हो जाता है। संग्रह पढ़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। उपन्यास लिखोगे तो सभी वीरबालक लोकार्पण गोष्ठी में बिना पढ़े ही पहुँच जाएँगे। लेकिन दि बेस्ट तो यह है कि कुछ भी मत लिखो। बस विवादस्पद वक्तव्य, साक्षात्कार देते रहो। इस बात को समझो कि वीरबालकों के साहित्य-दरबार में राजा इंद्र का रोल ऐसे रिवोल्युशनरी ऋषि को ही नसीब हो पाता है जो आसार-संसार में आकंठ लिप्त होते हुए भी साहित्य संसार में संन्यास ले चुका हो। अब लगे हाथों कुछ बातें वीरबालकवाद के ऋषि पक्ष के संदर्भ में भी कर ली जाए। साहित्यिक हाजमा ठीक रखने के लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम की डोज नियमित रूप से पीने और पिलाने वाले हमारे वीरबालकों का ऐसा विश्वास है कि ऋषिगण सुरा-सुंदरी और राजदरबार में मिलने वाले मान-सम्मान तीनों से सख्त दूरी बरतते आए हैं। सांसारिक भोग-विलास से यह परहेज ही उन्हें समाज की आँखों में राजा से ऊँचा स्थान दिलाता आया था। अब सुरा का ऐसा है कि उसका आविष्कार हुआ ही इस लिए की कतिपय कविमन किस्म के प्राणियों ने पाया कि नशे के अभाव में सही सुर लग नहीं पाता है। और सुंदरी का ऐसा है कि मानव जाति ने लँगोट का ईजाद किया ही तब जब आमराय यह बनी कि जो मर्द बच्चा सो लँगोट कच्चा।
प्राचीन ऋषियों के बारे में मेरी जानकारी नहीं के बराबर है इसलिए मैं पंडित वागीश शुक्ल से पूछकर ही आपको बता सकूँगा कि वे सुरा और सुंदरी से कितना परहेज बरतते थे। संभव है तब भी न बता पाऊँ क्योंकि प्राचीन भारत के बारे में किसी तरह की गड़बड़ बात बोलना निरापद नहीं है। दो नवीन ऋषियों उर्फ वीरबालकों में से ज्यादातर सुरा-सुंदरी त्याग नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो इस संदर्भ में सारा वीरबालकत्व यह सिद्ध करने में है कि मैं पीता भी हूँ तो अपने पैसे की जबकि दूसरे मुफ्त की पीते हैं? जी हाँ, और अगर कौनो जन बहुत पीछे पड़ जाए तो हमहु पी लेते हैं। इस संदर्भ में वयोवृद्ध वीरबालकों के बारे में तरुण वीरबालक दिलचस्प जानकारियाँ देते रहे हैं मुझे। जैसे यह कि उनमें से एक सुरा-प्रेमियों को दर्शन देने बहुधा आ जाते हैं लेकिन मधुशाला को उनसे एक कानी कौड़ी भी लेने का आज तक कष्ट नहीं उठाना पड़ा है। कलम का कोई भी मजदूर शराब पीने में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बरबाद नहीं कर सकता, अपना जिगर भले कर दे।
जहाँ तक सुंदरियों का संबंध है कदाचित इतना ही कह देना पर्याप्त हो कि साहित्यकार होने के नाते वीरबालक में आरंभ से ही उत्कट सौंदर्यबोध रहता है और आयु के साथ-साथ उक्त सौंदर्यबोध तीव्रतर होता चला जाता है। स्वाभाविक है कि जो सुंदरियाँ युवा वीरबालक को माताएँ-बहनें लगती रहीं थीं वे वृद्धावस्था में बेटियाँ प्रतीत होने लगती हैं। पूर्णाहुत से ठीक पहले या ठीक बाद के क्षण में। नितांत प्रीतिकर रूप से पारिवारिक यह सौंदर्यप्रियता वीरबालकों के ऋषिपद की सुरक्षा करती रहती हैं। अब ऐसा है कि वीरबालक ऋषि के साथ-साथ क्रांतिकारी भी होते हैं और क्रांतिकारी आप जानिए आधुनिक भी होता है और आधुनिकता के मारे आप जानिए कि जैनेंद्र जी जैसे गांधीवादी लेखक तक को पत्नी के साथ-साथ प्रेमिका भी आवश्यक प्रतीत होने लगी थी। तो वीरबालक को क्रांतिकारी रूप में एक ठो प्रेमिका भी अपेक्षित रहती है। बल्कि दो ठो क्योंकि अज्ञेय नदी के द्वीप में अपने साथ रेखा और गौरा दूनों को ले गए थे और सौंदर्यबोध के क्षेत्र में अज्ञेय ही क्रांतिकारियों के आदर्श हैं। वीरबालकवादी साहित्यकार अपने आसपास से जुड़ा रहता है इसलिए जोड़ीदार प्रेमिका को भी आस-पास से ही प्राप्त करना चाहता है। इसके चलते साहित्य-साधिका को ही प्रेमिका बनाने की परिपाटी चली आ रही है। आज वीरबालकवादी डींगें वीरबालकवादी ढोंग के अनुपात में ही इतनी बढ़ चली हैं कि अब हर साहित्य-साधिका किसी न किसी वीरबालक को प्रेमिका ठहराई जा रही है। प्रतिपक्ष के वीरबालक हर सफल साहित्य-साधिका के विषय में यहाँ तक कहते सुने जाते हैं कि वह स्वयं नहीं लिखती, भले घर की औरतों को बिगाड़ने वाला अमुक लंपट वीरबालक उसके लिए लिख दिया करता है। यह शंका करना अपनी मूर्खता का परिचय देना होगा कि अगर वह लंपट-लँगोट-लुच्चा इतना अच्छा लिख सकता है तो अपने नाम से ही क्यों नहीं लिख लेता?
वीरबालक अपनी प्रेमिका का इस अर्थ में भी संरक्षक होता है कि वह उस पर दूसरों की बुरी नजर नहीं पड़ने देता। एक साहित्य-सभा के बाद चाय-पान के दौरान मैं अपना परिपक्व सौंदर्याबोध एक नवोदिता पर आजमाने लगा तो एक वयोवृद्ध वीरबालक विशेष मुझे बाँह पकड़कर एकांत में ले गए और उन्होंने फुसफुसाकर मुझसे कहा कि अइसा है ये बहुत ही संभ्रांत घर की महिला हैं और इनसे हमारा पारिवारिक सा संबंध रहा है। आप इनसे कुछ इस टाइप... आप समझ रहे हैं ना? अब इतना नासमझ तो बंधुवर मैं भी नहीं हूँ। इधर कुछ अन्य वीरबालक जो कोई ओर क्रांतिकारी चीज लिखने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, अपनी प्रेम-लीलाओं का सार्वजनिक स्वीकार करके अपनी वीरता का प्रमाण दे रहे हैं। सिद्ध कर रहे हैं कि भले ही वे अपने आराध्य पश्चिमी लेखकों जैसा कुछ रच न सके हों प्रेमिकाएँ अपनाने-छोड़ने के मामले में उनसे कभी पीछे नहीं रहे हैं।
ऋषि-ग्रंथि के अंतर्गत वीरबालक बिरादरी में राजाश्रय और सेठाश्रय दोनों बड़ी घटिया किस्म की चीजें मानी जाती है। इसीलिए वीरबालक अपने लिए एक ठो स्टैंडर्ड बायोग्राफी गढ़ चुका होता है। मामूली हैसियकत वाले परिवार में जन्म, संघर्षरत माता अथवा पिता अथवा दोनों से प्रेरणा प्राप्त, निर्दय समाज से निर्भीक टक्कर, प्रलोभन ठुकरा क्रांति पथ पर अग्रसर, सीकरी को ठेंगा दिखाने के दंड-स्वरूप मान-सम्मान से वंचित, तिकड़मबाजों द्वारा उपेक्षित किंतु आश्वस्त कि हिस्ट्री बोलेगी ही वाज सिंपली ग्रेट बट हिस्ट्री की डिफिकल्टी यह है कि वह ससुरी मरणोपरांत शुरू होगी। तो वीरबालक दारू से महकती एक आह भरकर कहता है अपने से और अपनों से कि 'अइसे तो हम निराला, मुक्तिबोध की तरह अनचीन्हे मर जावेंगे' इसलिए नौकरी-वौकरी करनी पड़ जाती है और अपना स्थान बानने के लिए भी संघर्षरत रहना पड़ता है।
बता ही चुका हूँ कि वीरबालक-बिरादरी में यह माना जाता है कि दूसरों को नौकरी भ्रष्ट विचारधारा और उत्कृष्ट चमचागीरी के कारण मिली है। इसमें इतना और जोड़ना आवश्यक है कि इस बिरादरी में अगर किसी की कुर्सी जाती है तो वह यही कहता है कि मुझे अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण प्रतिक्रियावादी प्रतिष्ठान ने पद से हटाया। खैर इतना निर्विवाद है कि वीरबालक नौकरी सरकार की कर रहे हों या सेठ की वे सच्चे सेवक क्रांति के ही होते हैं। जैसा कि सरकारी नौकरी वाले एक नवोदित वीरबालक ने भरी सभा में मुझे 'सिनिसिज्म' के लिए लताड़ते हुए घोषणा की थी, जैसे तुलसी ने राम की चपरास गले में डाल ली थी वैसे हमने क्रांति की चपरास गले में डाल ली है। गोया वीरबालक राज हो या सेठ के दिए कपड़े भले ही पहन ले नीचे क्रांति की कोई जनेऊनुमा चपरास बराबर डाले रहते हैं कि नौकरी जाते ही कपड़े उतार के उसे दिखा दें।
राजाश्रय या सेठाश्रय की अनिवार्यता से तिलमिलाते वीरबालक फिर एक क्रांतिकारी स्थापना यह करते हैं कि हमें साहित्य में सेठों और नेताओं की घुसपैठ स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अस्तु, न सरकारों और सेठों के दिए पुरस्कार ग्रहण किए जाएँ और न ऐसे किसी साहित्यिक आयोजन में सम्मिलित हुआ जाए जिसमें किसी मंत्री या सेठ को बुलाया जा रहा हो। लेकिन इसमें भी कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे यह कि नेता न आए तो टी.वी. कवरेज नहीं होता, और तमाम जिस चीज का टी.वी. में कवरेज न हुआ हो वह न हुई मान ली जाती है। पुरस्कारों का ऐसा है कि सरकारों या सेठों द्वारा ही दिए जाते हैं। उन्हें ग्रहण न किया जाए तो बेटी की शादी से लेकर फ्लैट की खरीद तक कई काम अटके रह जाते हैं और कायदे का बायोडाटा भी नहीं बन पाता। 'अस्तु, लेने ही पड़ जाते हैं बंधु।' और फिर आप यह भी तो समझिए ना कि अगर कौनो बड़का मंत्री या कैपिटलिस्टुआ हमको सम्मानित करे के बदे आता है तब हमारा अस्टेटस उससे हाई ही न कहा जाएगा?
इसके बाद ले-देकर यह बचता है कि साधारण साहित्यिक आयोजन में नेता या सेठ न बुलाए जाएँ। महमूर्ख किस्म के लोग ही यह शंका कर सकते हैं कि जब वीरबालकों को नेताओं के दरबार में स्वयं हाजिरी लगाते कोई आपत्ति नहीं होती तब साहित्य के दरबार में उनकी उपस्थित से इतना कष्ट क्यों होता है। हमारे वीरबालक सिद्धांतवादी है। इसलिए उनके तमाम विरोध सैद्धांतिक स्तर पर ही होते आए हैं, व्यावहारिक स्तर पर नहीं। सुनता हूँ कि एक वीरबालक ने अपने घनिष्ठ मित्र और संरक्षक छोटा सेठ से कहा, 'भाई मेरे बुरा मत मानियो सिद्धांत का मामला है आज मैं भरी सभा में तेरा जौत्य-कर्म करूँगा।' इस पर छोटा सेठ ने कहा, 'कर लियो भई लेकिन मीटिंग के बाद मंत्री जी से मेरा सौदा जरूर करवा दीयो।' इस तरह के तमाम दिलचस्प किस्से मुझे नवोदित वीरबालकों के मुँह से सुनने को मिलते रहते हैं क्योंकि अब मैं वीरबालक बिरादरी में स्वयं ज्यादा चलायमान नहीं रह गया हूँ।
तरुण वीरबालकों के कई किस्से सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और यही प्रमाणित होता है कि हमारे नेताओं की तरह साहित्यिक मठाधीशों ने भी ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें सब एक-दूसरे को और जाहिर है कि अपने को भी चोर मान रहे हैं। तरुण वीरबालक अधेड़ और वयोवृद्ध वीरबालकों की अनैतिकता, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के किस्से सुनाते जाते हैं और बेसब्री से मुझ वयोवृद्ध वीरबालक की किसी टिप्पणी की प्रतिक्षा करते हैं कि जाके संबद्ध व्यक्ति को सुना आएँ। मैं अपनी जबान को भरसक लगाम देता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि चुप रहने से भी वीरबालक बिरादरी में कोई बात बनती नहीं है क्योंकि आपके मुँह से निकला कोई-न-कोई उद्गार सुविधानुसार गढ़ लिया जा सकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि तरुण वीरबालक आकर कभी कोई साहित्यिक चर्चा नहीं करते। उनकी सारी बातचीत साहित्यिकार चर्चा को समर्पित रहती है। वह यही बताना चाहते हैं कि किसको जमाने-उखाड़ने के सिलसिले में वयोवृद्ध वीरबालकों में क्या सौदेबाजी हुई है।
उनके अनुसार कभी-कभी ये सौदे साहित्य के दायरे तक सीमित होते हैं जैसे यह कि वीरबालक 'ए' ने वीरबालक 'बी'' के लेखन की पहली बार निंदा की जगह प्रशंसा इसलिए की है कि वीरबालक बी ने वीरबालक 'ए' के विवादास्पद वक्तव्य के समर्थन में कुछ लिख दिया है। लेकिन अकसर ये सौदे अहो रूपम अहो ध्वनि के दायरे से बाहर होते हैं। प्रशंसा की कीमत कैश या कांइड में वसूल की जाती है। तरुण वीरबालक आते हैं और आश्चर्य करते हैं कि सर क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अलाँ ने फलाँ को अपने खर्चे से विदेश यात्रा कराई है। अलाँ को तो फलाँ ने अपनी मिस्ट्रेस बना लिया है। अलाँ ने फलाँ के लिए उसकी कृति के विदेश अनुवाद किए जाने का या उसे विदेश में कोई फेलोशिप मिल जाने का जुगाड़ करवा दिया है। यह विदेश वाली बात तरुण वीरबालकों की चर्चा में अक्सर आ जाती है।
वीरबालकवाद के विदेश पक्ष का ऐसा है कि जहाँ ऋषि होने के नाते वीरबालक पश्चिम विरोधी होता है वहाँ क्रांतिकारी होने के होने के नाते वह आधुनिकता और मार्क्सवाद दानों का पक्षधर भी होता है और ये दोनों ही चीजें आप जानिए पश्चिमी ही हैं। इसलिए उसका आग्रह रहता है कि जिस हद तक मैं जीवन और लेखन में आधुनिक हुआ हूँ उस हद तक ठीक है लेकिन उसमें ज्यादातर पश्चिम के रंग में रंग जाना बहुत बुरा है। मेरे पाँव देश की माटी में मजबूती से जमे हुए हैं और मेरी जड़ें गाँव में गहरी गई हुई हैं। इसलिए मैं पश्चिमी-प्रदूषण की चपेट में आ ही नहीं सकता। लेकिन साथ ही वीरबालक को यह बोध भी रहता है कि मुझे गरीब, गँवई और आउट आफ डेट समझ लिए जाने का खतरा है इसीलिए वह सीकरी से कोई काम न रखते हुए भी सीकरी में अपने लिए एक ठो फ्लैट बनवा लेता है क्योंकि गाँव वाला घर तो वह फूँककर निकला होता है। सीकरी में प्रतीकात्मक माटी से सने हाथ वह ओडि क्लोन से धुलाने और प्रतीकात्मक पत्थर तोड़ते हुए सूखे कंठ को स्काच से तर करने की तथा बीच-बीच में फारेन कंट्रीज में हिंदी का झंडा गाड़ आने की व्यवस्था करता है।
वीरबालकों की इस विदेश ग्रंथि का जनक अज्ञेय जी को माना जा सकता है जिनके अभिजात्य से लोग-बाग उतने ही आक्रांत थे जितने कि उनके विदेश में प्रवास करते रहने से। मुझे लगता है कि जो लोग यह कहते सुने जाते थे कि अज्ञेय सी.आई.ए. के पैसे से विदेश जाकर नोबेल पुरस्कार के जुगाड़ में लगे रहते हैं, वे साथ ही इस बात के लिए भी ललक रहे थे कि हमारा भी कोई अंतरराष्ट्रीय चक्कर चले और हमारा भी दूसरों पर उतना ही रौब गालिब हो जितना कि अज्ञेय का हम पर हो रहा है। यही वजह है कि वीरबालक अपने साहित्यिक व्यायाम के लिए अंतरराष्ट्रीय आयाम तलाशते रहते हैं और अपनी हर उपलब्धि की सूचना अन्य वीरबालकों तक किसी न किसी तरह पहुँचाते रहते हैं ताकि जलने वाले जला करें।
तो हिंदी साहित्य में स्त्री-विमर्श पर बोलते हुए आप किसी वी.आई.वी.वी. को यह बोलते हुए सुन सकते हैं, 'अभी मेरे पूर्व वक्ता आयोवा की अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का जिक्र कर रहे थे, अमरीका के ही एक अन्य राज्य वरमोंट में उससे भी बड़ा आयोजन होता है जिसमें साहित्यकारों समेत चंद चुने हुए रचना-धर्मी व्यक्ति शांत, सुनम्य वन-प्रदेश में बनी कोटेजेज में साल-छह महीने रहने और विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। पिछले साल मुझे भी वहाँ बुलाया गया था जहाँ मेरी भेंट एस्ट्रोनिया की प्रसिद्ध कवयित्री जालीमा योन्यारी से हुई जो आजकल मेरी कविताओं का अपनी भाषा में अनुवाद कर रही हैं। तो जालिमा की छोटी सी कविता की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसमें सारा स्त्री-विमर्श समा गया है - स्त्री अहा, आ स्त्री आ स्त्री बला, जा स्त्री जा, स्त्री हाय-हाय, हाय स्त्री।' इस पर तालियाँ बजती हैं क्योंकि वीरबालक की कविता में अब इतना भी उक्ति चमत्कार दुर्लभ हो चला है।
तो सभी वीरबालक विदेशों में कहीं-न-कहीं बुलाए जा रहे हैं और वहाँ कोई न कोई उनकी रचनाओं का अपनी भाषा में अनुवाद भी कर रहा है। थोड़ी सी दिक्कत है तो यही कि विदेशों में हिंदी लेखकों की साहित्यिक उपस्थिति कहीं दर्ज हो नहीं रही है जबकि अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को वहाँ तगड़ी रायल्टी और कलमतोड़ दाद मिल रही है। इसे चलते सहसा वीरबालकों का पश्चिम विरोध और अंग्रेजी विरोध भड़क उठता है। एक गोष्ठी में मैंने एक वी.आई.वी.वी. को यह सिद्ध करते हुए सुना कि अंग्रेजी में लिखने वाल सारे भारतीय लेखक चालू किस्म का लेखन करने वाली शोभा डे के भाई-बंद ही हैं। उन्होंने सारे उदाहरण शोभा डे के लेखन से ही दिए। वीरबालकवादियों के पश्चिम-विरोध का एक पक्ष यह भी है कि वे एक-दूसरे को पश्चिम की नकल करने वाला ठहराते रहते हैं। तो वीरबालक आधुनिक तो होता है लेकिन पश्चिम का पिछलग्गू नहीं। कृपया उसके पश्चिम के पिछलग्गू न होने का यह अर्थ भी न लगाया जाए कि वह पोंगापंथी होता है और साहित्य के संदर्भ में भारतीयता की बात करता है।
तो वयोवृद्ध वीरबालकों की कृपा से तरुण वीरबालकों की एक ऐसी पीढ़ी पनप रही है जो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों से समान रूप से कटी हुई है और जो पांडित्य और इंटेलेक्टचुअलता दोनों की विरोधी है। वह हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएँ पढ़ लेना ही पर्याप्त समझती है और इन पत्रिकाओं में भी सबसे ज्यादा ध्यान से वी.आई.वी.वी. के वक्तव्य और गोष्ठी-समाचार पढ़ती है। अधिकतर वीरबालक अब अपने को जनवादी कहते हैं लेकिन उमें से अधिकतर के शास्त्रार्थ से कहीं यह संकेत नहीं मिलता कि उन्होंने मार्क्सवादी-लेनिनवादी शास्त्रों का बाकायदा कभी अध्ययन किया है। बल्कि स्थिति यह है कि मार्क्सवादी-लेनिनवादी पोथे बाँचे हुए लोग अब वी.आई.वी.वी. को थोड़े हास्यास्पद प्रतीत होने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि कात्यायनी बहुत अच्छी कवयित्री होने के साथ-साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद की गहन समझ रखने वाली विदुषी भी हैं। इसलिए मेरे आश्चर्य का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने एक वी.आई.वी.वी. बहुल निर्णायक समिति में उनका नाम किसी पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया और पाया कि अनुमोदन करने के लिए कोई तैयार नहीं है।
वीरबालकवाद पर अपने इस वीरबालकवादी लेख की समाप्ति में एक काल्पनिक वीरबालक के बारे में एक ऐसे काल्पनिक संस्मरण से करना चाहता हूँ जो वास्तविकता के काफी निकट है और जो इस ओर इशारा करता है कि वीरबालकवादी तेवर हमें किन ऊँचाइयों की आरे ले जा रहे हैं। किसी कस्बे के हिंदी विभागाध्यक्ष ने 'अस्तित्ववाद' पर संगोष्ठी की अध्यक्षता के लिए ऐसे संपादक वीरबालक को आमंत्रित किया जिसने स्वर्गीय सार्त्र और लगभग स्वर्गीय अस्तित्ववाद का नाम नहीं सुना था लेकिन जो अपनी पत्रिका में हर उस गोष्ठी का वृतांत सचित्र छापता था जिसकी उससे अध्यक्षता कराई गई हो। अब पूछिए कि अस्तित्ववाद से अनजान वह वीरबालक अध्यक्ष पद पर विराजमान होकर क्या करता है?
वह ऊँघता है। सभी वीरबालक व्यस्तातिव्यस्त किस्म के व्यक्ति होते हैं और अध्यक्षताओं के सिलसिले में बादल आवारा को मात करते हैं। उन्हें सोने और साँस लेने की फर्सत तक अध्यक्ष पर विराजमान होने के बाद ही मिलती है। ऊँघने को वीरबालकों के संसार में ध्यान से सुनने का पर्याय ठहराया जाता है। और हर वीरबालक ऊँघते-ऊँघते भी बीच-बीच में दो-चार फिकरे सुन ही लेता है ताकि अगर विरोधी खेमे का कोई वीरबालक उसके सो जाने पर चुटकी ले तो फौरन डेढ़ आँख खोले और कहे, 'अरे आप कहते न रहिए महाराज, हम ध्यान से सुन रहे हैं और जल्दी से मेन पांइट पर आइए नहीं तो हम सचमुच सो जावेंगे। खैर तो जब हमारे वीरबालक अध्यक्ष की बोलने की बारी आती है तब वह ऊँघते-ऊँघते सुनी हुई बातों के आधार पर अपने को वीरबालक सिद्ध करने वाली कुछ बातें कहकर तालियाँ बजवा ही लेता है।'
यथा, हमें यह बहुत गड़बड़ लगता है कि हिंदी के आधुनिक लेखक पश्चिम के बड़े लेखकों की नकल मारकर अपने को बड़ा कहलवाना चाहते हैं। उससे भी ज्यादा गड़बड़ बात यह है कि नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी टाइप हमारे मार्डन मठाधीश इन नकली लोगों की पीठ ठोंकते रहते हैं। देखिए हमें भी बहुत लालच दिया गया कि मार्डन बनने के लिए एक्जस्टेन्सवाद अपनाओ। बट हमने कह दिया नो। आप पूछेंगे नो क्यों कहा? हमने तो इसलिए किया कि हम जानते हैं कि जो भी एक्जिस्टेन्सवाद है, वह भारतीयों के मार्डन नहीं एन्सिएंट है। भगवान बुद्ध हमारे यहाँ बहुत पहले कह चुके थे। फ्रांस के सारतरे ने उनके आइडिया की नकल मारकर अपने को बड़ा भारी राइटर और फिलासफर साबित करने की कोशिश की है। इस मरे सारतरे का रौब भारत भवन वाले खाते हों, हम जेनुइन भारतीय नहीं खाते क्योंकि हम प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं।
इस पर देशभक्ति और हिंदीभक्ति में लीन रहने वाले लोग इतनी तालियाँ बजाते हैं कि गदगदायमान वीरबालक को सहसा याद आता है कि संपादक की हैसियत से पिछली गर्मियों में मुझे पेरिस-प्रवास करने का सुख भी मिला था। अस्तु वह अब दूसरी ताली-तलब बात भी कह डालता है, पिछली गर्मियों में पेरिस विश्वविद्यालय ने हमें एक सेमिनार पर प्रिसाइड करने के लिए बुलाया था। वहाँ अंग्रेजी में लिखने वाले कुछ इंडियन राइटर्स भी थे। लंच ब्रेक में हमने देखा कि वे सब के सब हमें अकेला छोड़कर किसी अभी-अभी पहुँचे आदमी से बात करने के लिए चले गए हैं। तो हमने अपनी फ्रांसिसी मेजबान को बुलाया और उनसे फ्रेंच में कहा, 'हलो एक्सक्यूज मी', हू दैट मैन देयर?' मेजबान फ्रेंच में बोली, 'अरे दै! ही इज तो अपना सारतरे। सुनते ही हमने फैसला किया कि इसको यहीं सबके सामने खरी-खरी सुनाएँगे ताकि इसे पता चल जाए कि हिंदी राइटर इंडियन इंग्लिश राइटर्स की तरह पश्चिम का थूका हुआ चाटने वाला चाटुकार नहीं है।
इस पर तालियाँ बजती हैं वीरबालक अपनी विनम्रता और दुस्साहस दोनों का परिचय देते हुए बताता है, तो हम अपनी प्लेट लेकर सरतरे के पास पहुँचे। पहले सोच रहे थे कि उससे फ्रेंच बोलें लेकिन एक तो हमारी फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं है कि उसमें गूढ़ साहित्यिक चर्चा कर सकें। दूसरे हम चाहते थो कि अदर इंडियन राइटर्स भी हमारी बात समझ सकें। तो हमने सारतरे से कहा, 'हलो एक्स्क्यूज मी, आई आल्सो इंडियन राइटर बट मैं आपका रौब नहीं खाता। बल्कि पोजीशन यह है कि अब आप यहाँ आ गए हैं तो मैं खाना भी नहीं खाऊँगा। इसका रीजन यह है कि आपने सारा सहित्य उल्टी करने की इच्छा पर लिखा है। इसलिए आपको देखते ही मुझे उल्टियाँ आने लगी हैं। हम इंडियन्स हैं और हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता है इसलिए मैं आपसे बहुत आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि आपको बुद्ध से चुरायी हुई एक्जिस्टेन्सवाद की फिलासफी सैकेंड हैंड है और आपका लिटरेचर थर्ड रेट। थैंक्यु एंड गुड बाई। इतना कहकर हम वाकआउट कर गए।'
हमारा वीरबालक तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से उतरता है और जिस स्थानिक कवियित्री के वह दो मुक्तक छाप चुका होता है वह भाव-विभोर होकर उसकी ओर बढ़ती है। एक मुसरचंद-मार्का मूर्खबालक हमारे वीरबालक के आगे वह शंका रखने की धृष्टता करता है, लेकिन सर सार्त्र तो बहुत पहले ही मर चुके थे। वीरबालक बहुत आश्वासन के साथ कहता है, हाँ, मारे शर्म के।
वीरबालकवाद क्या होता है? यह प्रश्न आपके उर में विह्वलता भरने लगे उससे पहले यह समझ लें कि वीरबालकवाद वह होता है जो समझदार वीरबालकों द्वारा किया जाता है और समझदार वीरबालक वे होते हैं जो अपने को वीरगति को प्राप्त नहीं होने देते। अब पूछिए कि समझदार वीरबालकों द्वारा क्या किया जाता है? और समझ लीजिए अपने को जमाया और और दूसरों को उखाड़ा जाता है। और हाँ, हर बात का श्रेय स्वयं ले लिया जाता है। तो इस लेख के आरंभ में ही स्वयं वीरबालकवाद का अच्छा नमूना पेश करते हुए मैं 'वीरबालक' और 'वीरबालकवाद' दोनों फिकरे चलाने का श्रेय लेते हुए विषय-निरूपण के नाम पर संस्मरण सुनाऊँगा और आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि सभी वीरबालक विषय-निरूपण के नाम पर संस्मरण अवश्य सुनाते हैं क्योंकि आखिर ऐसा हो क्या हो सकता है जिससे वह व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए न रह हों?
तो साहब हुआ यह कि मैं जब साठ के दशक में मुंबई आया तब शुरू में अपने मित्र उमेश माथुर के यहाँ रहा। बंबइया इंडस्ट्री में किस्मत आजमाते हुए संघर्षरत लड़कों के लिए मैंने वीरबालक संबोधन प्रस्तावित किया और उमेश जी ने उसे अनुमोदित कर दिया। उन्हीं दिनों देवानंद के एक सहायक अमरजीत को जुहू में में टायर पंचर लगाते हुआ एक किशोर मिला जो बहैसियत लेखक बंबइया फिल्मों में किस्मत आजमाने अपने घर से भागकर आया था। उस वीरबालक को उमेश जी ने समझाया कि अभी तुम्हारी पढ़ने-लिखने की उम्र है इसलिए पहले पढ़ाई पूरी करो फिर बंबई आओ। उस वीरबालक की वापसी के लिए चंदा इकट्ठा करके हमने उसे बंबई से विदा किया। लगभग सात वर्ष बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक नौजवान पत्रकार मुझसे मिलने आया और उसे देखते ही मेरे मुँह से निकला, 'कहो वीरबालक तुम यहाँ कैसे?'
रामशरण जोशी जयपुर में अपनी पढ़ाई पूरी करके बहैसियत फिल्म-लेखक बंबई में किस्मत आजमाने आ गए थे। मैंने उस वीरबालक का स्वागत किया और उसकी सारगर्भित पत्रकारिता के कई नमूने छापे। शुरू में रामशरण जनसंघियों की न्यूज एजेंसी 'हिंदुस्तान समाचार' से जुड़े हुए थे। फिर वह एक नक्सलवादी के रूप में प्रकट हुए। उनकी बातचीत और पत्रकारिता से यह संकेत मिलने लगा कि संघर्ष है जहाँ, वीरबालक है वहाँ। इसके साथ ही नेताओं के बारे में उनकी व्यक्तिगत जानकारी में बड़ी तेजी से इजाफा होता चला गया। सत्ता-प्रतिष्ठान के पत्रों के लिए लिख तो पहले से ही रहे थे फिर वह उनमें से एक में अच्छे पद पर नियुक्ति भी पा गए। और इसके साथ ही उनका संघर्षरत क्रांतिकारी वाला स्वरूप ज्यादा जोर पकड़ने लगा।
तो फिर मैंने एक फिकरा गढ़ा - वीरबालकवाद। वीरबालकवादी का जीवन बगैर क्रांति की क्रांतिकारिता को, बगैर संघर्ष के संघर्ष को और बगैर जोखिम के जोखिम को समर्पित रहता है। कलम का सिपाही होने के नाते वह सारी लड़ाई शब्दों में लड़ता है अर्थात उसकी वीरता वाचा के आयाम तक सीमित रहती है। मनसा और कर्मणा वह सयाना बनता चला जाता है और जितना सयाना होता जाता है उतना ही बोलने और दिखने में वीरता को प्राप्त होता है। इसी के चलते आज हिंदी में सारी सत्ता वयोवृद्ध वीरबालकों के हाथ में है और उनकी छत्रछाया में तरुण वीरबालक तेजी से पनप रहे हैं। वह समझ गए हैं कि वाचा ही वीरबालक बनना चाहिए। और अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरे वीरबालकों का कद घटाना चाहिए। दस रीत को अपनाकर 'करियरिस्ट' और 'क्रांतिकारी' दोनों एक साथ हुआ जा सकता है।
अगर आप मनसा और कर्मणा भी वीरबालक बने रहें तो आप झगड़ालू, सिरफिरे औ सिनिकल समझ लिए जाएँगे। शैलेश मटियानी की तरह किसी भी गुट में फिट नहीं हो पाएँगे और सभी के हाथों पीटे जाएँगे। आपको अपने जीते जी किसी तरह की कोई मान्यता, पद-प्रतिष्ठा, पुरस्कार-पुरस्कार राशि और सुख सुविधा कभी नहीं मिल सकेगी। मरने के बाद मिलेगी इस भरोसे भी आप तभी मर सकेंगे जब आपको यह विश्वास हो कि दो-चार वीरबालकवादी आपकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कर-करके अतिरिक्त प्रतिष्ठा अर्जित करने को लालयित होंगे। मनसा और कर्मणा वीरता को आप जितना ही छोड़ते जाएँ उतनी ही 'वाचा' के स्तर पर अपनी वीरता को उद्घोष शुरू कर दें। ऐसा न करने पर आप अपनी नजरों में भी गिर जाएँगे, दूसरों की नजरों में तो खैर आप गिरे हुए होंगे ही।
कारण सच्चा वीरबालक उसे ही माना जाता है जो भौतिक सुखों को जूते की नोक पर रखने वाला ऋषि और लेनिन के पद-चिह्नों पर चलने वाला रिवोल्युशनरी दोनों हो। इस कसौटी पर खरा उतर सकने वाला साहित्यकार मिल सकना कहीं भी कठिन है और हमारे अर्द्धसामंती समाज में तो असंभवप्राय है। अपने इस इतने लंबे साहित्यिक जीवन में मैंने अब तक कुल एक ऐसा लेखक देखा है जो अच्छी खासी नौकरी छोड़कर नक्सलवादी बनने चला गया। वह था दिनमान में मेरे साथ काम कर चुका रामधनी। लेकिन अभी पिछले दिनों में कोई बात रहा था कि वह भी अब मुख्यधारा में शामिल हो गया है। अपने मित्र मुद्राराक्षस को छोड़ मैंने किसी और लेखक को नहीं देखा जिसने किसान या मजदूर मोर्चे पर काम किया हो। और तो और स्वतंत्र लेखन कर सकने और अपनी बात बेरोक-टोक कहने की खातिर नौकरी छोड़ने वाले पंकज बिष्ट जैसे लोग भी गिने-चुने ही मिल पाएँगे। लुत्फ ये है कि सभी वीरबालक अपने बायोडाटा में एक इंदराज संप्रति अवश्य रखते हैं। यथा - संप्रति - गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अध्यापनरत। मानो इससे पूर्व एवरेस्ट अभियान में रत थे और इसके बाद पेरू के जंगलों में छापामारों के कंधे से कंधा मिलाकर युद्धरत हो जाएँगे।
तो जहाँ सभी अपनी ही मान्यताओं के अनुसार छोंगी, कायर और पतित तीनों ही हों, वहाँ सारा खेल इस बात तक सीमित रह जाता है कि साहित्यिक राजनीति की आवश्यकता और अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए कब किसको कितना ज्यादा गिरा हुआ बताना है अथवा मन की बात मन में ही रखते हुए कब कितना उठा देना है? हर समझदार वीरबालक इस बात को समझता है कि अगर मैं कुछ दूसरों को गिरा कुछ दूसरों को उठा हुआ बताऊँगा तो कुछ नासमझ तीसरे मुझे इसलिए उठा हुआ मान लेंगे कि ऊँचाई पर बैठा हुआ इनसान ही इस तरह के प्रमाण पत्र बाँट सकता है, यही नहीं, जिन वीरबालकों को मैंने उठा हुआ बताया है वे सब मुझे हाथोंहाथ उठा लेंगे। कुछ नादान पाठक शंका कर सकते हैं कि क्या दूसरों को पतित बताने वाला वीरबालक यह जोखिम उठा रहा होता है कि वे पलटकर उस पर वार कर देंगे?
इन शंकालुओं को यह समझना चाहिए कि हर वीरबालक जहाँ तक हो सके हेड आफ डिपाट कटगरी के किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता जो पलटकर उसका कोई नुकसान कर सकता हो। अगर वह ऐसे व्यक्ति पर प्रहार करता भी है तो किसी अन्य हेड आफ डिपाट के आशीर्वाद और कृपादृष्टि आश्वासन ले लेने के बाद ही। रीडर और लेक्चरर कटगरी के वीरबालकों पर प्रहार करना निरापद ही नहीं, आवश्यक भी समझा गया है। नई पीढ़ी के वीरबालक पुरानी पीढ़ी के अब वयोवृद्ध हो चले ऐसे नामवर वीरबालकों पर निर्भय होकर प्रहार करने लगे हैं जिनके पास अब कोई खास सत्ता रह न गई हो। लेकिन पुरानी पीढ़ी के वीरबालक इतने सयाने हैं कि टाप पोजिशन पर रह चुके किसी अन्य वृद्ध वीरबालक पर तब तक वार नहीं करते जब तक उसकी तेरहवीं क्या, बरसी न हो गई हो।
कुछ पाठकों को शंका हो सकती है कि जब वो वाले 'सर' सत्तावान अथवा प्राणवान अथवा दोनों ही थे तब वीरबालकों ने जाकर उनसे यह नम्र निवदेन क्यों नहीं किया कि 'सर' अन्यथा न लें लेकिन हमारी समझ से आप रिएक्शनरी और डिकाडेंट दूनों हैं। वीरबालक रिवोल्युशनरी के साथ-साथ ऋषि भी होता है और ऋषियों को बड़ों का निरादर करना शोभा नहीं देता। अब शंकालु यह पूछ सकता है कि क्या ऋषियों को गाली-गलौज करना शोभा देता है? अरे ऋषियों को न देता हो रिवोल्युशनरियों को तो देता है ना। इस तरह की क्रांतिकारी कार्रवाई ही तो वीरबालक-बिरादरी के जाग्रतावस्था में पहुँची है वर्ना उसमें तो ऊँघते रहने की महामारी व्याप्त है। वीरबालकों की आँखें तभी खुलती हैं जब कान में गालियों की आवाज पड़े या काकटेल्स के लिए पुकार।
रीडर कटगरी के वीरबालकों के लिए यह भी निरापद समझा जाता है कि वह परोक्ष प्रहार करें अर्थात कोई ऐसी कहानी या कविता लिख दें जिसमें कुछ वीरबालक विशेष या एक वीरबालक विशेष नितांत घृणित किस्म का पात्र बना दिया गया/दिए गए हों। ऐसी हर रचना की बहुत चर्चा होती है और सभी वीरबालक उसके विषय में एक-दूसरे को फुनियाते हैं। इस तरह का प्रच्छन्न प्रहार इसलिए निरापद माना गया है कि जिस किसी पर प्रहार किया गया हो वह तो मानेगा ही नहीं कि इस रचना का निशाना मैं हूँ। स्वयं रचनाकार को भी यह सुविधा मिल जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने निशाने से कह दें कि सर आपके शत्रु इतने घृणित हैं कि मेरे और आपके संबंध बिगाड़ने के लिए कहते डोल रहे हैं कि अपनी रचना में मैंने उनका नहीं, आपका पर्दाफाश किया है।
समझदार वीरबालक एक समय में एक से ज्यादा हेड आफ डिपाट को नहीं जुतियाता। और उसे जुतियाने से पहले भी किसी अन्य हेड आफ डिपाट से वचन ले लेता है कि आप हमको एक जोड़ा नया जूता तो दिलवा दीजिएगा ना? सभी सरों के सिर पर ताबड़तोड़ जूते बरसाने में दो खतरे पेश आते हैं। पहला यह कि आप पागल समझ लिए जाएँगे। दूसरा यह कि आपका जूता टूट जाएगा और आप जानिए नंगे पाँव चलने वाले का वीरबालकों के साहित्य में भले ही अनन्य स्थान हो, वीरबालकों की बिरादरी में वे नगण्य समझे जाते हैं। उनके बारे में यह तक नहीं माना जाता कि वे वे मकबूल फिदा हुसैन मार्का बेहतरीन स्टंटबाज हैं। सीरियस वीरबालक बिरादरी में स्टंटबाजी नहीं चलती तो सुजान वीरबालक किसी सर के सिर पर जूता तभी बरसाता है जब किन्हीं अन्य सर की वरद हथेली उसके अपने सिर पर टिकी हुई हो। ज्ञातव्य है कि हिंदी में जूनियर वीरबालक डाक्साब और सीनियर वीरबालक सर कहकर संबोधित किए जाते हैं। जौत्यकर्म के विषय में विधान यह है कि इसे दो अवस्थाओं में ही अधिक करना उचित है। या तो तब जब आप करियर बनाने के लिए हाथ-पाँव मार रहे हों या फिर जब आप हेड आफ डिपाट बन चुके हों। करियर की तलाश में लगभग घिस चुका फटा-पुराना जूता धड़ाधड़ प्रतिष्ठितों के सिर पर बरसाएँगे तभी वयोवृद्ध वीरबालकों की नोटिस में आएँगे। उनमें से हर हेड आफ डिपाट ललचाएगा कि क्यों नहीं इस बलिष्ठ-बाहु को फैलोशिप दिलवाकर पटा लूँ कि यह मेरे दिए जूते से मेरे प्रतिद्वंद्वियों को तसल्लीबख्श ढंग से गंजा करता रहे। फैलोशिप मिल जाने के कुछ ही समय बाद गुरुजनों की संगत में तरुण वीरबालक को यह बात समझ में आती है कि राजनीति की तरह साहित्य में भी स्थायी दोस्त दुश्मन-जैसी कोई चीज नहीं होती। शत्रुता का एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण मैच चलता रहता है। सौदेबाजी चलती रहती है और समीकरण बदलते रहते हैं। इसलिए आपसी गाली-गलौज को बहुत सिर-यसली में नहीं टेक किया जाता।
सच तो यह है कि जौत्यकर्म को मनोरंजक रूप से उत्तेजक और उत्तेजक रूप से मनोरंजक विधा का दर्जा दिया जाता है। 70 के दशक से उस मुक्तमंडी का वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ जिसकी संस्कृति ओर राजनीति दोनों में ही इस तरह के उत्तेजक-मनोरंजक जौत्यकर्म का अच्छा भाव लगता है। मुझे याद है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना के अवसर पर साहू जैनों द्वारा आयोजित महासम्मेलन में बहैसियत तरुण वीरबालक मैं थोड़ा गरजा-बरसा और मेरे बाद श्रीकांत ने तो उसी हैसियत से सत्ता-प्रतिष्ठान और उससे जुड़े साहित्यकारों पर इतना जोरदार प्रहार किया कि बोलते हुए उसकी कमजोर काया अपने दुस्साहस पर स्वयं ही काँपती रही। वह तब हैरान हो गया जब बाद में श्रीमती रमा जैन ने उसे बुलवाया और बहुत प्यार से समझाया कि जोश बहुत अच्छी चीज है लेकिन थोड़ा संयम भी जरूरी होता है। कुछ ही समय बाद श्रीकांत भी मेरे साथ साहू जैनों के दिनमान में काम करता नजर आया।
अगर मैं भूला नहीं होऊँ तो लगभग उन्हीं दिनों पेरिस में पी.ई.एन. के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए अमरीकी नाटककार आर्थर मिलर ने ने इस विडंबना की ओर ध्यान दिलाया था कि लोकतंत्र वाले देशों में सत्ता प्रतिष्ठान को मुँह बिराते संस्कृतकर्मी अब जेलों में नहीं, भव्य दफ्तरों में कैद किए जा रहे हैं। उनकी हैसियत खतरनाक क्रांतिकारियों की नहीं, मनोरंजक उछल-कूद करने वाले बंदरों की रह गई है इसलिए वे जितना ही ज्यादा गाली-गलौच करते हैं उन्हें उतना ही ज्यादा प्यार से गले लगाया जाता है। उन्हें अपनाकर सत्ता प्रतिष्ठान अपनी छवि सुधार लेता है और साथ ही स्वयं उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान का ही एक हिस्सा बना देता है। कृपया ध्यान दें कि मिलर ने यह बात विचारधारा की समाप्ति और मुक्तमंडी की विश्वविजय के मौजूदा दौर से कई दशक पहले कही थी।
आज तो पूँजीवादी मीडिया हर कहीं वामपंथी वीरबालकों को वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर सर्वहारा की पैरवी और मुक्तमंडी की भर्त्सना करने के लिए तगड़ा वेतन और हर तरह की सुख-सुविधा दे रहा है। लोकतंत्र और मुक्तमंडी के अंतर्गत स्वयं राजनीति भी कुल मिलाकर वीरबालकवादी हो चली है इसलिए आज भारत जैसे असामंती देश तक यह संभव है कि आप किसी सेठ की या सरकार की नौकरी करते हुए भी अपने को सत्ता-प्रतिष्ठान-विरोधी क्रांतिकारी मान और मनवा सकें। कभी कम्युनिस्ट होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, आज विचारधारा की समाप्ति के बाद यह आलम है कि पूँजीपति मीडिया में काम करने वाले पत्रकार और आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारी भी अपने को कम्युनिस्ट बता रहे हैं। बहरहाल वीरबालक बिरादरी सेठाश्रय और राजाश्रय का मुक्तकंठ से विरोध करती पाई जाती है उसमें एक-दूसरे पर सेठाश्रय या राजाश्रय लेने का आरोप लगाने का रिवाज है।
हर समझदार वीरबालक यह जानता है कि प्रतिरक्षा का श्रेष्ठ उपाय प्रहार है। इसीलिए वह 'जो पहले मारे सो मीर' के सिद्धांत पर पूरी आस्था रखता है। पहले हमला करने वाला अपने पर जवाबी हमला करने वाले को लचर सफाई देने वाला ठहराते हुए पूछ सकता है कि अगर आपको मैं पतित और प्रतिक्रियावादी लग रहा था तो आप अब तक चुप्पी काहे साधे थे? इस पर सफाई देने वाला यदि अतिरिक्त सफाई देते हुए यह कहे कि मैं तो शालीनतावश चुप था तो कोई बात बनती नहीं। कारण, वीरबालक बिरादरी में 'शालीनता' की तो होती है लेकिन शालीनता की नहीं। शालीनता अर्थात अपनी समस्त प्रगतिशीलता के बावजूद सरस्वती-वंदना सुनने और शंख-ध्वनि के बीच शाल, श्रीफल, प्रतिमा और चेक लेने की स्वीकृति। मैं बराबर इस प्रतीक्षा में रहा हूँ कि कोई वीरबालक 'शालीनता' पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक आपत्ति उठाएगा। व्यावहारिक यह कि जब हम न शाल ओढ़ते हैं और न हमें नारियल गिरी की बर्फी पसंद है तब आप शाल-श्रीफल ही क्यों दिए चले जाते हैं? सूट लेंथ और स्काच नहीं दे सकते क्या? सैद्धांतिक यह कि हम क्रांतिकारियों को इस तरह की भारतीयता अर्थात प्रतिक्रियावाद से जुड़ी चीजें क्यों दी और सुनाई जा रही हैं।
यहाँ उल्लेखनीय है कि वीरबालक बिरादरी के लिए 'भारतीयता' खासी गड़बड़ सी चीज रही है। किसी के पतित ठहरा देने का अचूक तरीका वीरबालकों में यही माना जाता रहा है कि उसे पुरातनपंथियों या हिंदुत्ववादियों से जोड़ दिया जाए। जब से भाजपा भी सत्ता की भागीदारी होने लगी है तब से वीरबालकों के लिए उससे जुड़ने का लालच और उससे जोड़ दिए जाने का खतरा दोनों ही बहुत बढ़ गए हैं। एक संस्मरण ठोकने की अनुमति चाहता हूँ। मुझे व्यंग्य लेखन के लिए पुरस्कार दिया जाना था। आयोजकों ने कहा कि अपनी पसंद का कोई वक्ता बता दीजिए। मैंने ऐसे अधेड़ वीरबालक का नाम सुझाया जिसकी रचनाएँ मैं बहुत पसंद करता हूँ। आयोजन से हफ्ता भर पहले उसका मेरे पास फोन आया कि जोशी जी मैं दो रात से सो नहीं सका हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ?
मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, पूछा, 'क्या हुआ भाई?' पता चला कि पुरस्कार देने अटल जी आ रहे हैं। और उनके वयोवृद्ध बालकों ने कहा है कि संघ परिवार से जुड़े पी.एम. के साथ मंच शेयर करना ठीक नहीं रहेगा। मैंने उनसे न यह पूछा कि सी.पी.एम. के नेता संघियों के साथ क्यों पर्लियामेंट शेयर कर रहे हैं और न यह कि वयोवृद्ध वीरबालक संघीय पी.एम. की सरकार द्यारा गठित समितियों और आयोजित गोष्ठियों में क्यों चले जा रहे हैं? मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि परेशान क्यों होते हो मना कर दो। इस पर उसने राहत और हैरानी दोनों एक साथ व्यक्त की। वीरबालकवादियों के लिए सही मंत्रों का जाप करना और राजनीतिक छुआछूत बरतना बहुत आवश्यक माना गया है। इसके अभाव में आपकी वीरता संदिग्ध हो जाएगी क्योंकि वीरता दिखाने के लिए कोई और अवसर न प्रस्तुत हुआ है और मुक्तमंडी ने चाहा तो आगे भी प्रस्तुत नहीं होगा। परम प्रसन्नता का विषय है कि स्वाधीनता के बाद से अब तक हिंदी भाषी प्रदेश में कुल एक बार ऐसा अवसर आया जब वीरता के प्रदर्शन से कष्ट में पड़ने का कोई खतरा पैदा हो सकता था।
वह था आपातकाल। लेकिन उसके दौरान वीरबालकों ने कोई खास वीरता प्रदर्शित की नहीं। शायद इसलिए कि वे जेल नहीं जाना चाहते थे या शायद इसलिए कि वे इंदिरा गांधी को वामपंथी समझते थे। खैर जो हो, उसके वर्षों बाद कुछ वीरबालक आपातकाल के संदर्भ में भी वीरता और कायरता के प्रमाण पत्र बाँटते रहे। मेरी कायरता असंदिग्ध है क्योंकि मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी। लेकिन यह भी असंदिग्ध है कि उस दौर में वीरबालक बिरादरी में कुर्सी छोड़ देने की कोई प्रतियोगिता नहीं चली हुई थी। मेरे मित्र साहित्यकारों में केवल कमलेश ही ऐसे थे जो इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ कर दिखाने के लिए निकले थे। प्रसंगवश बाद में कमलेश वीरबालक बिरादरी के लिए समर्थ कवि और प्रकांड विद्वान से ज्यादा इस रूप में सांय स्मरणीय हुए कि समर्थ मेजबान हैं। मेरे दोस्तों में कुल निर्मल वर्मा ने ही 'जोशी हाउ कैन यू...' वाली शैली में लताड़ते हुए तब कायर संपादक कहा था। औरों को तो यह इलहाम इंदिरा गांधी के हार बल्कि मर जाने के बाद हुआ।
वीरबालक कुर्सी छोड़ना नहीं, कुर्सी पाना चाहते हैं। औसत वीरबालक ने ज्यादा नहीं तो इतना समझने लायक मार्क्सवाद तो पढ़ ही रखा होता है कि हम एक अर्द्धसामंती समाज में जी रहे हैं जिसमें कलम से कहीं ज्यादा महिमा कुर्सी की है। रुतबा, रौब, रुपया, कुर्सी पर बैठने के बाद ही मिलता है। कुर्सी ही जमाने और उखाड़ने के लिए अधिकार दिलाती है, जो भक्तों को आकर्षित शत्रुओं को आतंकित करती है। वीरबालक भयंकर रूप से सत्ता-ग्रंथि का मारा हुआ होता है क्योंकि हिंदीभाषी क्षेत्र में साहित्य और साहित्यकार की अपनी अलग से कोई सत्ता बची ही नहीं है। मुझे अपने दोस्त श्रीकांत का एक सवाल याद आता है जो उसने मुझसे एक दिन दिनमान कार्यालय में पूछा था, यह बताओ जोशी कि ज्यादा पावर किस में होती है - पोस्ट में कि पालिटिशियन में? अगर मैं अपने कसबे बिलासपुर में पावरफुल पोस्ट होकर लौटूँ तो मुझे ज्यादा सम्मान मिलेगा कि पावरफुल मिनिस्टर बनकर लौटने में?
श्रीकांत मिनिस्टर तो नहीं बाद में एम.पी. जरूर बन गया और खुद यह देख सका कि जहाँ तक वीरबालकों का सवाल है उनके लिए संसद की सत्ता साहित्यकार की सत्ता से कहीं ज्यादा बड़ी है। श्रीकांत एक बढ़िया कवि के रूप में हमेशा याद किया जाएगा लेकिन उस दौर में वह पी एम के निकट होने और बड़ी दरियादिली से स्काच पिलाने के लिए याद किया जाता था। उसे भाव-विह्वल श्रद्धांजलि देते हुए एक वीरबालक ने कहा था, 'अब श्रीकांत जैसा स्काच पिलाने वाला कहाँ मिलेगा।' खैर तो वीरबालक एक-दूसरे पर प्रहार करते हुए यह मानकर चलते हैं कि राजनेता सर्वशक्तिशाली हैं और कुर्सियाँ उनकी कृपा से ही मिलती हैं और जब हमसे छिनती हैं तो राजनेताओं के कोप के कारण ही। बिरादरी में किसी को घटिया साबित करने का सबसे बढ़िया उपाय यह समझा जाता है कि उसे राजनेता की चापलूसी करके कुर्सी पाने और बचाने वाला सिद्ध कर दिया जाए।
अब जैसा रामशरण जोशी ने मुझे आपातकाल में कायरता दिखाने का प्रमाण पत्र देने के साथ-साथ यह भी बताया है कि इंदिरा गांधी के हार जाने के बाद अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए मैंने अटल जी की कुंडलियाँ छापनी शुरू कर दीं। सफाई देना इसलिए व्यर्थ नहीं है कि किस्सा खासा दिलचस्प है। हुआ यह कि जेल से अटल जी ने एक कुंडली संपादक के नाम पत्र के रूप में भेजी जिसमें मारीशस में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन पर कटाक्ष किया गया था। पत्र जेल-सेंसर से पास हो कर आया था इसलिए मैंने छाप दिया लेकिन इसके छापे जाने पर सूचना मंत्रालय के सेंसर ने मुझे फटकार सुनाई। फिर विदेशमंत्री बन जाने के बाद अटल जी ने अपने कुछ गीत प्रकाशनार्थ भेजे जिन्हें मैंने तुरंत नहीं छापा। इस पर उन्होंने संपादक पर व्यंग्य करते हुए एक कुंडली भेजी। फिर मैंने उनके गीत छापे और उनकी भेजी कुंडली और जवाबी संपादकीय कुंडली भी साथ ही साथ छाप दिए। संपादकीय कुंडली में कहा गया था कि मंत्री पद पा जाने पर कवि हो जाना सहज संभाव्य है।
मुझे सचमुच बहुत अफसोस है कि मुझे अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे घटिया काम करने पड़े। जहाँ तक रामशरण जोशी का सवाल है मेरे लिए यह अपार संतोष का विषय है कि उन्हें अपने नक्सलवादी विचारों के कारण माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कार्यकारी निर्देशक का पद मिल गया है और इसे पाने या बचाने के लिए उन्हें कभी किसी कांग्रेसी सी.एम.,पी.एम. की चाटुकारिता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। खैर शत्रुतापूर्ण मैत्री और मैत्रीपूर्ण शत्रुता में विश्वास करने वाले वीरबालकों में एक-दूसरे के बारे में झूठ बोल देने से परहेज उतना ही कम किया जाता है जितना कि अपने बारे में सच्चाई स्वीकार करने से। दूसरों के बारे में कहीं से कोई गड़ा मुर्दा उखाड़कर ले आया जाता है तो अपने बारे में यह तक भुला दिया जाता है कि अभी कल ही हम कहीं और क्या कह अथवा कर चुके हैं। अरे परिपक्वता आने के साथ-साथ आदमी का विचार बदलता है कि नहीं? कुछ वयोवृद्ध वीरबालक तो इस मामले में इतने भुलक्कड़ हैं कि एक ही गोष्ठी में बोलते-बोलते परिपक्व हुए चले जाते हैं। वीरबालक बिरादरी में कुर्सी इसलिए भी बहुत जरूरी समझी जाती है कि यद्यपि हर वीरबालक अपने को कलम का मजदूर कहता है तथापि वह लिखकर पैसा कमाने को कलम बेच देने का पर्याय मानता है। इसलिए कभी वीरबालकों को पत्रकारिता से भी परहेज था। अब उससे तो नहीं लेकिन फिल्म और टीवी के लिए लिखने से है। खैर पत्रकार या लेखक के रूप में मीडिया से जुड़ने वाला हर वीरबालक यह कहते रहने जरूरी समझता है कि मैंने अपनी कलम बेची नहीं है और सरकार या सेठ से किसी तरह का समझौता नहीं किया है। पूँजीपतियों से जोड़े जाने के कलंक से बचने के लिए कुछ सयाने वीरबालकों ने किसी ऐसे छोटे-मोटे सेठ को पकड़ लेने की युक्ति अपनाई है जो साहित्य का मारा हुआ हो और बुद्धिजीवियों की सोहबत करा देने की एवज में सारे खर्चे-पानी का जुगाड़ खुशी-खुशी कर देता हो।
जो वीरबालक बड़े सेठों के लिए काम करते हैं वे इस बात को छिपा जाते हैं कि मालिक को नौकर की वैचारिक क्रांतिकारिता से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो केवल जी-हजूरी और हितरक्षा चाहता है। जब तक आप विज्ञापन से आय बढ़वाते और सत्तावान लोगों से संबंध सुधरवाते रहेंगे तब तक सेठ आपको सांस्कृतिक पृष्ठों पर कुछ भी लिखने-छापने की पूरी छूट देता रहेगा। दूसरे वीरबालक आपकी शिकायत करें तो वह अनसुनी कर देगा। जी हाँ, सेठ से यह शिकायत की जाती थी कि आपका संपादक कम्युनिस्ट है और पश्चिमी रंग में रंगा हुआ है। अब यह शिकायत की जाती है कि आपका संपादक पोंगापंथी हिंदी वाला है जो भूमंडलीकरण के तकाजों से अनजान है।
कभी मेरे द्वारा साप्ताहिक हिंदुस्तान कि आवरण पर कांगड़ा-शैली के श्री राधा जी के चित्र के बारे में कृष्ण कुमार जी से यह शिकायत की गई कि पश्चिमी रंग में रंगे कम्युनिस्ट संपादक ने राधा का नग्न चित्र छापकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। कृष्ण कुमार जी ने मुझे बुलाकर कहा था, कांगड़ा शैली का है वह तो मैं समझ गया लेकिन भई देखो अपन ऐसे फोटो निकालें ही क्यों की लोग नाराज होवें और सर्कुलेशन घटे। मैं समझता हूँ कि अब नई पीढ़ी के सेठ भी नई पीढ़ी के संपादक जी को बुलाकर कुछ यों कहते होंगे, पोर्नोग्राफी के लिए कौन कह रहा है भई लेकिन अपने प्रोडक्ट की अपमार्केट इमेज तो बनानी ही चाहिए। हिंग्लिश यूज करके और लुगाइयों के सेमीन्यूड फोटो निकालकर। नहीं तो अपनी तो एड-रेवेन्यु निल रह जाएगी। जिसे पुराना सेठ अपसंस्कृति की जननी समझता था उसे नया सेठ अपमार्केट की मदर बताता है।
किसी छोटे या बड़े नेता, किसी छोटे या बड़े सेठ की कृपा से किसी गद्दी पर आसीन साहित्यिक सामंत वीरबालक का जलवा देखना हो तो उसके साथ कभी दौरे पर निकलिए। जहाँ जाइएगा स्टेशन या हवाईअड्डे पर स्थानिक वीरबालकों की सलामी गारद अटेंशन में पाइएगा। उसका स्थानिक मन-सबदार उसे हार पहनाएगा और वेरी इंपोर्टेंट वयोवृद्ध वीरबालक वी.आई.वी.वी. की चरण रज अपने माथे लगाएगा। फिर अपने यहाँ के सबसे बड़े नेता, सेठ या अधिकारी की कार में वी.आई.वी.वी. को अपने यहाँ के सबसे बढ़िया होटल या सरकारी विश्राम गृह में ले जाइएगा जहाँ कार-दाता एक और सलामी-गारद, एक और हार के साथ प्रस्तुत होगा। सलामी की रस्म पूरी हो जाने के बाद कारदात अपना स्काचदाता रूप दिखाते हुए एक बोतल सेवा में प्रस्तुत करेगा। जो सभा होगी उसमें वी.आई.वी.वी. अपनी वीरता और शत्रुओं की कायरता का बखान करके स्थानीय वीरबालकों की दाद पाएगा और स्थानीक साहित्यकारों के वीरबालकवादी तेवरों पर स्वयं दाद देगा। साहित्य चर्चा अंतर्गत इतना ही होगा कि स्थानिक वीरबालक वी.आई.वी.वी. को अपनी कोई पुस्तक थमाते जाएँगे कि सर पढ़कर दो शब्द लिखने की कृपा करें। सर प्रोत्साहन के दो शब्द वहीं बगैर पढ़े कह डालेंगे और दिनभर में मिली कई किलो रद्दी स्थानिक मनसबदार के लिए छोड़ आएँगे।
वी.आई.वी.वी. तरुण वीरबालकों को यह नेक सीख दे जाता है कि अच्छा साहित्यकार होने के लिए अच्छा वीरबालक होना जरूरी है, कुछ अच्छा पढ़ना या लिखना नहीं। जहाँ तक हो सके लिखो ही मत। लिखो तो अच्छा मत लिखो क्योंकि रूपवादी समझ लिए जाओगे। और देखो तुम्हें लिखने के जिद ही हो तो ऐसी छोटी-मोटी कविताएँ लिखो जिनकी तारीफ में मित्र आलोचक जितना भी कहें वो कम हो लेकिन जिनके बारे में इतना कहना ही काफी हो कि याद न रखी जा सकने के मामले में ये सर्वथा यादगार है। ऐसी कविताएँ लिखने में समय कम लगता है और संग्रह जल्दी तैयार हो जाता है। संग्रह पढ़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। उपन्यास लिखोगे तो सभी वीरबालक लोकार्पण गोष्ठी में बिना पढ़े ही पहुँच जाएँगे। लेकिन दि बेस्ट तो यह है कि कुछ भी मत लिखो। बस विवादस्पद वक्तव्य, साक्षात्कार देते रहो। इस बात को समझो कि वीरबालकों के साहित्य-दरबार में राजा इंद्र का रोल ऐसे रिवोल्युशनरी ऋषि को ही नसीब हो पाता है जो आसार-संसार में आकंठ लिप्त होते हुए भी साहित्य संसार में संन्यास ले चुका हो। अब लगे हाथों कुछ बातें वीरबालकवाद के ऋषि पक्ष के संदर्भ में भी कर ली जाए। साहित्यिक हाजमा ठीक रखने के लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम की डोज नियमित रूप से पीने और पिलाने वाले हमारे वीरबालकों का ऐसा विश्वास है कि ऋषिगण सुरा-सुंदरी और राजदरबार में मिलने वाले मान-सम्मान तीनों से सख्त दूरी बरतते आए हैं। सांसारिक भोग-विलास से यह परहेज ही उन्हें समाज की आँखों में राजा से ऊँचा स्थान दिलाता आया था। अब सुरा का ऐसा है कि उसका आविष्कार हुआ ही इस लिए की कतिपय कविमन किस्म के प्राणियों ने पाया कि नशे के अभाव में सही सुर लग नहीं पाता है। और सुंदरी का ऐसा है कि मानव जाति ने लँगोट का ईजाद किया ही तब जब आमराय यह बनी कि जो मर्द बच्चा सो लँगोट कच्चा।
प्राचीन ऋषियों के बारे में मेरी जानकारी नहीं के बराबर है इसलिए मैं पंडित वागीश शुक्ल से पूछकर ही आपको बता सकूँगा कि वे सुरा और सुंदरी से कितना परहेज बरतते थे। संभव है तब भी न बता पाऊँ क्योंकि प्राचीन भारत के बारे में किसी तरह की गड़बड़ बात बोलना निरापद नहीं है। दो नवीन ऋषियों उर्फ वीरबालकों में से ज्यादातर सुरा-सुंदरी त्याग नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो इस संदर्भ में सारा वीरबालकत्व यह सिद्ध करने में है कि मैं पीता भी हूँ तो अपने पैसे की जबकि दूसरे मुफ्त की पीते हैं? जी हाँ, और अगर कौनो जन बहुत पीछे पड़ जाए तो हमहु पी लेते हैं। इस संदर्भ में वयोवृद्ध वीरबालकों के बारे में तरुण वीरबालक दिलचस्प जानकारियाँ देते रहे हैं मुझे। जैसे यह कि उनमें से एक सुरा-प्रेमियों को दर्शन देने बहुधा आ जाते हैं लेकिन मधुशाला को उनसे एक कानी कौड़ी भी लेने का आज तक कष्ट नहीं उठाना पड़ा है। कलम का कोई भी मजदूर शराब पीने में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बरबाद नहीं कर सकता, अपना जिगर भले कर दे।
जहाँ तक सुंदरियों का संबंध है कदाचित इतना ही कह देना पर्याप्त हो कि साहित्यकार होने के नाते वीरबालक में आरंभ से ही उत्कट सौंदर्यबोध रहता है और आयु के साथ-साथ उक्त सौंदर्यबोध तीव्रतर होता चला जाता है। स्वाभाविक है कि जो सुंदरियाँ युवा वीरबालक को माताएँ-बहनें लगती रहीं थीं वे वृद्धावस्था में बेटियाँ प्रतीत होने लगती हैं। पूर्णाहुत से ठीक पहले या ठीक बाद के क्षण में। नितांत प्रीतिकर रूप से पारिवारिक यह सौंदर्यप्रियता वीरबालकों के ऋषिपद की सुरक्षा करती रहती हैं। अब ऐसा है कि वीरबालक ऋषि के साथ-साथ क्रांतिकारी भी होते हैं और क्रांतिकारी आप जानिए आधुनिक भी होता है और आधुनिकता के मारे आप जानिए कि जैनेंद्र जी जैसे गांधीवादी लेखक तक को पत्नी के साथ-साथ प्रेमिका भी आवश्यक प्रतीत होने लगी थी। तो वीरबालक को क्रांतिकारी रूप में एक ठो प्रेमिका भी अपेक्षित रहती है। बल्कि दो ठो क्योंकि अज्ञेय नदी के द्वीप में अपने साथ रेखा और गौरा दूनों को ले गए थे और सौंदर्यबोध के क्षेत्र में अज्ञेय ही क्रांतिकारियों के आदर्श हैं। वीरबालकवादी साहित्यकार अपने आसपास से जुड़ा रहता है इसलिए जोड़ीदार प्रेमिका को भी आस-पास से ही प्राप्त करना चाहता है। इसके चलते साहित्य-साधिका को ही प्रेमिका बनाने की परिपाटी चली आ रही है। आज वीरबालकवादी डींगें वीरबालकवादी ढोंग के अनुपात में ही इतनी बढ़ चली हैं कि अब हर साहित्य-साधिका किसी न किसी वीरबालक को प्रेमिका ठहराई जा रही है। प्रतिपक्ष के वीरबालक हर सफल साहित्य-साधिका के विषय में यहाँ तक कहते सुने जाते हैं कि वह स्वयं नहीं लिखती, भले घर की औरतों को बिगाड़ने वाला अमुक लंपट वीरबालक उसके लिए लिख दिया करता है। यह शंका करना अपनी मूर्खता का परिचय देना होगा कि अगर वह लंपट-लँगोट-लुच्चा इतना अच्छा लिख सकता है तो अपने नाम से ही क्यों नहीं लिख लेता?
वीरबालक अपनी प्रेमिका का इस अर्थ में भी संरक्षक होता है कि वह उस पर दूसरों की बुरी नजर नहीं पड़ने देता। एक साहित्य-सभा के बाद चाय-पान के दौरान मैं अपना परिपक्व सौंदर्याबोध एक नवोदिता पर आजमाने लगा तो एक वयोवृद्ध वीरबालक विशेष मुझे बाँह पकड़कर एकांत में ले गए और उन्होंने फुसफुसाकर मुझसे कहा कि अइसा है ये बहुत ही संभ्रांत घर की महिला हैं और इनसे हमारा पारिवारिक सा संबंध रहा है। आप इनसे कुछ इस टाइप... आप समझ रहे हैं ना? अब इतना नासमझ तो बंधुवर मैं भी नहीं हूँ। इधर कुछ अन्य वीरबालक जो कोई ओर क्रांतिकारी चीज लिखने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, अपनी प्रेम-लीलाओं का सार्वजनिक स्वीकार करके अपनी वीरता का प्रमाण दे रहे हैं। सिद्ध कर रहे हैं कि भले ही वे अपने आराध्य पश्चिमी लेखकों जैसा कुछ रच न सके हों प्रेमिकाएँ अपनाने-छोड़ने के मामले में उनसे कभी पीछे नहीं रहे हैं।
ऋषि-ग्रंथि के अंतर्गत वीरबालक बिरादरी में राजाश्रय और सेठाश्रय दोनों बड़ी घटिया किस्म की चीजें मानी जाती है। इसीलिए वीरबालक अपने लिए एक ठो स्टैंडर्ड बायोग्राफी गढ़ चुका होता है। मामूली हैसियकत वाले परिवार में जन्म, संघर्षरत माता अथवा पिता अथवा दोनों से प्रेरणा प्राप्त, निर्दय समाज से निर्भीक टक्कर, प्रलोभन ठुकरा क्रांति पथ पर अग्रसर, सीकरी को ठेंगा दिखाने के दंड-स्वरूप मान-सम्मान से वंचित, तिकड़मबाजों द्वारा उपेक्षित किंतु आश्वस्त कि हिस्ट्री बोलेगी ही वाज सिंपली ग्रेट बट हिस्ट्री की डिफिकल्टी यह है कि वह ससुरी मरणोपरांत शुरू होगी। तो वीरबालक दारू से महकती एक आह भरकर कहता है अपने से और अपनों से कि 'अइसे तो हम निराला, मुक्तिबोध की तरह अनचीन्हे मर जावेंगे' इसलिए नौकरी-वौकरी करनी पड़ जाती है और अपना स्थान बानने के लिए भी संघर्षरत रहना पड़ता है।
बता ही चुका हूँ कि वीरबालक-बिरादरी में यह माना जाता है कि दूसरों को नौकरी भ्रष्ट विचारधारा और उत्कृष्ट चमचागीरी के कारण मिली है। इसमें इतना और जोड़ना आवश्यक है कि इस बिरादरी में अगर किसी की कुर्सी जाती है तो वह यही कहता है कि मुझे अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण प्रतिक्रियावादी प्रतिष्ठान ने पद से हटाया। खैर इतना निर्विवाद है कि वीरबालक नौकरी सरकार की कर रहे हों या सेठ की वे सच्चे सेवक क्रांति के ही होते हैं। जैसा कि सरकारी नौकरी वाले एक नवोदित वीरबालक ने भरी सभा में मुझे 'सिनिसिज्म' के लिए लताड़ते हुए घोषणा की थी, जैसे तुलसी ने राम की चपरास गले में डाल ली थी वैसे हमने क्रांति की चपरास गले में डाल ली है। गोया वीरबालक राज हो या सेठ के दिए कपड़े भले ही पहन ले नीचे क्रांति की कोई जनेऊनुमा चपरास बराबर डाले रहते हैं कि नौकरी जाते ही कपड़े उतार के उसे दिखा दें।
राजाश्रय या सेठाश्रय की अनिवार्यता से तिलमिलाते वीरबालक फिर एक क्रांतिकारी स्थापना यह करते हैं कि हमें साहित्य में सेठों और नेताओं की घुसपैठ स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अस्तु, न सरकारों और सेठों के दिए पुरस्कार ग्रहण किए जाएँ और न ऐसे किसी साहित्यिक आयोजन में सम्मिलित हुआ जाए जिसमें किसी मंत्री या सेठ को बुलाया जा रहा हो। लेकिन इसमें भी कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे यह कि नेता न आए तो टी.वी. कवरेज नहीं होता, और तमाम जिस चीज का टी.वी. में कवरेज न हुआ हो वह न हुई मान ली जाती है। पुरस्कारों का ऐसा है कि सरकारों या सेठों द्वारा ही दिए जाते हैं। उन्हें ग्रहण न किया जाए तो बेटी की शादी से लेकर फ्लैट की खरीद तक कई काम अटके रह जाते हैं और कायदे का बायोडाटा भी नहीं बन पाता। 'अस्तु, लेने ही पड़ जाते हैं बंधु।' और फिर आप यह भी तो समझिए ना कि अगर कौनो बड़का मंत्री या कैपिटलिस्टुआ हमको सम्मानित करे के बदे आता है तब हमारा अस्टेटस उससे हाई ही न कहा जाएगा?
इसके बाद ले-देकर यह बचता है कि साधारण साहित्यिक आयोजन में नेता या सेठ न बुलाए जाएँ। महमूर्ख किस्म के लोग ही यह शंका कर सकते हैं कि जब वीरबालकों को नेताओं के दरबार में स्वयं हाजिरी लगाते कोई आपत्ति नहीं होती तब साहित्य के दरबार में उनकी उपस्थित से इतना कष्ट क्यों होता है। हमारे वीरबालक सिद्धांतवादी है। इसलिए उनके तमाम विरोध सैद्धांतिक स्तर पर ही होते आए हैं, व्यावहारिक स्तर पर नहीं। सुनता हूँ कि एक वीरबालक ने अपने घनिष्ठ मित्र और संरक्षक छोटा सेठ से कहा, 'भाई मेरे बुरा मत मानियो सिद्धांत का मामला है आज मैं भरी सभा में तेरा जौत्य-कर्म करूँगा।' इस पर छोटा सेठ ने कहा, 'कर लियो भई लेकिन मीटिंग के बाद मंत्री जी से मेरा सौदा जरूर करवा दीयो।' इस तरह के तमाम दिलचस्प किस्से मुझे नवोदित वीरबालकों के मुँह से सुनने को मिलते रहते हैं क्योंकि अब मैं वीरबालक बिरादरी में स्वयं ज्यादा चलायमान नहीं रह गया हूँ।
तरुण वीरबालकों के कई किस्से सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और यही प्रमाणित होता है कि हमारे नेताओं की तरह साहित्यिक मठाधीशों ने भी ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें सब एक-दूसरे को और जाहिर है कि अपने को भी चोर मान रहे हैं। तरुण वीरबालक अधेड़ और वयोवृद्ध वीरबालकों की अनैतिकता, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के किस्से सुनाते जाते हैं और बेसब्री से मुझ वयोवृद्ध वीरबालक की किसी टिप्पणी की प्रतिक्षा करते हैं कि जाके संबद्ध व्यक्ति को सुना आएँ। मैं अपनी जबान को भरसक लगाम देता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि चुप रहने से भी वीरबालक बिरादरी में कोई बात बनती नहीं है क्योंकि आपके मुँह से निकला कोई-न-कोई उद्गार सुविधानुसार गढ़ लिया जा सकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि तरुण वीरबालक आकर कभी कोई साहित्यिक चर्चा नहीं करते। उनकी सारी बातचीत साहित्यिकार चर्चा को समर्पित रहती है। वह यही बताना चाहते हैं कि किसको जमाने-उखाड़ने के सिलसिले में वयोवृद्ध वीरबालकों में क्या सौदेबाजी हुई है।
उनके अनुसार कभी-कभी ये सौदे साहित्य के दायरे तक सीमित होते हैं जैसे यह कि वीरबालक 'ए' ने वीरबालक 'बी'' के लेखन की पहली बार निंदा की जगह प्रशंसा इसलिए की है कि वीरबालक बी ने वीरबालक 'ए' के विवादास्पद वक्तव्य के समर्थन में कुछ लिख दिया है। लेकिन अकसर ये सौदे अहो रूपम अहो ध्वनि के दायरे से बाहर होते हैं। प्रशंसा की कीमत कैश या कांइड में वसूल की जाती है। तरुण वीरबालक आते हैं और आश्चर्य करते हैं कि सर क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अलाँ ने फलाँ को अपने खर्चे से विदेश यात्रा कराई है। अलाँ को तो फलाँ ने अपनी मिस्ट्रेस बना लिया है। अलाँ ने फलाँ के लिए उसकी कृति के विदेश अनुवाद किए जाने का या उसे विदेश में कोई फेलोशिप मिल जाने का जुगाड़ करवा दिया है। यह विदेश वाली बात तरुण वीरबालकों की चर्चा में अक्सर आ जाती है।
वीरबालकवाद के विदेश पक्ष का ऐसा है कि जहाँ ऋषि होने के नाते वीरबालक पश्चिम विरोधी होता है वहाँ क्रांतिकारी होने के होने के नाते वह आधुनिकता और मार्क्सवाद दानों का पक्षधर भी होता है और ये दोनों ही चीजें आप जानिए पश्चिमी ही हैं। इसलिए उसका आग्रह रहता है कि जिस हद तक मैं जीवन और लेखन में आधुनिक हुआ हूँ उस हद तक ठीक है लेकिन उसमें ज्यादातर पश्चिम के रंग में रंग जाना बहुत बुरा है। मेरे पाँव देश की माटी में मजबूती से जमे हुए हैं और मेरी जड़ें गाँव में गहरी गई हुई हैं। इसलिए मैं पश्चिमी-प्रदूषण की चपेट में आ ही नहीं सकता। लेकिन साथ ही वीरबालक को यह बोध भी रहता है कि मुझे गरीब, गँवई और आउट आफ डेट समझ लिए जाने का खतरा है इसीलिए वह सीकरी से कोई काम न रखते हुए भी सीकरी में अपने लिए एक ठो फ्लैट बनवा लेता है क्योंकि गाँव वाला घर तो वह फूँककर निकला होता है। सीकरी में प्रतीकात्मक माटी से सने हाथ वह ओडि क्लोन से धुलाने और प्रतीकात्मक पत्थर तोड़ते हुए सूखे कंठ को स्काच से तर करने की तथा बीच-बीच में फारेन कंट्रीज में हिंदी का झंडा गाड़ आने की व्यवस्था करता है।
वीरबालकों की इस विदेश ग्रंथि का जनक अज्ञेय जी को माना जा सकता है जिनके अभिजात्य से लोग-बाग उतने ही आक्रांत थे जितने कि उनके विदेश में प्रवास करते रहने से। मुझे लगता है कि जो लोग यह कहते सुने जाते थे कि अज्ञेय सी.आई.ए. के पैसे से विदेश जाकर नोबेल पुरस्कार के जुगाड़ में लगे रहते हैं, वे साथ ही इस बात के लिए भी ललक रहे थे कि हमारा भी कोई अंतरराष्ट्रीय चक्कर चले और हमारा भी दूसरों पर उतना ही रौब गालिब हो जितना कि अज्ञेय का हम पर हो रहा है। यही वजह है कि वीरबालक अपने साहित्यिक व्यायाम के लिए अंतरराष्ट्रीय आयाम तलाशते रहते हैं और अपनी हर उपलब्धि की सूचना अन्य वीरबालकों तक किसी न किसी तरह पहुँचाते रहते हैं ताकि जलने वाले जला करें।
तो हिंदी साहित्य में स्त्री-विमर्श पर बोलते हुए आप किसी वी.आई.वी.वी. को यह बोलते हुए सुन सकते हैं, 'अभी मेरे पूर्व वक्ता आयोवा की अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का जिक्र कर रहे थे, अमरीका के ही एक अन्य राज्य वरमोंट में उससे भी बड़ा आयोजन होता है जिसमें साहित्यकारों समेत चंद चुने हुए रचना-धर्मी व्यक्ति शांत, सुनम्य वन-प्रदेश में बनी कोटेजेज में साल-छह महीने रहने और विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। पिछले साल मुझे भी वहाँ बुलाया गया था जहाँ मेरी भेंट एस्ट्रोनिया की प्रसिद्ध कवयित्री जालीमा योन्यारी से हुई जो आजकल मेरी कविताओं का अपनी भाषा में अनुवाद कर रही हैं। तो जालिमा की छोटी सी कविता की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसमें सारा स्त्री-विमर्श समा गया है - स्त्री अहा, आ स्त्री आ स्त्री बला, जा स्त्री जा, स्त्री हाय-हाय, हाय स्त्री।' इस पर तालियाँ बजती हैं क्योंकि वीरबालक की कविता में अब इतना भी उक्ति चमत्कार दुर्लभ हो चला है।
तो सभी वीरबालक विदेशों में कहीं-न-कहीं बुलाए जा रहे हैं और वहाँ कोई न कोई उनकी रचनाओं का अपनी भाषा में अनुवाद भी कर रहा है। थोड़ी सी दिक्कत है तो यही कि विदेशों में हिंदी लेखकों की साहित्यिक उपस्थिति कहीं दर्ज हो नहीं रही है जबकि अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को वहाँ तगड़ी रायल्टी और कलमतोड़ दाद मिल रही है। इसे चलते सहसा वीरबालकों का पश्चिम विरोध और अंग्रेजी विरोध भड़क उठता है। एक गोष्ठी में मैंने एक वी.आई.वी.वी. को यह सिद्ध करते हुए सुना कि अंग्रेजी में लिखने वाल सारे भारतीय लेखक चालू किस्म का लेखन करने वाली शोभा डे के भाई-बंद ही हैं। उन्होंने सारे उदाहरण शोभा डे के लेखन से ही दिए। वीरबालकवादियों के पश्चिम-विरोध का एक पक्ष यह भी है कि वे एक-दूसरे को पश्चिम की नकल करने वाला ठहराते रहते हैं। तो वीरबालक आधुनिक तो होता है लेकिन पश्चिम का पिछलग्गू नहीं। कृपया उसके पश्चिम के पिछलग्गू न होने का यह अर्थ भी न लगाया जाए कि वह पोंगापंथी होता है और साहित्य के संदर्भ में भारतीयता की बात करता है।
तो वयोवृद्ध वीरबालकों की कृपा से तरुण वीरबालकों की एक ऐसी पीढ़ी पनप रही है जो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों से समान रूप से कटी हुई है और जो पांडित्य और इंटेलेक्टचुअलता दोनों की विरोधी है। वह हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएँ पढ़ लेना ही पर्याप्त समझती है और इन पत्रिकाओं में भी सबसे ज्यादा ध्यान से वी.आई.वी.वी. के वक्तव्य और गोष्ठी-समाचार पढ़ती है। अधिकतर वीरबालक अब अपने को जनवादी कहते हैं लेकिन उमें से अधिकतर के शास्त्रार्थ से कहीं यह संकेत नहीं मिलता कि उन्होंने मार्क्सवादी-लेनिनवादी शास्त्रों का बाकायदा कभी अध्ययन किया है। बल्कि स्थिति यह है कि मार्क्सवादी-लेनिनवादी पोथे बाँचे हुए लोग अब वी.आई.वी.वी. को थोड़े हास्यास्पद प्रतीत होने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि कात्यायनी बहुत अच्छी कवयित्री होने के साथ-साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद की गहन समझ रखने वाली विदुषी भी हैं। इसलिए मेरे आश्चर्य का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने एक वी.आई.वी.वी. बहुल निर्णायक समिति में उनका नाम किसी पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया और पाया कि अनुमोदन करने के लिए कोई तैयार नहीं है।
वीरबालकवाद पर अपने इस वीरबालकवादी लेख की समाप्ति में एक काल्पनिक वीरबालक के बारे में एक ऐसे काल्पनिक संस्मरण से करना चाहता हूँ जो वास्तविकता के काफी निकट है और जो इस ओर इशारा करता है कि वीरबालकवादी तेवर हमें किन ऊँचाइयों की आरे ले जा रहे हैं। किसी कस्बे के हिंदी विभागाध्यक्ष ने 'अस्तित्ववाद' पर संगोष्ठी की अध्यक्षता के लिए ऐसे संपादक वीरबालक को आमंत्रित किया जिसने स्वर्गीय सार्त्र और लगभग स्वर्गीय अस्तित्ववाद का नाम नहीं सुना था लेकिन जो अपनी पत्रिका में हर उस गोष्ठी का वृतांत सचित्र छापता था जिसकी उससे अध्यक्षता कराई गई हो। अब पूछिए कि अस्तित्ववाद से अनजान वह वीरबालक अध्यक्ष पद पर विराजमान होकर क्या करता है?
वह ऊँघता है। सभी वीरबालक व्यस्तातिव्यस्त किस्म के व्यक्ति होते हैं और अध्यक्षताओं के सिलसिले में बादल आवारा को मात करते हैं। उन्हें सोने और साँस लेने की फर्सत तक अध्यक्ष पर विराजमान होने के बाद ही मिलती है। ऊँघने को वीरबालकों के संसार में ध्यान से सुनने का पर्याय ठहराया जाता है। और हर वीरबालक ऊँघते-ऊँघते भी बीच-बीच में दो-चार फिकरे सुन ही लेता है ताकि अगर विरोधी खेमे का कोई वीरबालक उसके सो जाने पर चुटकी ले तो फौरन डेढ़ आँख खोले और कहे, 'अरे आप कहते न रहिए महाराज, हम ध्यान से सुन रहे हैं और जल्दी से मेन पांइट पर आइए नहीं तो हम सचमुच सो जावेंगे। खैर तो जब हमारे वीरबालक अध्यक्ष की बोलने की बारी आती है तब वह ऊँघते-ऊँघते सुनी हुई बातों के आधार पर अपने को वीरबालक सिद्ध करने वाली कुछ बातें कहकर तालियाँ बजवा ही लेता है।'
यथा, हमें यह बहुत गड़बड़ लगता है कि हिंदी के आधुनिक लेखक पश्चिम के बड़े लेखकों की नकल मारकर अपने को बड़ा कहलवाना चाहते हैं। उससे भी ज्यादा गड़बड़ बात यह है कि नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी टाइप हमारे मार्डन मठाधीश इन नकली लोगों की पीठ ठोंकते रहते हैं। देखिए हमें भी बहुत लालच दिया गया कि मार्डन बनने के लिए एक्जस्टेन्सवाद अपनाओ। बट हमने कह दिया नो। आप पूछेंगे नो क्यों कहा? हमने तो इसलिए किया कि हम जानते हैं कि जो भी एक्जिस्टेन्सवाद है, वह भारतीयों के मार्डन नहीं एन्सिएंट है। भगवान बुद्ध हमारे यहाँ बहुत पहले कह चुके थे। फ्रांस के सारतरे ने उनके आइडिया की नकल मारकर अपने को बड़ा भारी राइटर और फिलासफर साबित करने की कोशिश की है। इस मरे सारतरे का रौब भारत भवन वाले खाते हों, हम जेनुइन भारतीय नहीं खाते क्योंकि हम प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं।
इस पर देशभक्ति और हिंदीभक्ति में लीन रहने वाले लोग इतनी तालियाँ बजाते हैं कि गदगदायमान वीरबालक को सहसा याद आता है कि संपादक की हैसियत से पिछली गर्मियों में मुझे पेरिस-प्रवास करने का सुख भी मिला था। अस्तु वह अब दूसरी ताली-तलब बात भी कह डालता है, पिछली गर्मियों में पेरिस विश्वविद्यालय ने हमें एक सेमिनार पर प्रिसाइड करने के लिए बुलाया था। वहाँ अंग्रेजी में लिखने वाले कुछ इंडियन राइटर्स भी थे। लंच ब्रेक में हमने देखा कि वे सब के सब हमें अकेला छोड़कर किसी अभी-अभी पहुँचे आदमी से बात करने के लिए चले गए हैं। तो हमने अपनी फ्रांसिसी मेजबान को बुलाया और उनसे फ्रेंच में कहा, 'हलो एक्सक्यूज मी', हू दैट मैन देयर?' मेजबान फ्रेंच में बोली, 'अरे दै! ही इज तो अपना सारतरे। सुनते ही हमने फैसला किया कि इसको यहीं सबके सामने खरी-खरी सुनाएँगे ताकि इसे पता चल जाए कि हिंदी राइटर इंडियन इंग्लिश राइटर्स की तरह पश्चिम का थूका हुआ चाटने वाला चाटुकार नहीं है।
इस पर तालियाँ बजती हैं वीरबालक अपनी विनम्रता और दुस्साहस दोनों का परिचय देते हुए बताता है, तो हम अपनी प्लेट लेकर सरतरे के पास पहुँचे। पहले सोच रहे थे कि उससे फ्रेंच बोलें लेकिन एक तो हमारी फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं है कि उसमें गूढ़ साहित्यिक चर्चा कर सकें। दूसरे हम चाहते थो कि अदर इंडियन राइटर्स भी हमारी बात समझ सकें। तो हमने सारतरे से कहा, 'हलो एक्स्क्यूज मी, आई आल्सो इंडियन राइटर बट मैं आपका रौब नहीं खाता। बल्कि पोजीशन यह है कि अब आप यहाँ आ गए हैं तो मैं खाना भी नहीं खाऊँगा। इसका रीजन यह है कि आपने सारा सहित्य उल्टी करने की इच्छा पर लिखा है। इसलिए आपको देखते ही मुझे उल्टियाँ आने लगी हैं। हम इंडियन्स हैं और हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता है इसलिए मैं आपसे बहुत आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि आपको बुद्ध से चुरायी हुई एक्जिस्टेन्सवाद की फिलासफी सैकेंड हैंड है और आपका लिटरेचर थर्ड रेट। थैंक्यु एंड गुड बाई। इतना कहकर हम वाकआउट कर गए।'
हमारा वीरबालक तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से उतरता है और जिस स्थानिक कवियित्री के वह दो मुक्तक छाप चुका होता है वह भाव-विभोर होकर उसकी ओर बढ़ती है। एक मुसरचंद-मार्का मूर्खबालक हमारे वीरबालक के आगे वह शंका रखने की धृष्टता करता है, लेकिन सर सार्त्र तो बहुत पहले ही मर चुके थे। वीरबालक बहुत आश्वासन के साथ कहता है, हाँ, मारे शर्म के।
Friday 2 March 2018
डोले बयरिया से अमवा की डरिया, चुनरिया पिउ की डगर बनि जाय..
मेरा एक मित्र था दीवाना। ये उसका उपनाम था। घर का नाम और। सचमुच दीवानगी के लहजों में लिपटा उपनाम उसके हावभाव पर खूब फबता था। एक बड़े महाकवि ने उसके रंग-ढंग देखकर उपनाम दिया था। फिर तो वह दीवाना नाम से ही जाना-पहचाना जाने लगा। वह भी कवि। जरा फिल्मी-विल्मी सा। वैसे भी उसे अपनी जिंदगी फिल्मी लगती थी। उसके जीवन और सृजन का दर्शन एक। कभी छेड़ने-कोंचने पर उल्टे पूछ बैठता, जब जग सारा फिल्मी है तो कविता क्यों न हो! वह सही कहता था क्या? उससे मेरी पहली मुलाकात 'दीवाना' नामकरण के वर्षों बाद हुई थी। गीत-गौनई जैसा बोलचाल में भी सुरीला, अत्यंत मधुर, मीठा-मीठा। मंच पर अपनी हल्की-फुल्की (वही फिल्मी टाइप) मोहब्बताना कविताएं गा-गाकर छा जाया करता। बात 1989 की है। एक दिन हम दोनो को एक साथ गोरखपुर आकाशवाणी से बुलावा आ गया, जुगानी भाई का (उनका भी नाम कुछ और)। कविता पढ़ने के लिए। कई दिन बाद जिस शाम उसका प्रसारण हो रहा था, एक ही ट्रांजिस्टर पर हम दोनो साथ अपने कविता पाठ सुनने के लिए काने साधे बैठ लिए। घर-पड़ोस के भी दो चार जन। दीवाना ने कूद-कूद कर सबको बता दिया था। पहले दीवाना की कविता प्रसारित हुई। मंच की तरह यहां भी वह छा गया। लेकिन, मेरी कविता प्रसारित होने से पहले उद्घोषक ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि दीवाना का दिल बैठ गया। उसी दिन से मित्रता में ईर्ष्या का विष घुल गया। उद्घोषक की टिप्पणी उस वक्त तो मेरे मन को बड़ी सुखद सी लगी थी लेकिन मित्र बुझा बुझा सा रहने लगा। मेरी कविता भी कोई ऐसी नहीं थी कि उसे उतना सराहा जाता, वह भी मेरे मित्र की कविता से तुलना करते हुए। और, उस दिन के बाद से मेरा वह अत्यंत आत्मीय मित्र दूर-दूर रहने लगा छिटक-विदक कर। मेरे एकांत कोलाहल से फिसलता हुआ।... मुझसे खो गया।
संयोग वशदस-ग्यारह वर्षों बाद वह एक दिन वाराणसी में 'आज' अखबार के मुख्यालय के बाहर मिल गया। दोनो दौड़कर मिले। जैसे पहले कुछ हुआ ही न हो। बगल की दुकान पर बैठ लिए। चाय पी, कहां थे, कैसे रहे, एक दूसरे से पूछते, बतियाते रहे। भरी-भरी आंखों से एक दूसरे का सम्मान किया। घंटों अतीत में खोये। अब हम वो फांकामस्त दोस्त नहीं रह गए थे, अब अपनी-अपनी तरह के दुनियादार, अपने-अपने घर-परिवार वाले। कविताओं की वह अल्हड़, साझा दुनिया कहीं पीछे छूटी रह गई थी। आगे-पीछे, दाएं-बाएं सिर्फ रोजी-रोटी के शोर-शराबा, भागमभाग। दीवाना बहुत दुखी था उस दिन। आवाज का वह सुरीलापन भी अनसुना सा, खुरदरे शब्दों से बोझिल, परेशान, माथे पर कई-कई दोहरी सिलवटें। मन के किसी कोने में शायद मुझसे कुछ उम्मीद भी। उस दिन उसे लगा होगा कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूं। उसे नहीं मालूम था कि मैं स्वयं उससे अधिक परेशान था। मैं मन से चाह कर भी उसका कोई सहयोग उस दिन नहीं कर सका। इस तरह मुद्दत बाद बरामद हुई मित्रता फिर धरी रह गयी थी। लेकिन उसके लगभग दो साल बाद एक वक्त ऐसा आया, जब एक अखबार में उसे अपने साथ काम पर बुला लेने के लिए मैंने उसे जाने कैसे-कैसे, कहां-कहां तलाशा लेकिन वह अपने सभी पुराने ठिकानों के लिए भी अपरिचित हो चुका था। कहीं नहीं मिला। आज तक नहीं। जब भी उसकी याद आती है, लगता है, मित्रों की इस छोटी सी दुनिया में अपने खोये दोस्त का दुख साझा न कर पाना भी कृतघ्ना हो सकती है। लगभग चार दशक पहले आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित हुई 'सावन की विरहिणी' पर उसकी भोजपुरी कविता की पहली पंक्ति थी - 'डोले बयरिया से अमवा की डरिया, चुनरिया पिउ की डगर बनि जाय...।'
संयोग वशदस-ग्यारह वर्षों बाद वह एक दिन वाराणसी में 'आज' अखबार के मुख्यालय के बाहर मिल गया। दोनो दौड़कर मिले। जैसे पहले कुछ हुआ ही न हो। बगल की दुकान पर बैठ लिए। चाय पी, कहां थे, कैसे रहे, एक दूसरे से पूछते, बतियाते रहे। भरी-भरी आंखों से एक दूसरे का सम्मान किया। घंटों अतीत में खोये। अब हम वो फांकामस्त दोस्त नहीं रह गए थे, अब अपनी-अपनी तरह के दुनियादार, अपने-अपने घर-परिवार वाले। कविताओं की वह अल्हड़, साझा दुनिया कहीं पीछे छूटी रह गई थी। आगे-पीछे, दाएं-बाएं सिर्फ रोजी-रोटी के शोर-शराबा, भागमभाग। दीवाना बहुत दुखी था उस दिन। आवाज का वह सुरीलापन भी अनसुना सा, खुरदरे शब्दों से बोझिल, परेशान, माथे पर कई-कई दोहरी सिलवटें। मन के किसी कोने में शायद मुझसे कुछ उम्मीद भी। उस दिन उसे लगा होगा कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूं। उसे नहीं मालूम था कि मैं स्वयं उससे अधिक परेशान था। मैं मन से चाह कर भी उसका कोई सहयोग उस दिन नहीं कर सका। इस तरह मुद्दत बाद बरामद हुई मित्रता फिर धरी रह गयी थी। लेकिन उसके लगभग दो साल बाद एक वक्त ऐसा आया, जब एक अखबार में उसे अपने साथ काम पर बुला लेने के लिए मैंने उसे जाने कैसे-कैसे, कहां-कहां तलाशा लेकिन वह अपने सभी पुराने ठिकानों के लिए भी अपरिचित हो चुका था। कहीं नहीं मिला। आज तक नहीं। जब भी उसकी याद आती है, लगता है, मित्रों की इस छोटी सी दुनिया में अपने खोये दोस्त का दुख साझा न कर पाना भी कृतघ्ना हो सकती है। लगभग चार दशक पहले आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित हुई 'सावन की विरहिणी' पर उसकी भोजपुरी कविता की पहली पंक्ति थी - 'डोले बयरिया से अमवा की डरिया, चुनरिया पिउ की डगर बनि जाय...।'
Wednesday 28 February 2018
मुंह पर पचारा पोते भांग में टुन्न सुदामा चाचा
जब भी होली के दिन आते हैं, नानी की यादें आंखें नम कर देती हैं। नानी मां के कच्चे मकान के सामने जन-मानुस जैसे बूढ़े बरगद और नीम-जामुन के तितर-बितर पेड़। पिछवाड़े बंसवारी की बगल में प्रायः बबूल के फूल ओढ़े छोटा-सा घूरा। आसपास की जमीन पर हरे-हरे गमछे की तरह गहरी जड़ों वाले दूब के चकत्ते। घूरता हूं उस वक्त की मटमैली चादर पर। हल्के झोकों से खेलते रहने वाले तृण-पतवार और गन्ना पेराई के दिनों वाले खोई के बिछौने अपनी बांहों में भर लेते हैं मुझे। प्राण रो उठते हैं। इस तरह घुल-मिल जाता है मन उनमें, कि जैसे कोई अबोध शिशु अपनी झीनी-झीनी दंतुलियां दिखाते हुए आंखों में आंखें डालकर डूब जाए उन अविरल क्षणों में। .... और पूछे कि हे जन-मानुसों, लोकजीवन के विकीपीडिया सी वह मेरी नानी मां अभी जिंदा तो नहीं! मेरे बाबा से मुझे आखिरी एक और मुलाकात करा दोगे क्या, जिन्होंने उंगलियां पकड़ कर चलना सिखाया था मुझे। मेरे मन, मेरे विवेक पर अमिट छाप सतर गयी थी जिनकी।
मेरे ननिहाल टिसौरा से पांच-छह किलो मीटर दक्षिण में भैंसही नदी के पार पड़ता था, मेरे पिता का गांव बभनवली। वह होली का दिन था। भांग छानकर मस्त गांव के बड़े-बुजुर्ग बसंत पंचमी से ही देर-देर रात तक समूह में होली गायन में डूब जाया करते थे। होली के दिन वह उल्लास अथाह हो जाता था। मेरे पिता ढोलक-झाल की गमक पर होली-चैता गाने में मशहूर थे। उस दिन भी गाना-बजाना चल रहा था। पूरे गांव पर रंग बरस रहे थे। थाप गूंज रहे थे चारो ओर। हर कोई बेसुध, बौराया सा। कोई रंग, कोई कीचड़, कोई धूल सना बदरंग चेहरा। उसी गहमागहमी, उछल-कूद में मस्तमौला मेरे रिश्ते के सुदामा चाचा बगल के गांव कम्हरिया से दोपहर को अचानक आ टपके। वह अपने घुमंतूपन के लिए चर्चित थे। शाम को जाते-जाते मुझसे पूछने लगे - 'चलोगो अपनी नानी से मिलने! मैं टिसौरा जा रहा हूं।' इतना सुनते ही मैं जोर-जोर से रोने लगा। नानी की याद ने अंदर तक ऐंठ दिया। तुरंत उनके साथ साइकिल से जाने को तैयार हो गए। मैंने अपनी छोटी बहन आशा से पूछा- तुम भी चलोगी मेरी नानी के घर? उसने मना कर दिया और चुपचाप लौट गई। मैं सुदामा चाचा के साथ साइकिल से टिसौरा चला गया।
इधर, होली की रंग-तरंग थमते ही मेरी ढूंढ मची। पिता जी के साथ ही घर-गांव के लोग कुंआ, ताल, पोखरे तक देख-घूम आए, मेरा कहीं पता नहीं चला। घर में कोहराम मच गया। पिता जी हलवाहे मोदी के साथ आधी रात बाद टिसौरा पहुंचे। उस समय सुदामा चाचा दरवाजे पर चारपाई डालकर खर्राटे भर रहे थे। खटर-पटर पर नींद उचटते ही पिता जी को देखा तो कूदकर पिछवाड़े की ओर भाग गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी थी कि मुझे ही खोजते हुए पिता जी उतनी रात गए आ धमके थे। अगली सुबह रोज की तरह मैं सोकर उठा तो दालान की चौखट पर जा बैठा था। नानी मां आकर बुदबुदाते हुए दुखी मन से मेरी पीठ सहलाने लगीं - 'अरे मेरे लाल, जरा देखें तो पीठ पर घाव तो नहीं लगा है, उसने कसाई की तरह पीठा तुझे।' फिर नानी मां ने बताया कि तुम्हारा बाप रात में मोदी हलवाहे के साथ आया था। जगाकर तुझे बैल की तरह पीटने लगा। इसी तरह तेरी मां तुझे पीटती थी। मैंने उसे बहुत डांटा। तब छोड़ कर गया। वह सुदामा को भी ढूंढ रहा था। वह तो कूद कर अंधेरे में पिछवाड़े जा छिपा था। फिर काफी देर तक वह मेरी पीठ और सर सहलाती रही थीं। मुझे जरा भी याद नहीं रहा था कि रात में मेरी जमकर थुराई हो चुकी थी। मुंह पर पचारा पोते भांग में टुन्न सुदामा चाचा तड़के ही डर के मारे चुपचाप साइकिल से अपने गांव लौट गए थे।
मेरे ननिहाल टिसौरा से पांच-छह किलो मीटर दक्षिण में भैंसही नदी के पार पड़ता था, मेरे पिता का गांव बभनवली। वह होली का दिन था। भांग छानकर मस्त गांव के बड़े-बुजुर्ग बसंत पंचमी से ही देर-देर रात तक समूह में होली गायन में डूब जाया करते थे। होली के दिन वह उल्लास अथाह हो जाता था। मेरे पिता ढोलक-झाल की गमक पर होली-चैता गाने में मशहूर थे। उस दिन भी गाना-बजाना चल रहा था। पूरे गांव पर रंग बरस रहे थे। थाप गूंज रहे थे चारो ओर। हर कोई बेसुध, बौराया सा। कोई रंग, कोई कीचड़, कोई धूल सना बदरंग चेहरा। उसी गहमागहमी, उछल-कूद में मस्तमौला मेरे रिश्ते के सुदामा चाचा बगल के गांव कम्हरिया से दोपहर को अचानक आ टपके। वह अपने घुमंतूपन के लिए चर्चित थे। शाम को जाते-जाते मुझसे पूछने लगे - 'चलोगो अपनी नानी से मिलने! मैं टिसौरा जा रहा हूं।' इतना सुनते ही मैं जोर-जोर से रोने लगा। नानी की याद ने अंदर तक ऐंठ दिया। तुरंत उनके साथ साइकिल से जाने को तैयार हो गए। मैंने अपनी छोटी बहन आशा से पूछा- तुम भी चलोगी मेरी नानी के घर? उसने मना कर दिया और चुपचाप लौट गई। मैं सुदामा चाचा के साथ साइकिल से टिसौरा चला गया।
इधर, होली की रंग-तरंग थमते ही मेरी ढूंढ मची। पिता जी के साथ ही घर-गांव के लोग कुंआ, ताल, पोखरे तक देख-घूम आए, मेरा कहीं पता नहीं चला। घर में कोहराम मच गया। पिता जी हलवाहे मोदी के साथ आधी रात बाद टिसौरा पहुंचे। उस समय सुदामा चाचा दरवाजे पर चारपाई डालकर खर्राटे भर रहे थे। खटर-पटर पर नींद उचटते ही पिता जी को देखा तो कूदकर पिछवाड़े की ओर भाग गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी थी कि मुझे ही खोजते हुए पिता जी उतनी रात गए आ धमके थे। अगली सुबह रोज की तरह मैं सोकर उठा तो दालान की चौखट पर जा बैठा था। नानी मां आकर बुदबुदाते हुए दुखी मन से मेरी पीठ सहलाने लगीं - 'अरे मेरे लाल, जरा देखें तो पीठ पर घाव तो नहीं लगा है, उसने कसाई की तरह पीठा तुझे।' फिर नानी मां ने बताया कि तुम्हारा बाप रात में मोदी हलवाहे के साथ आया था। जगाकर तुझे बैल की तरह पीटने लगा। इसी तरह तेरी मां तुझे पीटती थी। मैंने उसे बहुत डांटा। तब छोड़ कर गया। वह सुदामा को भी ढूंढ रहा था। वह तो कूद कर अंधेरे में पिछवाड़े जा छिपा था। फिर काफी देर तक वह मेरी पीठ और सर सहलाती रही थीं। मुझे जरा भी याद नहीं रहा था कि रात में मेरी जमकर थुराई हो चुकी थी। मुंह पर पचारा पोते भांग में टुन्न सुदामा चाचा तड़के ही डर के मारे चुपचाप साइकिल से अपने गांव लौट गए थे।
Tuesday 27 February 2018
जाने कहां खो गई प्रसाद जी की वह पांडुलिपि
कभी-कभी कोई-कोई पश्चाताप जीवन भर पीछा करता रहता है। एक ऐसा ही वाकया मेरे भी अतीत का हिस्सा रहा है। दरअसल, एक मित्र 'पिंक' को सराहते हुए मुझे भी सिनेमाहाल खींच ले गए। लौटते समय 'वह वाकया' घुमड़ने लगा। साहित्य और सिनेमा पर दिमाग दौड़ते-दौड़ते पहुंच गया जयशंकर प्रसाद एवं मुंशी प्रेमचंद से जुड़े एक पांडुलिपि प्रकरण पर। उन दिनो मैं 'आज' अखबार आगरा में कार्यरत था। वहां के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी पीठ में एक प्रोफेसर थे त्रिवेदीजी। उनके आकस्मिक देहावसान के बाद उनके चार बच्चों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया। सबसे बड़ी बेटी थी। मृत्यु के बाद नेपाल में कार्यरत रहे एक प्रोफेसर की निगाह त्रिवेदीजी के अथाह संग्रहालय पर जा टिकी। वह त्रिवेदीजी की बेटी से संग्रहालय की समस्त पुस्तकें, पांडुलिपियां आदि खरीदना चाहते थे। संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपियां थीं।
एक व्यक्ति त्रिवेदीजी के बेटे को नौकरी लगवाने के लिए आज अखबार के कार्यालय ले आया। उसे प्रशिक्षित करने के लिए मेरे हवाले कर दिया गया। उसने एक दिन बताया कि उसकी बहन पापा की सारी किताबें बेचने वाली है। फिर पूरा वाकया बताया। अगले दिन मैं उसके घर गया। उस घरेलू संग्रहालय में एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली। त्रिवेदीजी की बेटी ने बताया कि पापा को इसे कवि जयशंकर प्रसाद ने टाइप करवाकर छपवाने के लिए दिया था। आग्रहकर वह पांडुलिपि मैं इस उद्देश्य से ले आया कि अगर कहीं नेपाल वाले प्रोफेसर इसे ले गये तो इस दुर्लभ सामग्री का जाने क्या हाल हो। मैंने वह पांडुलिपि आगरा विश्वविद्यालय के एक मित्र प्रोफेसर को देखने के लिए दी। उन्होंने उसे कुलपति को दिखाने के बहाने लापता कर दिया।
लंबे समय तक लौटाने का आग्रह करता, पर मिली नहीं। अब तो वह प्रोफेसर भी इस दुनिया में नहीं रहे। उस पांडुलिपि में हिंदी के अनेकशः शीर्ष साहित्यकारों (प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, निरालाजी, नंददुलारे वाजपेयी, पंत आदि) के जयशंकर प्रसाद से हुए पत्राचार की मूल प्रतियां थीं। उसी में एक लंबा पत्र मुंशी प्रेमचंद का था, जो उन्होंने बंबई (मुंबई) की फिल्मी दुनिया से लौटने के बाद लिखा था। काश, वह पांडुलिपि प्रकाशित होकर हिंदी पाठकों को उपलब्ध हो पाती। वह दुख आज तक टीसता है।
एक व्यक्ति त्रिवेदीजी के बेटे को नौकरी लगवाने के लिए आज अखबार के कार्यालय ले आया। उसे प्रशिक्षित करने के लिए मेरे हवाले कर दिया गया। उसने एक दिन बताया कि उसकी बहन पापा की सारी किताबें बेचने वाली है। फिर पूरा वाकया बताया। अगले दिन मैं उसके घर गया। उस घरेलू संग्रहालय में एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली। त्रिवेदीजी की बेटी ने बताया कि पापा को इसे कवि जयशंकर प्रसाद ने टाइप करवाकर छपवाने के लिए दिया था। आग्रहकर वह पांडुलिपि मैं इस उद्देश्य से ले आया कि अगर कहीं नेपाल वाले प्रोफेसर इसे ले गये तो इस दुर्लभ सामग्री का जाने क्या हाल हो। मैंने वह पांडुलिपि आगरा विश्वविद्यालय के एक मित्र प्रोफेसर को देखने के लिए दी। उन्होंने उसे कुलपति को दिखाने के बहाने लापता कर दिया।
लंबे समय तक लौटाने का आग्रह करता, पर मिली नहीं। अब तो वह प्रोफेसर भी इस दुनिया में नहीं रहे। उस पांडुलिपि में हिंदी के अनेकशः शीर्ष साहित्यकारों (प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, निरालाजी, नंददुलारे वाजपेयी, पंत आदि) के जयशंकर प्रसाद से हुए पत्राचार की मूल प्रतियां थीं। उसी में एक लंबा पत्र मुंशी प्रेमचंद का था, जो उन्होंने बंबई (मुंबई) की फिल्मी दुनिया से लौटने के बाद लिखा था। काश, वह पांडुलिपि प्रकाशित होकर हिंदी पाठकों को उपलब्ध हो पाती। वह दुख आज तक टीसता है।
Sunday 25 February 2018
चकई कs चकधुम, मकई कs लावा...
जीवन में कभी कोई ऐसा भी वाकया गुजरता है, भुलाए न भूले। वह 1984 की एक शाम थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने एक चाय की दुकान पर तनावग्रस्त बैठा था। चिंता में घिरा सोचते-सोचते गुस्सा आ गया। तुरंत थैले से कापी निकाली और काशी विद्यापीठ, वाराणसी के हिंदी विभाग के रीडर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय कवि डॉ. श्याम तिवारी (अब स्वर्गीय) के नाम लंबा पत्र लिख डाला। दरअसल, कुछ ही घंटे पहले एक नवविवाहित मित्र ने यह कहकर मुझे कहीं और ठिकाना ढूंढ लेने को कहा था कि उनकी पत्नी ऐसा चाहती हैं। उस वक्त मेरी जेब में चार आने थे। जाऊं तो कहां जाऊं। बड़ी तेज भूख लगी थी। सोचने लगा, चार आने में चाय पीने से भूख कम होगी या चना खाने से। खुद पर कोफ्त। चना लिया। चबाते हुए तिवारी जी को कुछ इस तरह चिट्ठी लिखने लगा- 'निराला को कक्षाओं में पढ़ाना, मंचों पर बखानना बड़ा आसान होता होगा, निराला की तरह एक दिन भी जीना बहुत मुश्किल है, ऐसा मैं निराला के शहर में इस शाम महसूस रहा। ....' पत्र पूरा करने के बाद अनायास दो पंक्तियां मन से निकलीं -
'जब थके आदमी को ढोता हूं,
सोचता हूं, उदास होता हूं,
वक्त थोड़ा-सा गुदगुदाता है,
खूब हंसता हूं, खूब रोता हूं।...'
फिर तो भूख के मारे बरबस फूट पड़े शब्द जाने किधर-किधर ले जाने लगे। उस शाम के कई दशक बाद। उस वक्त मैं वाराणसी अमर उजाला में था। रात की नौकरी। गर्मी की दोपहर मुंह ढंके गहरी नींद में था। तभी किसी ने मेरे चेहरे से गमछा खींच दिया। उनका चेहरा भी गमछे से ढंका था। कोई और नहीं, वह डॉ. श्याम तिवारी थे। दरअसल, उस सुंदरपुर मोहल्ले के जिस मकान में मैं रहता था, उसके मालिक बाल-साहित्यकार थे। उनसे ही तिवारी जी को मेरे बारे में पता चला था। मेरे चेहरे से गमछा खींचने के बाद उन्होंने मुझे मीठी झिड़की दी। चपत मारी। पहचानते ही मैं अगले पल चारपाई से उछल कर खड़ा हो गया। उन्हें आदर से बैठाया। घड़े से ठंडा पानी पिलाया।
वह डाट पिलाते हुए बोले- 'बनारस में तुम्हे किराए के मकान में रहने की क्या जरूरत थी?'
वह एक वक्त में मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे। अस्सी के उस अपने मंदिराकार मकान में प्रायः साथ ले जाते, ढुंडा (मेवा मिश्रित सत्तू का लड्डू) और छाछ का नाश्ता, फिर भोजन कराते। और शाम होते ही साथ लेकर मेरे लिए नौकरी की तलाश में अखबारों के दफ्तरों के चक्कर लगाने निकल पड़ते। उनकी लाख कोशिश अकारथ गई। और एक दिन शहर छोड़ना पड़ा।
उस दोपहर भी कड़ी धूप के बावजूद वह मुझे अपने साथ घर घसीट ले गए थे। वहीं छाछ-ढुंडे का नाश्ता, बीच में इलाहाबाद वाली चिट्ठी पर चुहल। आज भी उनकी यादें आंख गीली कर जाती हैं। डॉ. श्याम तिवारी ध्वन्यात्मक कविताएं जब मंचों से सुनाते थे- श्रोता एक-एक पंक्ति में ताल देने लगते थे.... 'चकई कs चकधुम, मकई कs लावा...'
'जब थके आदमी को ढोता हूं,
सोचता हूं, उदास होता हूं,
वक्त थोड़ा-सा गुदगुदाता है,
खूब हंसता हूं, खूब रोता हूं।...'
फिर तो भूख के मारे बरबस फूट पड़े शब्द जाने किधर-किधर ले जाने लगे। उस शाम के कई दशक बाद। उस वक्त मैं वाराणसी अमर उजाला में था। रात की नौकरी। गर्मी की दोपहर मुंह ढंके गहरी नींद में था। तभी किसी ने मेरे चेहरे से गमछा खींच दिया। उनका चेहरा भी गमछे से ढंका था। कोई और नहीं, वह डॉ. श्याम तिवारी थे। दरअसल, उस सुंदरपुर मोहल्ले के जिस मकान में मैं रहता था, उसके मालिक बाल-साहित्यकार थे। उनसे ही तिवारी जी को मेरे बारे में पता चला था। मेरे चेहरे से गमछा खींचने के बाद उन्होंने मुझे मीठी झिड़की दी। चपत मारी। पहचानते ही मैं अगले पल चारपाई से उछल कर खड़ा हो गया। उन्हें आदर से बैठाया। घड़े से ठंडा पानी पिलाया।
वह डाट पिलाते हुए बोले- 'बनारस में तुम्हे किराए के मकान में रहने की क्या जरूरत थी?'
वह एक वक्त में मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे। अस्सी के उस अपने मंदिराकार मकान में प्रायः साथ ले जाते, ढुंडा (मेवा मिश्रित सत्तू का लड्डू) और छाछ का नाश्ता, फिर भोजन कराते। और शाम होते ही साथ लेकर मेरे लिए नौकरी की तलाश में अखबारों के दफ्तरों के चक्कर लगाने निकल पड़ते। उनकी लाख कोशिश अकारथ गई। और एक दिन शहर छोड़ना पड़ा।
उस दोपहर भी कड़ी धूप के बावजूद वह मुझे अपने साथ घर घसीट ले गए थे। वहीं छाछ-ढुंडे का नाश्ता, बीच में इलाहाबाद वाली चिट्ठी पर चुहल। आज भी उनकी यादें आंख गीली कर जाती हैं। डॉ. श्याम तिवारी ध्वन्यात्मक कविताएं जब मंचों से सुनाते थे- श्रोता एक-एक पंक्ति में ताल देने लगते थे.... 'चकई कs चकधुम, मकई कs लावा...'
पत्र-कार, मालिक का तलवा और चमचों की पंचाट
घुड़की भी एक कला है। इसके कई रूप हैं। रोब-रुतबे का प्रदर्शन घुड़की है। मैंने ऐसे घुड़कीबाज नामवरों को मीडिया की दुनिया में बहुत करीब से देखा-भोगा है। अखबार या न्यूज चैनल के सिरहाने बैठे हैं। अपने नखरों के मारे हुए ऐसे कई नामवरों को शब्द तो दुत्कार-खदेड़ देते हैं। फिर वे घुड़की, रुतबे, नाज-नखरें से काम चलाते हैं। साहब को खबरें लिखने नहीं आता तो क्या, घुड़की है न। काम चल जाता हैं। लिखने-पढ़ने से क्या वास्ता। पत्र-कार हैं, पत्र का तमगा है, कार है, चमचों की पंचाट है, नौकर-चाकर हैं और गुदगुदाने के लिए मालिक के तलवे हैं...बस नौकरी चल निकलती है।
Friday 23 February 2018
आजकल तो सबसे ज्यादा कविता नहीं, चुटकले पढ़े जा रहे - नरेश सक्सेना
प्रतिष्ठित कवि नरेश सक्सेना कहते हैं- कविता के कम या अधिक पढ़े जाने के प्रश्न का जवाब हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता क्योंकि हां और ना, दोनों जवाब सही हैं। इस पर लंबी बहस है, फिर कभी बात होगी। ध्यान देने की बातें और हैं। कविता, गीत जो है, सोचिए, छंद में कविता कौन लिखता है और कौन पढ़ता है, कौन लेखक है, कितने उसके पढ़ने वाले हैं? जब से कविता छंद से बाहर आ गई है, जितनी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, उनमें ज्यादातर में गीत न कहीं छपता है, न पढ़ी जाती हैं। सरिता, कादंबिनी आदि को छोड़कर, बहुत कम जगहें हैं, जहां ऐसी कविताएं छपती हैं। वैसे ऐसी पत्रिकाएं रह भी नहीं गई हैं, जो गीत-वीत छापती रही हैं। अब सोचिए कि जब गीत छपता नहीं तो पढ़ा कैसे जाए! मंच के एक कवि अपनी एक कविता चालीस साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते बूढ़े हो चले, उस तरह के गीत अब छपते नहीं हैं। आज लिखे जाएं तो छापे नहीं जाते। छंदमुक्त कविताएं भी पढ़ी जाती हैं। अच्छी कविताएं कम संख्या में लिखी जाती हैं, उसके पाठक वही हैं, जो लिखते हैं, जो लेखक हैं। मुख्यतः ऐसी कविताओं के नॉन राइटर पाठक कम हैं, गिने-चुने। छंदमुक्त कविताएं भी ज्यादातर ठीक नहीं होतीं, इसलिए भी पाठक कम रह गए हैं। वह जमाना और था, जब मेरे गीत रंगीन पृष्ठों पर छपते थे, पूरे-पूरे पेज पर। जहां तक अच्छी कविता का प्रश्न है, अब छंद के बाहर ही अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, फिर भी पूरा साहित्य मंगलेश डबराल या राजेश जोशी का खंगाल लेंगे तो दस-बीस ही अच्छी कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। पढ़ी फिर भी कविता इसलिए ज्यादा जाती है कि वह फटाक से पढ़ ली जाती है। बाकी साहित्य की अपेक्षा कविता जल्दी पढ़ ली जाती है। यह आसान है। आसानी से पढ़ ली जाती है। कहानीकार भी कविता पढ़ लेता है, लेकिन हर कवि उतनी आसानी से कहानी पढ़ने के लिए स्वयं को सहजतः तैयार नहीं कर पाता है। जहां तक कविता के अच्छा या खराब होने की बात है, कविता होती है या नहीं होती है। वह आसान नहीं होती है- 'शेर अच्छा-बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता।' ग़ज़लों में आजकल रिपिटीशन बहुत हो रहा है। नई बात कम होती है। छंद में वे ही कवि पढ़े जा रहे हैं, जो जैसे नीरज आदि, उनकी किताबें छपती भी हैं, बिकती भी है, बाकी किसकी छपती हैं, किसकी बिकती हैं! आजकल ज्यादादर कविता की किताबें अपने पैसे से छपवाई जा रही हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा चुटकला पढ़ा जाता है, उसके बाद कविता का नंबर आता है।
वरिष्ठ कवि लीलाधर जगूड़ी कहते हैं - जो कुछ लिखा जा रहा है, क्या वो सच है, जो कुछ पढ़ा जा रहा है क्या वो सच है? सच और झूठ की भीड़ में जाएंगे तो पता चलेगा कि सारे झूठ एक न एक दिन सच होना चाहते हैं। पहले भी जिन्हें हम काल्पनिक झूठ समझते थे, वे आज के यथार्थ बने हुए हैं। उसमें सहायक तत्व स्वयं मनुष्य है और विज्ञान है। इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ा जाना और सबसे कम पढ़ा जाना महत्वपूर्ण नहीं होता, मेरी समझ से सबसे महत्वपूर्ण है किसी का पढ़ा जाना। आज जितनी चीजें सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही हैं, क्या वही सफल मान ली जाएं। सवाल सफलता और असफलता का भी नहीं है, लेकिन उपयोगिता और उपादेयता का तो है। पहले भी कविता बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी जाती रही है, और आज भी कविता बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी जा रही है तो भी यह आश्चर्य होता है कि कविता खराब ही सही, इतनी ज्यादा क्यों लिखी जा रही है? कोई भी रचनात्मक विधा अगर अपने रचनाकारों को कम या ज्यादा मात्रा में पैदा करती है तो यह उस विधा का दोष या कमजोरी नहीं, बल्कि यह रचनाकार की अपनी सुविधा और अपने रुझान पर निर्भर करता है। स्वाद का भी कोई मानदंड नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर साहित्य के रसास्वादन का मानदंड कैसे बनाया जाए। पढ़ने वालों की गिनती से साहित्य ऊंचा नहीं हो जाता है, न लिखने वालों की बढ़ी हुई तादाद से। हो सकता है कि कम ही बहुत ज्यादा लगने लगे। और ये भी संभव है कि बहुत ज्यादा कम दिखने लगे। जितनी भी जटिल प्रक्रिया और व्यापक अनुभव वाली चीजें होती हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए भी एक जटिल और व्यापक अनुभव चाहिए। जिस पाठक का जैसा स्वभाव, जैसी तितीक्षा होगी, उसे अपने स्वाद के अनुसार रचनात्मक संसार में जाने का अवसर मिलेगा। यह अलग बात है कि कितने कवि हैं, जो कविता जैसी कविता नहीं लिख रहे हैं बल्कि कुछ अलग ढंग की कविताएं लिख रहे हैं, और कितने लोग हैं, जो इस खूबी को जानते पहचानते और खोजते हैं। कविता कोई महामारी नहीं है, जिसकी चपेट में सब लोग आ जाएं।
वरिष्ठ कवि लीलाधर जगूड़ी कहते हैं - जो कुछ लिखा जा रहा है, क्या वो सच है, जो कुछ पढ़ा जा रहा है क्या वो सच है? सच और झूठ की भीड़ में जाएंगे तो पता चलेगा कि सारे झूठ एक न एक दिन सच होना चाहते हैं। पहले भी जिन्हें हम काल्पनिक झूठ समझते थे, वे आज के यथार्थ बने हुए हैं। उसमें सहायक तत्व स्वयं मनुष्य है और विज्ञान है। इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ा जाना और सबसे कम पढ़ा जाना महत्वपूर्ण नहीं होता, मेरी समझ से सबसे महत्वपूर्ण है किसी का पढ़ा जाना। आज जितनी चीजें सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही हैं, क्या वही सफल मान ली जाएं। सवाल सफलता और असफलता का भी नहीं है, लेकिन उपयोगिता और उपादेयता का तो है। पहले भी कविता बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी जाती रही है, और आज भी कविता बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी जा रही है तो भी यह आश्चर्य होता है कि कविता खराब ही सही, इतनी ज्यादा क्यों लिखी जा रही है? कोई भी रचनात्मक विधा अगर अपने रचनाकारों को कम या ज्यादा मात्रा में पैदा करती है तो यह उस विधा का दोष या कमजोरी नहीं, बल्कि यह रचनाकार की अपनी सुविधा और अपने रुझान पर निर्भर करता है। स्वाद का भी कोई मानदंड नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर साहित्य के रसास्वादन का मानदंड कैसे बनाया जाए। पढ़ने वालों की गिनती से साहित्य ऊंचा नहीं हो जाता है, न लिखने वालों की बढ़ी हुई तादाद से। हो सकता है कि कम ही बहुत ज्यादा लगने लगे। और ये भी संभव है कि बहुत ज्यादा कम दिखने लगे। जितनी भी जटिल प्रक्रिया और व्यापक अनुभव वाली चीजें होती हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए भी एक जटिल और व्यापक अनुभव चाहिए। जिस पाठक का जैसा स्वभाव, जैसी तितीक्षा होगी, उसे अपने स्वाद के अनुसार रचनात्मक संसार में जाने का अवसर मिलेगा। यह अलग बात है कि कितने कवि हैं, जो कविता जैसी कविता नहीं लिख रहे हैं बल्कि कुछ अलग ढंग की कविताएं लिख रहे हैं, और कितने लोग हैं, जो इस खूबी को जानते पहचानते और खोजते हैं। कविता कोई महामारी नहीं है, जिसकी चपेट में सब लोग आ जाएं।
Thursday 22 February 2018
नागार्जुन का गुस्सा और त्रिलोचन का ठहाका
घर का नाम 'वैद्यनाथ मिश्र', साहित्यक नाम 'नागार्जुन', मैथिली उपनाम 'यात्री', प्रचलित पूरा नाम 'बाबा नागार्जुन'। रचना के मिजाज में सबसे अलग, अलख निरंजन। बाबा के साथ बीता एक वाकया याद आता है। 1980 के दशक में बाबा से मुलाकात हुई थी जयपुर में। जैसे बाबा, वैसी अनोखी मुलाकात। उस दिन देशभर के प्रगतिशील कवि-साहित्यकार जमा थे गुलाबी नगरी में। अमृत राय, त्रिलोचन, भीष्म साहनी, अब्दुल बिस्मिल्लाह, शिवमूर्ति आदि-आदि। बाबा से मुलाकात की बात बाद में, पहले एक प्रसंगेतर आख्यान।
महापंडित राहुल सांकृत्यायन में मेरी छात्र जीवन से जिज्ञासा रही। इसकी भी एक खास वजह। मेरे गृह-जनपद आजमगढ़ में राहुलजी का गांव कनैला हमारे गांव से सात-आठ किलो मीटर दूर। अगल-बगल के गांवों में रिश्तेदारियां, प्रायः आना-जाना। संयोग वश मैं जिस हरिहरनाथ इंटर कॉलेज, शेरपुर का छात्र रहा, क्लास टीचर पारसनाथ पांडेय राहुलजी के ही गृहग्राम कनैला के। वह क्लास में अक्सर राहुलजी पर तरह-तरह के प्रिय-अप्रिय वृत्तांत सुनाया करते। वह बातें फिर कभी। ....तो जयपुर यात्रा के उन दिनो मैं राहुल सांकृत्यायन पर लिखी एक ऐसी किताब पढ़ रहा था, जिसका संपादन उनकी धर्मपत्नी कमला सांकृत्यायन ने किया था। उस पुस्तक से पहली बार राहुलजी के संबंध में उनके जीवन की तमाम अज्ञात जानकारियां मिली थीं। उस पुस्तक से ही ज्ञात हुआ था कि कमला सांकृत्यायन मसूरी के हैप्पी वैली (उत्तराखंड) इलाके में रहती हैं। बाबा नागार्जुन वहां कभी-कभार जाया-आया करते।
उस दिन जयपुर में जैसे ही मुझे पता चला कि बाबा नागार्जुन भी यहां आए हुए हैं, कमला सांकृत्यायन के बारे में बाबा से और भी जानकारियां प्राप्त कर लेने की मेरी जिज्ञासा बेकाबू हो ली। उस दिन कवि-साहित्यकारों में मुझे कवि त्रिलोचन बड़े सहज लगे, सो किसी बात के बहाने मैं उनके निकट हो लिया। संयोग से हम जहां ठहरे थे, वहीं अगल-बगल के कमरों में त्रिलोचनजी और बाबा नागार्जुन भी रुके हुए थे। दबी जुबान मैंने अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा त्रिलोचनजी से साझा कर ली। सुनते ही पहले तो उनके चेहरे पर मैंने अजीब रंग उभरते देखे, जैसे आंखें अचानक चौकन्नी हो उठीं हों। फिर उन्होंने कुछ पल मुझे गौर से देखा, बोले- 'हां-हां, बाबा से बोलो, वह तुम्हें सब बता देंगे। अगर कमलाजी से मिलना चाहते हो तो मिलवा भी देंगे।' उस वक्त उनके मन का आशय मैं भला कैसे पढ़ पाता। असल में त्रिलोचनजी आनंद लेने की मुद्रा में आ गए थे। मुझे बाबा से मिलने के लिए उकसाते समय उन्होंने मान लिया था कि इसकी कोई न कोई मजेदार प्रतिक्रिया जरूर होगी। मुझे बाबा के पास भेजकर वह बगल के कमरे में अन्य लेखकों के बीच जा बैठे। कानाफूसी होने लगी लेकिन उनके कान मेरी तरफ सधे हुए।
ठीक उसी समय बाबा तेजी से हमारे बगल के अपने कमरे से बाहर निकले। मैंने उन्हें रोकते हुए तपाक से पूछा - 'बाबा मुझे कमला सांकृत्यायन के बारे में आप से कुछ बात करनी है।' सुनते ही बाबा ऐसे चिग्घाड़ उठे कि मेरे कमरे से जोर का ठहाका गूंजा। दरअसल, त्रिलोचनजी तब तक इस बारे में अंदर कमरे में बैठे अन्य लेखकों को सब कुछ बता चुके थे और प्रतिक्रिया होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका उकसावा ठीक निशाने पर बैठा था। मेरी बात सुनते ही बाबा ने तिलमिलाते हुए कहा- 'मैं क्या जानूं कमला-समला को.... चले आते हैं पता नहीं कहां-कहां से, न जाने कैसी-कैसी बातें करते हुए।' एक बात और। उस वक्त बाबा बॉथरूम जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वह पेटझरी (लूज मोशन) से पीड़ित थे। उन्हें तेजी से बॉथरूम जाते वक्त रोककर मैंने उन्हें क्षुब्ध कर दिया था, सो उससे भी वह तिलमिला उठे थे।
बाबा की फटकार पाकर मैं जैसे ही अंदर अपने कमरे में पहुंचा, वहां ठाट जमाए सभी लेखक महामनाओं की निगाहें मेरे ऊपर आ जमीं। त्रिलोचनजी ने बड़े स्नेह से (ठकुर सुहाती अंदाज में) मेरा माथा सहलाते हुए पूछा- 'क्या हो गया बेटा, बाबा नाराज हो गए क्या?' मेरे कंठ से कोई आवाज ही न फूटे। चुप। मेरी आंख भर आई थी। गला रुंध सा गया। अब बाबा के गुस्से और लेखकों के ठहाके का मर्म बताते हैं। उन दिनो बाबा सचमुच कमला सांकृत्यायन से नाखुश चल रहे थे। उन्हीं लेखक 'गुरुओं' में से एक ने बताया था कि कुछ माह पहले ही की बात है। बाबा कमलाजी के ठिकाने पर हैप्पी वैली, मसूरी गए थे। कमला जी ने उन्हें फटकार कर दोबारा वहां आने से मना कर दिया था। जिस वक्त मैंने बाबा से पूछा, एक तो पहले से कमलाजी से नाखुशी, दूसरे पेटझरी की पीड़ा से उनका मिजाज बेकाबू हो उठा था। वैसे भी वह स्वभाव से तुनक मिजाजी थे। इस पर मैं जब बाद में त्रिलोचनजी से बात करनी चाही, वह मुसकरा कर चुप रह गए थे। अब आइए, अकाल पर बाबा नागार्जुन की एक सबसे चर्चित कविता पढ़ते हैं -
कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास।
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास।
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त,
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद,
धुआँ उठा आँगन से ऊपर कई दिनों के बाद।
चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद,
कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद।
साहित्य में बाबा कालजयी रचनाओं के शीर्ष कवि रहे हैं। निराला और कबीर की तरह। उनके शब्द आज भी जन-गण-मन में लोकप्रिय हैं। वह संस्कृत के विद्वान तो थे ही, मैथिली, पालि, प्राकृत, बांग्ला, सिंहली, तिब्बती आदि अनेकानेक भाषाओं के भी ज्ञाता थे। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में उनकी लेखनी आजीवन कुलाचें भरती रही। राहुल, निराला, त्रिलोचन की तरह उन्होंने भी जीवन में कत्तई बड़े से बड़े सरकारी प्रलोभनों से परहेज किया। उनके भी अंतिम दिन अन्य ईमानदार साहित्यकारों की तरह बड़े अभाव में बीते। उनके काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा जीवंत रूप में उपस्थित है। वह नवगीत, छायावाद से छंदमुक्त कविताओं के तरह-तरह के रचनात्मक दौर के सबसे सक्रिय साक्षी रहे। और बाबा की एक कविता 'मंत्र' -
ॐ शब्द ही ब्रह्म है,
ॐ शब्द और शब्द और शब्द और शब्द
ॐ प्रणव, ॐ नाद, ॐ मुद्राएं
ॐ वक्तव्य, ॐ उदगार, ॐ घोषणाएं
ॐ भाषण...ॐ प्रवचन...
ॐ हुंकार, ॐ फटकार, ॐ शीत्कार
ॐ फुसफुस, ॐ फुत्कार, ॐ चित्कार
ॐ आस्फालन, ॐ इंगित, ॐ इशारे
ॐ नारे और नारे और नारे और नारे
ॐ सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ
ॐ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं
ॐ पत्थर पर की दूब, खरगोश के सींग
ॐ नमक-तेल-हल्दी-जीरा-हींग
ॐ मूस की लेड़ी, कनेर के पात
ॐ डायन की चीख, औघड़ की अटपट बात
ॐ कोयला-इस्पात-पेट्रोल
ॐ हमी हम ठोस, बाकी सब फूटे ढोल
ॐ इदमन्नं, इमा आप:, इदमाज्यं, इदं हवि
ॐ यजमान, ॐ पुरोहित, ॐ राजा, ॐ कवि:
ॐ क्रांति: क्रांति: क्रांति: सर्वग्वं क्रांति:
ॐ शांति: शांति: शांति: सर्वग्वं शांति:
ॐ भ्रांति भ्रांति भ्रांति सर्वग्वं भ्रांति:
ॐ बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ
ॐ हटाओ हटाओ हटाओ हटाओ
ॐ घेराओ घेराओ घेराओ घेराओ
ॐ निभाओ निभाओ निभाओ निभाओ
ॐ दलों में एक दल अपना दल, ओं
ॐ अंगीकरण, शुद्धीकरण, राष्ट्रीकरण
ॐ मुष्टीकरण, तुष्टीकरण, पुष्टीकरण
ॐ एतराज, आक्षेप, अनुशासन
ॐ गद्दी पर आजन्म वज्रासन
ॐ ट्रिब्युनल ॐ आश्वासन
ॐ गुटनिरपेक्ष सत्तासापेक्ष जोड़तोड़
ॐ छल-छंद, ॐ मिथ्या, ॐ होड़महोड़
ॐ बकवास, ॐ उद्घाटन
ॐ मारण-मोहन-उच्चाटन
ॐ काली काली काली महाकाली महाकाली
ॐ मार मार मार, वार न जाए खाली
ॐ अपनी खुशहाली
ॐ दुश्मनों की पामाली
ॐ मार, मार, मार, मार, मार, मार, मार
ॐ अपोजिशन के मुंड बनें तेरे गले का हार
ॐ ऐं हीं वली हूं आङू
ॐ हम चबाएंगे तिलक और गांधी की टांग
ॐ बूढ़े की आंख, छोकरी का काजल
ॐ तुलसीदल, बिल्वपत्र, चंदन, रोली, अक्षत, गंगाजल
ॐ शेर के दांत, भालू के नाखून, मर्कट का फोता
ॐ हमेशा हमेशा हमेशा करेगा राज मेरा पोता
ॐ छू: छू: फू: फू: फट फिट फुट
ॐ शत्रुओं की छाती पर लोहा कुट
ॐ भैरो, भैरो, भैरो, ॐ बजरंगबली
ॐ बंदूक का टोटा, पिस्तौल की नली
ॐ डालर, ॐ रूबल, ॐ पाउंड
ॐ साउंड, ॐ साउंड, ॐ साउंड
ओम् ओम् ओम्
ओम धरती धरती धरती,
व्योम व्योम व्योम.....
महापंडित राहुल सांकृत्यायन में मेरी छात्र जीवन से जिज्ञासा रही। इसकी भी एक खास वजह। मेरे गृह-जनपद आजमगढ़ में राहुलजी का गांव कनैला हमारे गांव से सात-आठ किलो मीटर दूर। अगल-बगल के गांवों में रिश्तेदारियां, प्रायः आना-जाना। संयोग वश मैं जिस हरिहरनाथ इंटर कॉलेज, शेरपुर का छात्र रहा, क्लास टीचर पारसनाथ पांडेय राहुलजी के ही गृहग्राम कनैला के। वह क्लास में अक्सर राहुलजी पर तरह-तरह के प्रिय-अप्रिय वृत्तांत सुनाया करते। वह बातें फिर कभी। ....तो जयपुर यात्रा के उन दिनो मैं राहुल सांकृत्यायन पर लिखी एक ऐसी किताब पढ़ रहा था, जिसका संपादन उनकी धर्मपत्नी कमला सांकृत्यायन ने किया था। उस पुस्तक से पहली बार राहुलजी के संबंध में उनके जीवन की तमाम अज्ञात जानकारियां मिली थीं। उस पुस्तक से ही ज्ञात हुआ था कि कमला सांकृत्यायन मसूरी के हैप्पी वैली (उत्तराखंड) इलाके में रहती हैं। बाबा नागार्जुन वहां कभी-कभार जाया-आया करते।
उस दिन जयपुर में जैसे ही मुझे पता चला कि बाबा नागार्जुन भी यहां आए हुए हैं, कमला सांकृत्यायन के बारे में बाबा से और भी जानकारियां प्राप्त कर लेने की मेरी जिज्ञासा बेकाबू हो ली। उस दिन कवि-साहित्यकारों में मुझे कवि त्रिलोचन बड़े सहज लगे, सो किसी बात के बहाने मैं उनके निकट हो लिया। संयोग से हम जहां ठहरे थे, वहीं अगल-बगल के कमरों में त्रिलोचनजी और बाबा नागार्जुन भी रुके हुए थे। दबी जुबान मैंने अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा त्रिलोचनजी से साझा कर ली। सुनते ही पहले तो उनके चेहरे पर मैंने अजीब रंग उभरते देखे, जैसे आंखें अचानक चौकन्नी हो उठीं हों। फिर उन्होंने कुछ पल मुझे गौर से देखा, बोले- 'हां-हां, बाबा से बोलो, वह तुम्हें सब बता देंगे। अगर कमलाजी से मिलना चाहते हो तो मिलवा भी देंगे।' उस वक्त उनके मन का आशय मैं भला कैसे पढ़ पाता। असल में त्रिलोचनजी आनंद लेने की मुद्रा में आ गए थे। मुझे बाबा से मिलने के लिए उकसाते समय उन्होंने मान लिया था कि इसकी कोई न कोई मजेदार प्रतिक्रिया जरूर होगी। मुझे बाबा के पास भेजकर वह बगल के कमरे में अन्य लेखकों के बीच जा बैठे। कानाफूसी होने लगी लेकिन उनके कान मेरी तरफ सधे हुए।
ठीक उसी समय बाबा तेजी से हमारे बगल के अपने कमरे से बाहर निकले। मैंने उन्हें रोकते हुए तपाक से पूछा - 'बाबा मुझे कमला सांकृत्यायन के बारे में आप से कुछ बात करनी है।' सुनते ही बाबा ऐसे चिग्घाड़ उठे कि मेरे कमरे से जोर का ठहाका गूंजा। दरअसल, त्रिलोचनजी तब तक इस बारे में अंदर कमरे में बैठे अन्य लेखकों को सब कुछ बता चुके थे और प्रतिक्रिया होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका उकसावा ठीक निशाने पर बैठा था। मेरी बात सुनते ही बाबा ने तिलमिलाते हुए कहा- 'मैं क्या जानूं कमला-समला को.... चले आते हैं पता नहीं कहां-कहां से, न जाने कैसी-कैसी बातें करते हुए।' एक बात और। उस वक्त बाबा बॉथरूम जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वह पेटझरी (लूज मोशन) से पीड़ित थे। उन्हें तेजी से बॉथरूम जाते वक्त रोककर मैंने उन्हें क्षुब्ध कर दिया था, सो उससे भी वह तिलमिला उठे थे।
बाबा की फटकार पाकर मैं जैसे ही अंदर अपने कमरे में पहुंचा, वहां ठाट जमाए सभी लेखक महामनाओं की निगाहें मेरे ऊपर आ जमीं। त्रिलोचनजी ने बड़े स्नेह से (ठकुर सुहाती अंदाज में) मेरा माथा सहलाते हुए पूछा- 'क्या हो गया बेटा, बाबा नाराज हो गए क्या?' मेरे कंठ से कोई आवाज ही न फूटे। चुप। मेरी आंख भर आई थी। गला रुंध सा गया। अब बाबा के गुस्से और लेखकों के ठहाके का मर्म बताते हैं। उन दिनो बाबा सचमुच कमला सांकृत्यायन से नाखुश चल रहे थे। उन्हीं लेखक 'गुरुओं' में से एक ने बताया था कि कुछ माह पहले ही की बात है। बाबा कमलाजी के ठिकाने पर हैप्पी वैली, मसूरी गए थे। कमला जी ने उन्हें फटकार कर दोबारा वहां आने से मना कर दिया था। जिस वक्त मैंने बाबा से पूछा, एक तो पहले से कमलाजी से नाखुशी, दूसरे पेटझरी की पीड़ा से उनका मिजाज बेकाबू हो उठा था। वैसे भी वह स्वभाव से तुनक मिजाजी थे। इस पर मैं जब बाद में त्रिलोचनजी से बात करनी चाही, वह मुसकरा कर चुप रह गए थे। अब आइए, अकाल पर बाबा नागार्जुन की एक सबसे चर्चित कविता पढ़ते हैं -
कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास।
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास।
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त,
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद,
धुआँ उठा आँगन से ऊपर कई दिनों के बाद।
चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद,
कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद।
साहित्य में बाबा कालजयी रचनाओं के शीर्ष कवि रहे हैं। निराला और कबीर की तरह। उनके शब्द आज भी जन-गण-मन में लोकप्रिय हैं। वह संस्कृत के विद्वान तो थे ही, मैथिली, पालि, प्राकृत, बांग्ला, सिंहली, तिब्बती आदि अनेकानेक भाषाओं के भी ज्ञाता थे। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में उनकी लेखनी आजीवन कुलाचें भरती रही। राहुल, निराला, त्रिलोचन की तरह उन्होंने भी जीवन में कत्तई बड़े से बड़े सरकारी प्रलोभनों से परहेज किया। उनके भी अंतिम दिन अन्य ईमानदार साहित्यकारों की तरह बड़े अभाव में बीते। उनके काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा जीवंत रूप में उपस्थित है। वह नवगीत, छायावाद से छंदमुक्त कविताओं के तरह-तरह के रचनात्मक दौर के सबसे सक्रिय साक्षी रहे। और बाबा की एक कविता 'मंत्र' -
ॐ शब्द ही ब्रह्म है,
ॐ शब्द और शब्द और शब्द और शब्द
ॐ प्रणव, ॐ नाद, ॐ मुद्राएं
ॐ वक्तव्य, ॐ उदगार, ॐ घोषणाएं
ॐ भाषण...ॐ प्रवचन...
ॐ हुंकार, ॐ फटकार, ॐ शीत्कार
ॐ फुसफुस, ॐ फुत्कार, ॐ चित्कार
ॐ आस्फालन, ॐ इंगित, ॐ इशारे
ॐ नारे और नारे और नारे और नारे
ॐ सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ
ॐ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं
ॐ पत्थर पर की दूब, खरगोश के सींग
ॐ नमक-तेल-हल्दी-जीरा-हींग
ॐ मूस की लेड़ी, कनेर के पात
ॐ डायन की चीख, औघड़ की अटपट बात
ॐ कोयला-इस्पात-पेट्रोल
ॐ हमी हम ठोस, बाकी सब फूटे ढोल
ॐ इदमन्नं, इमा आप:, इदमाज्यं, इदं हवि
ॐ यजमान, ॐ पुरोहित, ॐ राजा, ॐ कवि:
ॐ क्रांति: क्रांति: क्रांति: सर्वग्वं क्रांति:
ॐ शांति: शांति: शांति: सर्वग्वं शांति:
ॐ भ्रांति भ्रांति भ्रांति सर्वग्वं भ्रांति:
ॐ बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ
ॐ हटाओ हटाओ हटाओ हटाओ
ॐ घेराओ घेराओ घेराओ घेराओ
ॐ निभाओ निभाओ निभाओ निभाओ
ॐ दलों में एक दल अपना दल, ओं
ॐ अंगीकरण, शुद्धीकरण, राष्ट्रीकरण
ॐ मुष्टीकरण, तुष्टीकरण, पुष्टीकरण
ॐ एतराज, आक्षेप, अनुशासन
ॐ गद्दी पर आजन्म वज्रासन
ॐ ट्रिब्युनल ॐ आश्वासन
ॐ गुटनिरपेक्ष सत्तासापेक्ष जोड़तोड़
ॐ छल-छंद, ॐ मिथ्या, ॐ होड़महोड़
ॐ बकवास, ॐ उद्घाटन
ॐ मारण-मोहन-उच्चाटन
ॐ काली काली काली महाकाली महाकाली
ॐ मार मार मार, वार न जाए खाली
ॐ अपनी खुशहाली
ॐ दुश्मनों की पामाली
ॐ मार, मार, मार, मार, मार, मार, मार
ॐ अपोजिशन के मुंड बनें तेरे गले का हार
ॐ ऐं हीं वली हूं आङू
ॐ हम चबाएंगे तिलक और गांधी की टांग
ॐ बूढ़े की आंख, छोकरी का काजल
ॐ तुलसीदल, बिल्वपत्र, चंदन, रोली, अक्षत, गंगाजल
ॐ शेर के दांत, भालू के नाखून, मर्कट का फोता
ॐ हमेशा हमेशा हमेशा करेगा राज मेरा पोता
ॐ छू: छू: फू: फू: फट फिट फुट
ॐ शत्रुओं की छाती पर लोहा कुट
ॐ भैरो, भैरो, भैरो, ॐ बजरंगबली
ॐ बंदूक का टोटा, पिस्तौल की नली
ॐ डालर, ॐ रूबल, ॐ पाउंड
ॐ साउंड, ॐ साउंड, ॐ साउंड
ओम् ओम् ओम्
ओम धरती धरती धरती,
व्योम व्योम व्योम.....
घुमंतू कबीलों वाले कवि आनंद परमानंद
वाराणसी के बुजुर्ग कवि आनंद परमानंद ऐसे रचनाकार हैं, जिन पर त्रिलोचन ने भी कविता लिखी। जाने कितने तरह के बोझ मन पर लादे-फादे हुए। अंदर क्या-कुछ घट रहा होता है, जो चुप्पियों से शब्दभर भी फूट नहीं पाता है। जैसे सड़क की भीड़ के बीच कोई अनहद एकांतिकता। भीतर आग, बाहर शब्दों से तप्त झरने फूटते हुए। कभी घंटों स्वयं में गुम, कभी अचानक धारा प्रवाह, राजनीति से साहित्य तक, डॉ.लोहिया से डॉ. शंभुनाथ सिंह तक, गीत-ग़ज़ल से नवगीत तक, अंतहीन, प्रसंगेतर-प्रसंगेतर। साथ का हरएक चुप्पी साधे, विमुग्ध श्रोताभर जैसे।
परमानंद की प्रकांडता का एक आश्चर्यजनक पक्ष है, उनमें संचित जीवंत अथाह स्मृतियां।
शब्द के जोखिम उठाता हूं, तो गीतों के लिए।
दर्द से रिश्ते निभाता हूं, तो गीतों के लिए।
गूंगी पीड़ा को नया शब्दार्थ देने के लिए,
भीड़ में भी छटपटाता हूं, तो गीतों के लिए।
सोचकर खेतों में ये प्रतिबद्धताएं रोपकर,
नये सम्बोधन उगाता हूं, तो गीतों के लिए।
माथ पर उंगली धरे सच्चाइयों के द्वार की,
सांकलें जब खटखटाता हूं, तो गीतों के लिए।
जिनके चेहरों पर हंसी फिर लौटकर आयी नहीं,
उनकी खातिर बौखलाता हूं, तो गीतों के लिए।
ओढ़कर कुहरे पड़ी चुपचाप ठंडी रात में,
पत्तियों सा खड़खड़ाता हूं, तो गीतों के लिए।
मिल गया मौसम सड़क पर जब असभ्यों की तरह,
वक्त को कुछ बड़बड़ाता हूं, तो गीतों के लिए।
जब तक साथ, सोचते रहिए कि ये आदमी है या कोई मास्टर कम्यूटर। भला किसी एक आदमी को इतनी बातें अक्षरशः कैसे याद रह सकती हैं, जबकि उम्र अस्सी के पार, स्मृतिभ्रंश की आशंकाओं से भरी रहती है। दरअसल, आनंद परमानंद दुष्यंत परंपरा के सशक्त ग़ज़लकार हैं। एक जमाने में इनकी ग़ज़लें प्रायः मंचों पर अपना प्रभाव स्थापित करती रही हैं। वह आदमी की तरह जिंदगी काटते हैं। आज तो यह आशंका जन्म लेने लगी है कि सही आदमी सड़क पर भी रह पाएगा अथवा नहीं। आखिर वह जाए भी तो कहां जाए। उनकी ग़ज़लें पढ़कर इस बात पर प्रसन्नता होती है कि कम से कम उन्होंने नकली और बनावटी बातें तो नहीं कही हैं।
कड़ी चिल्लाहटें क्यूं हैं इसी तस्वीर के पीछे।
मरा सच है कहीं फिर क्या उसी प्राचीर के पीछे।
यहां तो बेगुनाहों ने तड़प कर जिंदगी दी है,
खड़ा इतिहास है रोता हुआ जंजीर के पीछे।
बहुत बेआबरू संवेदनाएं जब हुई होंगी,
बड़ी हलचल मची होगी नयन के नीर के पीछे।
कठिन संघर्ष में संभावनाएं जन्म लेती हैं,
इसी उम्मीद में वह है खड़ा शहतीर के पीछे।
समय की झनझनाहट सुन, बराबर काम करते चल,
न लट्टू की तरह नाचा करो तकदीर के पीछे।
कलम जो जिंदगी देगी, कहीं फिर मिल नहीं सकती,
अरे मन अब कभी मत भागना जागीर के पीछे।
सरल अभिव्यंजनाएं गीत में बिल्कुल जरीरी हैं,
इसी से भागते हैं लोग ग़ालिब, मीर के पीछे।
आनंद परमानंद की ग़ज़लों के विषय भूख, गरीबी, बेरोजगारी, दलित, मजदूर, आदिवासी और किसान हैं। दहेज, लड़कियां, नारी, दंगे-फसाद जैसी समस्याएं हैं। इस कवि में, जिसे, चिंतनशील फ्रिक्रोपन कहते हैं, ग़ज़लों में अंत्यानुप्रास की नवीनता प्रशंसनीय है, जहां हिंदी भाषा की सामर्थ्य और कहन की शिष्टता-शालीनता दिखाई पड़ती है। जिंदगी की हद कहां तक है, जानते हुए, तनी रीढ़ से ललकारते आठ दशक पार कर गए ठाट के कद वाले इस कवि के शब्दों की लपट किसी भी कमजोर त्वचा वाले शब्द-बटोही को झुलसा सकती है।
खेलते होंगे उधर जाकर कहीं बच्चे मेरे।
वो खुला मैदान तट पर है, जिधर बच्चे मेरे।
भूख में लौटा हूं, पैदल रास्ते में रोककर,
मांगते हैं सेव, केले, ये मटर बच्चे मेरे।
साइकिल, छाता, गलीचे भी बनाना सीख लो,
काम देते हैं गरीबी में हुनर बच्चे मेरे।
भूख, बीमारी, उपेक्षा, कर्ज, महंगाई, दहेज,
सोच ही पाता नहीं, जाऊं किधर बच्चे मेरे।
जंतुओं के दांत-पंजों में जहर होता मगर
आदमी की आंख में बनता जहर बच्चे मेरे।
जो मिले, खा-पी के सोजा, मत किसी का नाम ले
कौन लेता है यहां, किसकी खबर बच्चे मेरे।
संस्कृतियां जब लड़ीं, सदियों की आंखें रो पड़ीं,
खंडहर होते गए, कितने शहर बच्चे मेरे।
यह बनारस है, यहां तुम पान बनकर मत जियो,
सब तमोली हैं, तुम्हे देंगे कतर बच्चे मेरे।
तुम मेरे हीरे हो, मोती हो, मेरी पहचान हो,
मेरे सब कुछ, मेरे दिल, मेरे जिगर बच्चे मेरे।
गालियां ग़ालिब, निराला खूब सहते थे यहां,
यह कमीनों का बहुत अच्छा शहर बच्चे मेरे।
मन से तरल इतने कि गोष्ठियों से मंचों तक कुछ उसी तरह शब्दों के साथ-साथ आंखों से बूंदें अनायास छलकती रहती हैं, जैसेकि कभी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कक्षा में अपने छात्रों को पढ़ाते हुए भावुक हो जाया करते थे। बुढ़ौती के कठिन-कठोर ठीये पर आज भी स्वभाव में बच्चों-सी हंसी-ठिठोली भरे अंदाज के आनंद परमानंद कहते हैं कि-
गरीबों के घरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
बदलते मंजरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
विचारों की मछलियां छटपटाकर मर नहीं जायें,
उबलते सागरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
तरक्की के तराजू पर नहीं तौले गये अब तक,
दबाये आखरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
जहां सदियों से डेरे डालकर रहती समस्याएं,
वो छानी-छप्परों तक जायेगा ये कारवां अपना।
जिन्हें हैं दुरदुराती वक्त की लाचारियां अक्सर
उन्हीं आहत स्वरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
जो ढरकी से लिखा करते नया इतिहास परिश्रम का
सभी उन बुनकरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
बताओ कब रुकेगा आबरू की आंख का पानी
तुम्हारे उत्तरों तक जाएगा ये कारवां मेरा।
आनंद परमानंद की कविता ही नहीं, इतिहास और पुरातत्व में भी गहरी अभिरुचि है। 'सड़क पर ज़िन्दगी' उनका चर्चित ग़ज़ल संग्रह है। जब भी उनकी रगों पर उंगलियां रखिए, दर्द से तिलमिलाते हुए भी सन्नध शिकारी की तरह दुश्मन-लक्ष्य पर झपट पड़ते हैं, व्यवस्था की एक-एक बखिया उधेड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम के इतने दशक बाद भी देश के आम आदमी का दुख और आक्रोश उनके शब्दों में धधकने लगता है-
ये बंधन तोड़कर बाहर निकलने की तो कोशिश कर।
सड़क पर जिंदगी है यार, चलने की तो कोशिश कर।
हवा में मत उड़ो छतरी गलतफहमी की तुम ताने,
कलेजा है तो धरती पर उतरने की तो कोशिश कर।
जहां दहशतभरी खामोशियों में लोग रहते हैं,
तू उस माहौल को थोड़ बदलने की तो कोशिश कर।
हकीकत पर जहां पर्दे पड़े हों, सब उठा डालो,
ये परिवर्तन जरूरी है, तू करने की तो कोशिश कर।
जलाकर मार डालेगी तुम्हे चिंता अकेले में,
कभी तू भीड़ से होकर गुजरने की तो कोशिश कर।
कठिन संघर्ष हो तो चुप्पियां मारी नहीं जातीं,
नयी उत्तेजना से बात कहने की तो कोशिश कर।
खुला आतंक पहले जन्म लेता है विचारों में,
परिंदे भी संभलते हैं, संभलने की तो कोशिश कर।
जरूरत है मुहब्बत-प्यार की, सद्भावनाओं की,
मिलेगा किस तरह, इसको समझने की तो कोशिश कर।
वाराणसी के ग्राम धानापुर (परियरा), राजा तालाब में 01 मई सन 1939 को पुरुषोत्तम सिंह के घर जनमे आनंद परमानंद आज भी गीत, ग़ज़लों के अपने रंग-ढंग के अनूठे कवि हैं। मिजाज में फक्कड़ी, बोल में विचारों के प्रति जितने कत्तई अडिग, कोमल भावों में मन-प्राण के उतने ही शहदीले। बेटियां उनके शब्दों में मुखर होती हैं, कई अध्यायों वाले घर-परिवारों के महाकाव्य की तरह, जिसमें अनुभवों की सघन पीड़ा भी है और वात्सल्य का अदभुत सामंजस्य भी-
फटे पुराने कपड़ों में यह मादल-डफली वाली लड़की।
जंगल से पैदल आयी है, पतली-दुबली-काली लड़की।
बड़े-बड़ों की बेटी होती, पढ़ती-लिखती, हंसती-गाती,
फोन बजाती, कार चलाती, लेती हाथ रुमाली लड़की।
गा-गाकर ही मांग रही है, फिर भी गाली सुन जाती है,
लो, प्रधान के घर से लौटी लिये कटोरी खाली लड़की।
ईर्ष्या-द्वेष कलुषता से है परिचय नहीं वंशगत इसका,
नीची आंखें बोल रही हैं, कितनी भोली-भाली लड़की।
इसका तो अध्यात्म भूख है, इसका सब चिंतन है रोटी,
गली-गली, मंदिर-मस्जिद हैं, दाता-ब्रह्म निराली लड़की।
मानवता के आदि दुर्ग पर लगा सभ्यता का जो ताला,
संसद को भी पता नहीं है, किस ताले की ताली लड़की।
दुर्योधन से बेईमान-युग के प्रति गुस्सा भरकर मन में,
भीम तुम्हीं से रक्त मांगती होगी यह पंचाली लड़की।
परमानंद की प्रकांडता का एक आश्चर्यजनक पक्ष है, उनमें संचित जीवंत अथाह स्मृतियां।
शब्द के जोखिम उठाता हूं, तो गीतों के लिए।
दर्द से रिश्ते निभाता हूं, तो गीतों के लिए।
गूंगी पीड़ा को नया शब्दार्थ देने के लिए,
भीड़ में भी छटपटाता हूं, तो गीतों के लिए।
सोचकर खेतों में ये प्रतिबद्धताएं रोपकर,
नये सम्बोधन उगाता हूं, तो गीतों के लिए।
माथ पर उंगली धरे सच्चाइयों के द्वार की,
सांकलें जब खटखटाता हूं, तो गीतों के लिए।
जिनके चेहरों पर हंसी फिर लौटकर आयी नहीं,
उनकी खातिर बौखलाता हूं, तो गीतों के लिए।
ओढ़कर कुहरे पड़ी चुपचाप ठंडी रात में,
पत्तियों सा खड़खड़ाता हूं, तो गीतों के लिए।
मिल गया मौसम सड़क पर जब असभ्यों की तरह,
वक्त को कुछ बड़बड़ाता हूं, तो गीतों के लिए।
जब तक साथ, सोचते रहिए कि ये आदमी है या कोई मास्टर कम्यूटर। भला किसी एक आदमी को इतनी बातें अक्षरशः कैसे याद रह सकती हैं, जबकि उम्र अस्सी के पार, स्मृतिभ्रंश की आशंकाओं से भरी रहती है। दरअसल, आनंद परमानंद दुष्यंत परंपरा के सशक्त ग़ज़लकार हैं। एक जमाने में इनकी ग़ज़लें प्रायः मंचों पर अपना प्रभाव स्थापित करती रही हैं। वह आदमी की तरह जिंदगी काटते हैं। आज तो यह आशंका जन्म लेने लगी है कि सही आदमी सड़क पर भी रह पाएगा अथवा नहीं। आखिर वह जाए भी तो कहां जाए। उनकी ग़ज़लें पढ़कर इस बात पर प्रसन्नता होती है कि कम से कम उन्होंने नकली और बनावटी बातें तो नहीं कही हैं।
कड़ी चिल्लाहटें क्यूं हैं इसी तस्वीर के पीछे।
मरा सच है कहीं फिर क्या उसी प्राचीर के पीछे।
यहां तो बेगुनाहों ने तड़प कर जिंदगी दी है,
खड़ा इतिहास है रोता हुआ जंजीर के पीछे।
बहुत बेआबरू संवेदनाएं जब हुई होंगी,
बड़ी हलचल मची होगी नयन के नीर के पीछे।
कठिन संघर्ष में संभावनाएं जन्म लेती हैं,
इसी उम्मीद में वह है खड़ा शहतीर के पीछे।
समय की झनझनाहट सुन, बराबर काम करते चल,
न लट्टू की तरह नाचा करो तकदीर के पीछे।
कलम जो जिंदगी देगी, कहीं फिर मिल नहीं सकती,
अरे मन अब कभी मत भागना जागीर के पीछे।
सरल अभिव्यंजनाएं गीत में बिल्कुल जरीरी हैं,
इसी से भागते हैं लोग ग़ालिब, मीर के पीछे।
आनंद परमानंद की ग़ज़लों के विषय भूख, गरीबी, बेरोजगारी, दलित, मजदूर, आदिवासी और किसान हैं। दहेज, लड़कियां, नारी, दंगे-फसाद जैसी समस्याएं हैं। इस कवि में, जिसे, चिंतनशील फ्रिक्रोपन कहते हैं, ग़ज़लों में अंत्यानुप्रास की नवीनता प्रशंसनीय है, जहां हिंदी भाषा की सामर्थ्य और कहन की शिष्टता-शालीनता दिखाई पड़ती है। जिंदगी की हद कहां तक है, जानते हुए, तनी रीढ़ से ललकारते आठ दशक पार कर गए ठाट के कद वाले इस कवि के शब्दों की लपट किसी भी कमजोर त्वचा वाले शब्द-बटोही को झुलसा सकती है।
खेलते होंगे उधर जाकर कहीं बच्चे मेरे।
वो खुला मैदान तट पर है, जिधर बच्चे मेरे।
भूख में लौटा हूं, पैदल रास्ते में रोककर,
मांगते हैं सेव, केले, ये मटर बच्चे मेरे।
साइकिल, छाता, गलीचे भी बनाना सीख लो,
काम देते हैं गरीबी में हुनर बच्चे मेरे।
भूख, बीमारी, उपेक्षा, कर्ज, महंगाई, दहेज,
सोच ही पाता नहीं, जाऊं किधर बच्चे मेरे।
जंतुओं के दांत-पंजों में जहर होता मगर
आदमी की आंख में बनता जहर बच्चे मेरे।
जो मिले, खा-पी के सोजा, मत किसी का नाम ले
कौन लेता है यहां, किसकी खबर बच्चे मेरे।
संस्कृतियां जब लड़ीं, सदियों की आंखें रो पड़ीं,
खंडहर होते गए, कितने शहर बच्चे मेरे।
यह बनारस है, यहां तुम पान बनकर मत जियो,
सब तमोली हैं, तुम्हे देंगे कतर बच्चे मेरे।
तुम मेरे हीरे हो, मोती हो, मेरी पहचान हो,
मेरे सब कुछ, मेरे दिल, मेरे जिगर बच्चे मेरे।
गालियां ग़ालिब, निराला खूब सहते थे यहां,
यह कमीनों का बहुत अच्छा शहर बच्चे मेरे।
मन से तरल इतने कि गोष्ठियों से मंचों तक कुछ उसी तरह शब्दों के साथ-साथ आंखों से बूंदें अनायास छलकती रहती हैं, जैसेकि कभी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कक्षा में अपने छात्रों को पढ़ाते हुए भावुक हो जाया करते थे। बुढ़ौती के कठिन-कठोर ठीये पर आज भी स्वभाव में बच्चों-सी हंसी-ठिठोली भरे अंदाज के आनंद परमानंद कहते हैं कि-
गरीबों के घरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
बदलते मंजरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
विचारों की मछलियां छटपटाकर मर नहीं जायें,
उबलते सागरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
तरक्की के तराजू पर नहीं तौले गये अब तक,
दबाये आखरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
जहां सदियों से डेरे डालकर रहती समस्याएं,
वो छानी-छप्परों तक जायेगा ये कारवां अपना।
जिन्हें हैं दुरदुराती वक्त की लाचारियां अक्सर
उन्हीं आहत स्वरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
जो ढरकी से लिखा करते नया इतिहास परिश्रम का
सभी उन बुनकरों तक जायेगा ये कारवां अपना।
बताओ कब रुकेगा आबरू की आंख का पानी
तुम्हारे उत्तरों तक जाएगा ये कारवां मेरा।
आनंद परमानंद की कविता ही नहीं, इतिहास और पुरातत्व में भी गहरी अभिरुचि है। 'सड़क पर ज़िन्दगी' उनका चर्चित ग़ज़ल संग्रह है। जब भी उनकी रगों पर उंगलियां रखिए, दर्द से तिलमिलाते हुए भी सन्नध शिकारी की तरह दुश्मन-लक्ष्य पर झपट पड़ते हैं, व्यवस्था की एक-एक बखिया उधेड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम के इतने दशक बाद भी देश के आम आदमी का दुख और आक्रोश उनके शब्दों में धधकने लगता है-
ये बंधन तोड़कर बाहर निकलने की तो कोशिश कर।
सड़क पर जिंदगी है यार, चलने की तो कोशिश कर।
हवा में मत उड़ो छतरी गलतफहमी की तुम ताने,
कलेजा है तो धरती पर उतरने की तो कोशिश कर।
जहां दहशतभरी खामोशियों में लोग रहते हैं,
तू उस माहौल को थोड़ बदलने की तो कोशिश कर।
हकीकत पर जहां पर्दे पड़े हों, सब उठा डालो,
ये परिवर्तन जरूरी है, तू करने की तो कोशिश कर।
जलाकर मार डालेगी तुम्हे चिंता अकेले में,
कभी तू भीड़ से होकर गुजरने की तो कोशिश कर।
कठिन संघर्ष हो तो चुप्पियां मारी नहीं जातीं,
नयी उत्तेजना से बात कहने की तो कोशिश कर।
खुला आतंक पहले जन्म लेता है विचारों में,
परिंदे भी संभलते हैं, संभलने की तो कोशिश कर।
जरूरत है मुहब्बत-प्यार की, सद्भावनाओं की,
मिलेगा किस तरह, इसको समझने की तो कोशिश कर।
वाराणसी के ग्राम धानापुर (परियरा), राजा तालाब में 01 मई सन 1939 को पुरुषोत्तम सिंह के घर जनमे आनंद परमानंद आज भी गीत, ग़ज़लों के अपने रंग-ढंग के अनूठे कवि हैं। मिजाज में फक्कड़ी, बोल में विचारों के प्रति जितने कत्तई अडिग, कोमल भावों में मन-प्राण के उतने ही शहदीले। बेटियां उनके शब्दों में मुखर होती हैं, कई अध्यायों वाले घर-परिवारों के महाकाव्य की तरह, जिसमें अनुभवों की सघन पीड़ा भी है और वात्सल्य का अदभुत सामंजस्य भी-
फटे पुराने कपड़ों में यह मादल-डफली वाली लड़की।
जंगल से पैदल आयी है, पतली-दुबली-काली लड़की।
बड़े-बड़ों की बेटी होती, पढ़ती-लिखती, हंसती-गाती,
फोन बजाती, कार चलाती, लेती हाथ रुमाली लड़की।
गा-गाकर ही मांग रही है, फिर भी गाली सुन जाती है,
लो, प्रधान के घर से लौटी लिये कटोरी खाली लड़की।
ईर्ष्या-द्वेष कलुषता से है परिचय नहीं वंशगत इसका,
नीची आंखें बोल रही हैं, कितनी भोली-भाली लड़की।
इसका तो अध्यात्म भूख है, इसका सब चिंतन है रोटी,
गली-गली, मंदिर-मस्जिद हैं, दाता-ब्रह्म निराली लड़की।
मानवता के आदि दुर्ग पर लगा सभ्यता का जो ताला,
संसद को भी पता नहीं है, किस ताले की ताली लड़की।
दुर्योधन से बेईमान-युग के प्रति गुस्सा भरकर मन में,
भीम तुम्हीं से रक्त मांगती होगी यह पंचाली लड़की।
Tuesday 20 February 2018
महाप्राण जितने फटेहाल, उतने दानवीर
महाप्राण निराला मस्तमौला, यायावर तो थे ही, फकीरी में भी दानबहादुरी ऐसी कि जेब का आखिरी आना-पाई तक मुफलिसों को लुटा आते थे। नया रजाई-गद्दा रेलवे स्टेशन के भिखारियों को दान कर खुद थरथर जाड़ में फटी रजाई तानकर सो जाते थे। जीवन की ऐसी विसंगतियां-उलटबासियां शायद ही किसी अन्य महान कवि-साहित्यकार की सुनने-पढ़ने को मिलें, जैसी की महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। सुख-दुख की ऐसी कई अनकही-अलिखित-अपठित गाथाएं उनके जीवन से जुड़ी हैं। वह मस्तमौला, यायावर तो थे ही, लाख फटेहाली में भी जेब का आखिरी आना-पाई तक दान कर देते थे। उत्तर प्रदेश के शीर्ष शिक्षाधिकारी रहे साहित्यकार श्रीनारायण चतुर्वेदी के ठिकाने पर वह अक्सर लखनऊ पहुंच जाया करते थे। और वहां कब तक रहेंगे, कब अचानक कहीं और चले जाएंगे, कोई तय नहीं होता था। श्रीनारायण चुतर्वेदी के साथ निरालाजी के कई प्रसंग जुड़े हैं। लोग चतुर्वेदीजी को सम्मान से 'भैयाजी' कहकर संबोधित करते थे। वह कवि-साहित्यकारों को मंच दिलाने से लेकर उनकी रचनाओं के प्रकाशन, आतिथ्य, निजी आर्थिक जरूरतें पूरी कराने तक में हर वक्त तत्पर रहते थे।
जाड़े का दिन था। कवि-सम्मेलन खत्म होने के बाद एक बार भैयाजी बनारसी, श्यामनारायण पांडेय, चोंच बनारसी समेत चार-पांच कवि सुबह-सुबह चतुर्वेदीजी के आवास पर पहुंचे और सीढ़ी से सीधे पहली मंजिल के उनके कमरे में पहुंचते ही अंचंभित होते हुए एक स्वर में चतुर्वेदीजी से पूछा - 'भैयाजी नीचे के खाली कमरे में फर्श पर फटी रजाई ओढ़े कौन सो रहा है? सिर तो रजाई में लिपटा है और पायताने की फटी रजाई से दोनों पांव झांक रहे हैं।' चतुर्वेदीजी ने ठहाका लगाते हुए कहा - 'अरे और कौन होगा! वही महापुरुष हैं।... निरालाजी। ... क्या करें जो भी रजाई-बिछौना देता हूं, रेलवे स्टेशन के भिखारियों को बांट आते हैं। अभी लंदन से लौटकर दो महंगी रजाइयां लाया था। उनमें एक उनके लिए खरीदी थी, दे दिया। पिछले दिनो पहले एक रजाई और गद्दा दान कर आए। दूसरी अपनी दी, तो उसे भी बांट आए। फटी रजाई घर में पड़ी थी। दे दिया कि लो, ओढ़ो। रोज-रोज इतनी रजाइयां कहां से लाऊं कि वो दान करते फिरें, मैं इंतजाम करता रहूं।'
इसके बाद छत की रेलिंग पर पहुंचकर मुस्कराते हुए चतुर्वेदी जी ने मनोविनोद के लिए इतने जोर से नीचे किसी व्यक्ति को कवियों के नाश्ते के लिए जलेबी लाने को कहा, ताकि आवाज निरालाजी के भी कानों तक पहुंच जाए। जलेबी आ गई। निरालाजी को किसी ने नाश्ते के लिए बुलाया नहीं। गुस्से में फटी रजाई ओढ़े वह स्वयं धड़धड़ाते कमरे से बाहर निकले और मुंह उठाकर चीखे - 'मुझे नहीं खानी आपकी जलेबी।' और तेजी से जलेबी खाने रेलवे स्टेशन निकल गए। इसके बाद ऊपर जोर का ठहाका गूंजा। लौटे तो वह फटी रजाई भी दान कर आए थे।
निरालाजी चाहे कितने भी गुस्से में हों, चतुर्वेदीजी की कदापि, कभी तनिक अवज्ञा नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ कि, कवि-सम्मेलन में संचालक ने सरस्वती वंदना (वर दे वीणा वादिनी..) के लिए निरालाजी का नाम माइक से पुकारा। वह मंच की बजाए, गुस्से से लाल-पीले श्रोताओं के बीच जा बैठे थे। मंच पर हारमोनियम भी रखा था। पहले से तय था, सरस्वती वंदना का सस्वर पाठ निरालाजी को ही करना है, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया था। निरालाजी बैठे-बैठे जोर से चीखे- 'मैं नहीं करूंगा सरस्वती वंदना।' इसके बाद एक-एक कर मंचासीन दो-तीन महाकवियों ने उनसे अनुनय-विनय किया। निरालाजी टस-से-मस नहीं। मंच पर श्रीनारायण चतुर्वेदी भी थे। उन्होंने संचालक से कहा - 'मंच पर आएंगे कैसे नहीं, अभी लो, देखो, उन्हें कैसे बुलाता हूं मैं।' वह निरालाजी को मनाने की कला जानते थे। उन्होंने माइक से घोषणा की - 'निरालाजी आज कविता पाठ नहीं करेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है।' तत्क्षण निरालाजी चीखे और उठ खड़े हुए - 'आपको कैसे मालूम, मेरी तबीयत खराब है! सुनाऊंगा। जरूर सुनाऊंगा।' और फिर तो हारमोनियम पर देर तक उनके स्वर गूंजते रहे।
जाड़े का दिन था। कवि-सम्मेलन खत्म होने के बाद एक बार भैयाजी बनारसी, श्यामनारायण पांडेय, चोंच बनारसी समेत चार-पांच कवि सुबह-सुबह चतुर्वेदीजी के आवास पर पहुंचे और सीढ़ी से सीधे पहली मंजिल के उनके कमरे में पहुंचते ही अंचंभित होते हुए एक स्वर में चतुर्वेदीजी से पूछा - 'भैयाजी नीचे के खाली कमरे में फर्श पर फटी रजाई ओढ़े कौन सो रहा है? सिर तो रजाई में लिपटा है और पायताने की फटी रजाई से दोनों पांव झांक रहे हैं।' चतुर्वेदीजी ने ठहाका लगाते हुए कहा - 'अरे और कौन होगा! वही महापुरुष हैं।... निरालाजी। ... क्या करें जो भी रजाई-बिछौना देता हूं, रेलवे स्टेशन के भिखारियों को बांट आते हैं। अभी लंदन से लौटकर दो महंगी रजाइयां लाया था। उनमें एक उनके लिए खरीदी थी, दे दिया। पिछले दिनो पहले एक रजाई और गद्दा दान कर आए। दूसरी अपनी दी, तो उसे भी बांट आए। फटी रजाई घर में पड़ी थी। दे दिया कि लो, ओढ़ो। रोज-रोज इतनी रजाइयां कहां से लाऊं कि वो दान करते फिरें, मैं इंतजाम करता रहूं।'
इसके बाद छत की रेलिंग पर पहुंचकर मुस्कराते हुए चतुर्वेदी जी ने मनोविनोद के लिए इतने जोर से नीचे किसी व्यक्ति को कवियों के नाश्ते के लिए जलेबी लाने को कहा, ताकि आवाज निरालाजी के भी कानों तक पहुंच जाए। जलेबी आ गई। निरालाजी को किसी ने नाश्ते के लिए बुलाया नहीं। गुस्से में फटी रजाई ओढ़े वह स्वयं धड़धड़ाते कमरे से बाहर निकले और मुंह उठाकर चीखे - 'मुझे नहीं खानी आपकी जलेबी।' और तेजी से जलेबी खाने रेलवे स्टेशन निकल गए। इसके बाद ऊपर जोर का ठहाका गूंजा। लौटे तो वह फटी रजाई भी दान कर आए थे।
निरालाजी चाहे कितने भी गुस्से में हों, चतुर्वेदीजी की कदापि, कभी तनिक अवज्ञा नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ कि, कवि-सम्मेलन में संचालक ने सरस्वती वंदना (वर दे वीणा वादिनी..) के लिए निरालाजी का नाम माइक से पुकारा। वह मंच की बजाए, गुस्से से लाल-पीले श्रोताओं के बीच जा बैठे थे। मंच पर हारमोनियम भी रखा था। पहले से तय था, सरस्वती वंदना का सस्वर पाठ निरालाजी को ही करना है, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया था। निरालाजी बैठे-बैठे जोर से चीखे- 'मैं नहीं करूंगा सरस्वती वंदना।' इसके बाद एक-एक कर मंचासीन दो-तीन महाकवियों ने उनसे अनुनय-विनय किया। निरालाजी टस-से-मस नहीं। मंच पर श्रीनारायण चतुर्वेदी भी थे। उन्होंने संचालक से कहा - 'मंच पर आएंगे कैसे नहीं, अभी लो, देखो, उन्हें कैसे बुलाता हूं मैं।' वह निरालाजी को मनाने की कला जानते थे। उन्होंने माइक से घोषणा की - 'निरालाजी आज कविता पाठ नहीं करेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है।' तत्क्षण निरालाजी चीखे और उठ खड़े हुए - 'आपको कैसे मालूम, मेरी तबीयत खराब है! सुनाऊंगा। जरूर सुनाऊंगा।' और फिर तो हारमोनियम पर देर तक उनके स्वर गूंजते रहे।
Monday 19 February 2018
'हल्दीघाटी' की रिकार्डिंग पर वाह-वाह
वह सब बड़ा धुंधला-धुंधला सा रह गया है स्मृतियों में। ओझल होता हुआ। प्रसिद्ध कवि रामावतार त्यागी की एक पंक्ति अक्सर मन पर तैरने लगती है- 'जिंदगी तू ही बता तेरा इरादा क्या है,...।' मौत बुलाई नहीं जाती, आ जाती है, बिना पूछताछ, अपना वक्त देखकर। रामावतार त्यागी जितने लोकप्रिय कवि, उतने ही बेहतर इंसान भी थे। आज वह हमारे बीच नहीं हैं लेकिन जब भी वह याद आते हैं, मुंबई का एक खुशहाल दिन दिल में खिल उठता है। लगभग तीस साल पहले 'हल्दीघाटी' के रचनाकार पं.श्याम नारायण पांडेय के साथ मुंबई जाना हुआ था। चौपाटी पर कवि सम्मेलन के अगले दिन 'हल्दीघाटी' की कविताओं की रिकार्डिंग होनी थी। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, सो रामावतार त्यागी का दूत बार-बार पांडेयजी से सम्पर्क साधने आ टपकता कि चलिए, रिकार्डिंग का समय हो रहा है।
इससे पांडेयजी को बड़ी झुझलाहट होती। इसकी एक और वजह थी। उन दिनो मंचों पर छाई रहीं कवयित्री माया गोविंद पांडेयजी को उनके सुमित्र हरिवंश राय बच्चन से मिलवाने ले जाना चाहती थीं। उस वक्त दिनो उनके पुत्र अमिताभ बच्चन 'कुली' के फिल्मांकन में घायल होने के बाद 'प्रतीक्षा' में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। माया गोविंद के साथ उनके दामाद भी थे, जो बच्चन जी से मिलने के बहाने अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते थे। पांडेयजी बार-बार मुझसे पूछते कि क्या करें। मेरा विचार था कि पहले रिकार्डिंग हो जाए, फिर समय बचता है तो बच्चनजी से मिलने चलें क्योंकि रामावतार त्यागी उन दिनो साहित्यिक विरासत के तौर पर देश के प्रमुख कवि-साहित्यकारों के शब्द उनकी जुबानी रिकार्ड करा रहे थे।
भीतर से मन तो मेरा भी था कि बच्चन जी से मुलाकात हो जाए, क्योंकि पांडेयजी से उनकी अंतरंग मित्रता के दिनो की अनेकशः कहानियां सुन रखी थीं किंतु तब तक मुलाकात नहीं हुई थी। इस बीच बच्चन जी के फोन आते रहे कि 'पांडेय कब पहुंचोगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं!' अंततः पांडेयजी पहले बच्चन जी से मिलने पहुंचे, साथ में माया गोविंद और उनके दामाद सहित हम तीनो भी। उस मुलाकात की बात विस्तार से और कभी। उस दिन इतना अप्रिय जरूर हुआ कि अमिताभ मिले नहीं। ज्योंही हम 'प्रतीक्षा' के मुख्य द्वार में प्रविष्ट हुए, परिसर के मंदिर से निकलकर अमिताभ सीधे अपने विश्राम कक्ष में चले गए। फिर लाख मिन्नत पर भी मिलने नहीं निकले।
वहां से हम पहुंचे रामावतार त्यागी के साथ रिकार्डिंग रूम। श्याम नारायण पांडेय 'हल्दीघाटी' का कविता पाठ करते रहे, और हम तीनो को साथ में वाह-वाह करने के लिए बैठा लिया गया। उन दिनो रामावतार त्यागी सांस की बीमारी से परेशान थे। बमुश्किल रिकार्डिंग करा सके लेकिन उस वाकये जैसे वक्त से एक सीख मिली कि उन दिनो बंबई जैसी चमक-दमक की दुनिया में भी साहित्य को लेकर वहां के चुनिंदा कवि-साहित्यकारों में कितना अनुराग और तल्लनीनता थी। 'हल्दीघाटी' का वह रिकार्ड कविता-पाठ तो कभी सुनने को नहीं मिला और रामावतार त्यागी भी नहीं रहे लेकिन कविता के प्रति उनकी लगन और मेहनत आज भी प्रेरणा देती रहती है। काश, वह रिकार्डिंग सुनने को कहीं से मिल जाती-
'रण बीच चौकड़ी, भर भरकर,
चेतक बन गया निराला था,
राणा प्रताप के घोड़े से,
पड़ गया हवा का पाला था'...।
इससे पांडेयजी को बड़ी झुझलाहट होती। इसकी एक और वजह थी। उन दिनो मंचों पर छाई रहीं कवयित्री माया गोविंद पांडेयजी को उनके सुमित्र हरिवंश राय बच्चन से मिलवाने ले जाना चाहती थीं। उस वक्त दिनो उनके पुत्र अमिताभ बच्चन 'कुली' के फिल्मांकन में घायल होने के बाद 'प्रतीक्षा' में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। माया गोविंद के साथ उनके दामाद भी थे, जो बच्चन जी से मिलने के बहाने अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते थे। पांडेयजी बार-बार मुझसे पूछते कि क्या करें। मेरा विचार था कि पहले रिकार्डिंग हो जाए, फिर समय बचता है तो बच्चनजी से मिलने चलें क्योंकि रामावतार त्यागी उन दिनो साहित्यिक विरासत के तौर पर देश के प्रमुख कवि-साहित्यकारों के शब्द उनकी जुबानी रिकार्ड करा रहे थे।
भीतर से मन तो मेरा भी था कि बच्चन जी से मुलाकात हो जाए, क्योंकि पांडेयजी से उनकी अंतरंग मित्रता के दिनो की अनेकशः कहानियां सुन रखी थीं किंतु तब तक मुलाकात नहीं हुई थी। इस बीच बच्चन जी के फोन आते रहे कि 'पांडेय कब पहुंचोगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं!' अंततः पांडेयजी पहले बच्चन जी से मिलने पहुंचे, साथ में माया गोविंद और उनके दामाद सहित हम तीनो भी। उस मुलाकात की बात विस्तार से और कभी। उस दिन इतना अप्रिय जरूर हुआ कि अमिताभ मिले नहीं। ज्योंही हम 'प्रतीक्षा' के मुख्य द्वार में प्रविष्ट हुए, परिसर के मंदिर से निकलकर अमिताभ सीधे अपने विश्राम कक्ष में चले गए। फिर लाख मिन्नत पर भी मिलने नहीं निकले।
वहां से हम पहुंचे रामावतार त्यागी के साथ रिकार्डिंग रूम। श्याम नारायण पांडेय 'हल्दीघाटी' का कविता पाठ करते रहे, और हम तीनो को साथ में वाह-वाह करने के लिए बैठा लिया गया। उन दिनो रामावतार त्यागी सांस की बीमारी से परेशान थे। बमुश्किल रिकार्डिंग करा सके लेकिन उस वाकये जैसे वक्त से एक सीख मिली कि उन दिनो बंबई जैसी चमक-दमक की दुनिया में भी साहित्य को लेकर वहां के चुनिंदा कवि-साहित्यकारों में कितना अनुराग और तल्लनीनता थी। 'हल्दीघाटी' का वह रिकार्ड कविता-पाठ तो कभी सुनने को नहीं मिला और रामावतार त्यागी भी नहीं रहे लेकिन कविता के प्रति उनकी लगन और मेहनत आज भी प्रेरणा देती रहती है। काश, वह रिकार्डिंग सुनने को कहीं से मिल जाती-
'रण बीच चौकड़ी, भर भरकर,
चेतक बन गया निराला था,
राणा प्रताप के घोड़े से,
पड़ गया हवा का पाला था'...।
किसी मंच पर श्याम नारायण पांडेय जब ये पंक्तियां पढ़ रहे थे (...चेतक बन गया निराला था), मंच पर मौजूद निराला जी चौंक पड़े थे- क्या कहा, 'निराला' था!
Thursday 15 February 2018
चोंच जी ने कहा - सुधारूंगा या सिधारूंगा
'सांड़', 'सूंढ़', 'चकाचक', 'झंड', 'भंड' जैसे नाना प्रकार के विकालांग नामों वाले आज तो तमाम कवि सुर्खियों में रहते हैं। आज क्या, पिछले कई दशकों से। इन ऐसों-वैसों के नाम गूंजते चले आ रहे हैं और अब तो हंसोड़ जोकर और मदारी कवि के रूप में मंचों से भांड़-भंड़ैती करते रहते हैं, कथित कविता की हर लाइन पर श्रोताओं से तालियों की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन स्वस्थ हास्य का भी एक ऐसा जमाना गुजरा है, जिस पर हिंदी साहित्य को गर्व है। हमारे वैसे ही पुरखों में एक थे हास्यकवि कांतानाथ पांडेय 'चोंच'। आज भी 'चोंच बनारसी' के नाम से उन्हें बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। वह अत्यंत प्रतिभा संपन्न 'आशु कवि' भी थे। 'आशु कवि' यानी किसी भी परिवेश पर, किसी भी विषय पर तुरंत कविता लिख देने में निपुण। हमारे उस जमाने के पुरखा कवि सिर्फ अच्छी कविताएं ही नहीं लिखते थे, वह अपनी जीवनचर्या से भी समाज को सीख देते थे।
कवि चोंच बनारसी के साथ घटा एक अत्यंत दुखद वाकया उसका एक जीवंत साक्ष्य है। जब उन्होंने वाराणसी के हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल का पद संभाला तो उस वक्त परिसर का माहौल काफी खराब था। कोई भी समझदार अभिभावक उस कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ने नहीं देना चाहता था। चार्ज संभालते ही चोंचजी ने शपथ ली कि वह कॉलेज का बिगड़ा माहौल या तो सुधारेंगे, या वहां से सिधारेंगे यानी चले जाएंगे। सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि कॉलेज में अराजक छात्रों का एडमिशन तुरंत सख्ती से रोक दिया। इससे पूरे बनारस में हड़कंप सा मच गया। चूंकि उन दिनों काशी नगरी कवियों, साहित्यकारों का गढ़ हुआ करती थी, चोंचजी के सख्त फरमान से यह चर्चा पूरे पूर्वांचल के कवि-लेखकों के बीच भी फैल गयी। चोंचजी के दुस्साहस पर तरह-तरह की बातें होने लगीं।
कॉलेज में एक छात्र ऐसा भी था, जो बार-बार फेल होने के बावजूद गुंडई के बल पर वर्षों से वहां जमा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे कॉलेज से निकाल दे, उसे परिसर में न आने दे। जब चोंचजी का नोटिस सार्वजनिक हुआ तो वह अगले ही दिन चैंबर में बड़े ताव से आ धमका। पांव पटकते हुए उन पर खूब गुर्राया। आपे से बाहर हुआ। जान लेने की धमकी तक दे गया। लेकिन चोंचजी ने भी उसी की भाषा में उसे समझाते हुए किसी भी कीमत पर उसे प्रवेश न देने की ठान ली। इससे परिसर का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। उस अराजक छात्र के जब साम-दाम-दंड-भेद, सारे जतन विफल हो गए, एक दिन उसने कॉलेज से रिक्शे पर घर लौटते समय चोंचजी पर पीछे से खूनी वार कर दिया। चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी में लगा। घटना के बाद वह तो भाग गया, चोंच जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी रिक्शे से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
इस घटना के बाद काशी के कवि-लेखकों में रोष फैल गया। जैसे पूरा बौद्धिक वर्ग विरोध में मुखर हो उठा। हर तरफ से प्रशासन की फजीहत होने लगी। पुलिस हमलावर का पता लगाने में जुट गई। उसी दौरान पुलिस की टीम बार-बार चोंच जी के ठिकाने पर भी पूछताछ के लिए पहुंचने लगी। पुलिस चाहती थी कि हमलावर के खिलाफ पीड़ित (चोंचजी) की ओर से नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी जाये। चोंचजी किसी भी कीमत पर छात्र का नाम बताने को तैयार नहीं ते। उनका कहना था कि गुनाह उस छात्र का नहीं, कॉलेज के माहौल का है, जिसे समय से ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया। इसके लिए वे अभिभावक भी जिम्मेदार हैं, जिनके बच्चे कॉलेज के इतने खराब माहौल में भी अब तक पढ़ने के लिए भेजे जाते रहे हैं। आखिरकार, उस घटना के छह महीने बाद घायल चोंचजी की मौत हो गई। अंत तक उन्होंने हमलावर का नाम अपनी जुबान पर नहीं आने दिया तो नहीं ही आने दिया। चोंचजी सिधार जरूर गए लेकिन उसके बाद कॉलेज का माहौल सुधर गया।
आजकल के शिक्षकों अथवा कवि-सम्मेलनी जोकरों, मदारियों से समाज अथवा परिसरों के बिगड़ते माहौल में उस तरह की कुर्बानियों की उम्मीद करना नासमझी होगी। मंच के हंसोड़ों को तो पैसा बटोरने से फुर्सत नहीं है। जरूरत तो आज भी है चोंचजी जैसे कवि-लेखकों, शिक्षकों की, हमारे सामने हर पल। लेकिन अब वैसा साहस कहां। उसमें हम कहां हैं, कैसे हैं, किस भूमिका में हैं, बात गौरतलब लगती है। साहित्यिक सन्नाटे में आज सबसे बड़े गुनहगार वे लगते हैं, जो नई पीढ़ी को सही राह दिखाने में लापता हैं। यही वजह है कि पिछले दो दशकों में कविता की एक भी ऐसी किताब नहीं आयी है, जिसके बारे में आम पाठकों के मुंह से कुछ सुनाई पड़े। ऐसों-वैसों के बारे में खिन्नमना तीक्ष्णता से इतना भर कहा जा सकता है कि वे सिर्फ.... 'परस्परम् प्रशंसति, अहो रूपम्, अहो ध्वनिः।'
कवि चोंच बनारसी के साथ घटा एक अत्यंत दुखद वाकया उसका एक जीवंत साक्ष्य है। जब उन्होंने वाराणसी के हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल का पद संभाला तो उस वक्त परिसर का माहौल काफी खराब था। कोई भी समझदार अभिभावक उस कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ने नहीं देना चाहता था। चार्ज संभालते ही चोंचजी ने शपथ ली कि वह कॉलेज का बिगड़ा माहौल या तो सुधारेंगे, या वहां से सिधारेंगे यानी चले जाएंगे। सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि कॉलेज में अराजक छात्रों का एडमिशन तुरंत सख्ती से रोक दिया। इससे पूरे बनारस में हड़कंप सा मच गया। चूंकि उन दिनों काशी नगरी कवियों, साहित्यकारों का गढ़ हुआ करती थी, चोंचजी के सख्त फरमान से यह चर्चा पूरे पूर्वांचल के कवि-लेखकों के बीच भी फैल गयी। चोंचजी के दुस्साहस पर तरह-तरह की बातें होने लगीं।
कॉलेज में एक छात्र ऐसा भी था, जो बार-बार फेल होने के बावजूद गुंडई के बल पर वर्षों से वहां जमा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे कॉलेज से निकाल दे, उसे परिसर में न आने दे। जब चोंचजी का नोटिस सार्वजनिक हुआ तो वह अगले ही दिन चैंबर में बड़े ताव से आ धमका। पांव पटकते हुए उन पर खूब गुर्राया। आपे से बाहर हुआ। जान लेने की धमकी तक दे गया। लेकिन चोंचजी ने भी उसी की भाषा में उसे समझाते हुए किसी भी कीमत पर उसे प्रवेश न देने की ठान ली। इससे परिसर का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। उस अराजक छात्र के जब साम-दाम-दंड-भेद, सारे जतन विफल हो गए, एक दिन उसने कॉलेज से रिक्शे पर घर लौटते समय चोंचजी पर पीछे से खूनी वार कर दिया। चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी में लगा। घटना के बाद वह तो भाग गया, चोंच जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी रिक्शे से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
इस घटना के बाद काशी के कवि-लेखकों में रोष फैल गया। जैसे पूरा बौद्धिक वर्ग विरोध में मुखर हो उठा। हर तरफ से प्रशासन की फजीहत होने लगी। पुलिस हमलावर का पता लगाने में जुट गई। उसी दौरान पुलिस की टीम बार-बार चोंच जी के ठिकाने पर भी पूछताछ के लिए पहुंचने लगी। पुलिस चाहती थी कि हमलावर के खिलाफ पीड़ित (चोंचजी) की ओर से नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी जाये। चोंचजी किसी भी कीमत पर छात्र का नाम बताने को तैयार नहीं ते। उनका कहना था कि गुनाह उस छात्र का नहीं, कॉलेज के माहौल का है, जिसे समय से ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया। इसके लिए वे अभिभावक भी जिम्मेदार हैं, जिनके बच्चे कॉलेज के इतने खराब माहौल में भी अब तक पढ़ने के लिए भेजे जाते रहे हैं। आखिरकार, उस घटना के छह महीने बाद घायल चोंचजी की मौत हो गई। अंत तक उन्होंने हमलावर का नाम अपनी जुबान पर नहीं आने दिया तो नहीं ही आने दिया। चोंचजी सिधार जरूर गए लेकिन उसके बाद कॉलेज का माहौल सुधर गया।
आजकल के शिक्षकों अथवा कवि-सम्मेलनी जोकरों, मदारियों से समाज अथवा परिसरों के बिगड़ते माहौल में उस तरह की कुर्बानियों की उम्मीद करना नासमझी होगी। मंच के हंसोड़ों को तो पैसा बटोरने से फुर्सत नहीं है। जरूरत तो आज भी है चोंचजी जैसे कवि-लेखकों, शिक्षकों की, हमारे सामने हर पल। लेकिन अब वैसा साहस कहां। उसमें हम कहां हैं, कैसे हैं, किस भूमिका में हैं, बात गौरतलब लगती है। साहित्यिक सन्नाटे में आज सबसे बड़े गुनहगार वे लगते हैं, जो नई पीढ़ी को सही राह दिखाने में लापता हैं। यही वजह है कि पिछले दो दशकों में कविता की एक भी ऐसी किताब नहीं आयी है, जिसके बारे में आम पाठकों के मुंह से कुछ सुनाई पड़े। ऐसों-वैसों के बारे में खिन्नमना तीक्ष्णता से इतना भर कहा जा सकता है कि वे सिर्फ.... 'परस्परम् प्रशंसति, अहो रूपम्, अहो ध्वनिः।'
कवि-मित्र का पुत्र मोस्ट वांटेड !
मेरे एक साहित्यिक मित्र थे। वीर रस की कविताएं लिखते थे। पेशे से टीचर थे। अभी हैं लेकिन अब न कवि हैं, न मित्र हैं, न टीचर हैं। जो हैं, सो हैं। बड़ी सांसत में हैं।
मित्रता के दिनो में उन्हे जब रत्ननुमा-पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनका पूरा गांव उल्लास में शामिल हो गया था। दूर-दूर से नाते-रिश्ते के लोग जुटे। खूब बधाइयां मिलीं। तब आजकल की तरह गिफ्टबाजी नहीं होती थी। पहुंचना, स्नेहालाप, मित्रालाप ही पर्याप्त रहता था। पेशे के चक्कर में अपना गांव-पुर, कस्बा-शहर छूटा तो उस जन्मोत्सव के दशकों बाद दोबारा उनसे मुलाकात संभव न हो सकी।
वह मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। बड़े पूजा-पाठ, मन्नतों के बाद वह इकलौता पुत्र पैदा हुआ था। पिता की ही तरह हृष्ट-पुष्ट। अपने शिक्षक पिता की साइकिल पर आगे बैठ कर रोजाना मैंने उसे बड़ा होकर स्कूल जाते देखा था। मुद्दत बाद अपने गांव-पुर पहुंचा तो पुराने दोस्तों-मित्रों के संबंध में हाल-चाल लेने लगा। जिनसे अब तक इक्का-दुक्का निभती रही थी, उन्हीं में एक मित्र ने उस सत्तर-अस्सी के दशक वाले साहित्यिक मित्र का दर्दनाक वाकया भी कह सुनाया, आह-उह करते हुए कि अरे उन महोदय की वीर-कविताई की तो ऐसी-तैसी हो चुकी है।
संक्षिप्ततः पूर्व साहित्यिक मित्र का ताजा एक दशक का जिंदगीनामा कुछ इस तरह है। पूर्व कविमित्र का इकलौता बेटा बड़ा होकर मोस्ट वांटेड हो गया। पुलिस की टॉप टेन लिस्ट में पहले नंबर पर। पूरा इलाका कांपने लगा। थानेदार को गोली से उड़ा दिया। ठेके पर मर्डर करने लगा। गिरफ्तार होकर जेल गया तो एक डिप्टी जेलर को ठिकाने लगा दिया। इस तरह वह जिले का सबसे बड़ा गुंडा बन गया। वीररस के कवि का वीर पुत्र।
उस दिन मित्र ने बताया कि अब तो बेचारे कविजी फिरौती के पैसे ठिकाने लगाते हैं। वीरपुत्र नेता बन गया है। जेल से ही नेतागीरी करता है। वीरकवि की बहू विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। एक माफिया उसे टिकट दिलाने वाला है। शायद ही कभी कोई अचंभे में रो पड़ा हो। उस दिन मैं पूर्व कविमित्र की व्यथा-कथा सुन कर अचंभे से रो पड़ा था।
कितनी अच्छी कविताएं लिखते थे वह। एक देशविख्यात महाकवि के सबसे प्रिय शिष्यों में गिने जाते रहे हैं। अब अपने पुत्र की माफिया-राजनीतिक यश-प्रतिष्ठा से काफी आह्लादित रहते हैं। दूर-दूर तक नयी पीढ़ी के लोग जानते हैं कि वो फलाने सिंह के पिता हैं।
जिले के साहित्यकारों को अब कोई आंख नहीं दिखा सकता है। उनके पास सब-कुछ है, बस कविता नहीं है।
मित्रता के दिनो में उन्हे जब रत्ननुमा-पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनका पूरा गांव उल्लास में शामिल हो गया था। दूर-दूर से नाते-रिश्ते के लोग जुटे। खूब बधाइयां मिलीं। तब आजकल की तरह गिफ्टबाजी नहीं होती थी। पहुंचना, स्नेहालाप, मित्रालाप ही पर्याप्त रहता था। पेशे के चक्कर में अपना गांव-पुर, कस्बा-शहर छूटा तो उस जन्मोत्सव के दशकों बाद दोबारा उनसे मुलाकात संभव न हो सकी।
वह मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। बड़े पूजा-पाठ, मन्नतों के बाद वह इकलौता पुत्र पैदा हुआ था। पिता की ही तरह हृष्ट-पुष्ट। अपने शिक्षक पिता की साइकिल पर आगे बैठ कर रोजाना मैंने उसे बड़ा होकर स्कूल जाते देखा था। मुद्दत बाद अपने गांव-पुर पहुंचा तो पुराने दोस्तों-मित्रों के संबंध में हाल-चाल लेने लगा। जिनसे अब तक इक्का-दुक्का निभती रही थी, उन्हीं में एक मित्र ने उस सत्तर-अस्सी के दशक वाले साहित्यिक मित्र का दर्दनाक वाकया भी कह सुनाया, आह-उह करते हुए कि अरे उन महोदय की वीर-कविताई की तो ऐसी-तैसी हो चुकी है।
संक्षिप्ततः पूर्व साहित्यिक मित्र का ताजा एक दशक का जिंदगीनामा कुछ इस तरह है। पूर्व कविमित्र का इकलौता बेटा बड़ा होकर मोस्ट वांटेड हो गया। पुलिस की टॉप टेन लिस्ट में पहले नंबर पर। पूरा इलाका कांपने लगा। थानेदार को गोली से उड़ा दिया। ठेके पर मर्डर करने लगा। गिरफ्तार होकर जेल गया तो एक डिप्टी जेलर को ठिकाने लगा दिया। इस तरह वह जिले का सबसे बड़ा गुंडा बन गया। वीररस के कवि का वीर पुत्र।
उस दिन मित्र ने बताया कि अब तो बेचारे कविजी फिरौती के पैसे ठिकाने लगाते हैं। वीरपुत्र नेता बन गया है। जेल से ही नेतागीरी करता है। वीरकवि की बहू विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। एक माफिया उसे टिकट दिलाने वाला है। शायद ही कभी कोई अचंभे में रो पड़ा हो। उस दिन मैं पूर्व कविमित्र की व्यथा-कथा सुन कर अचंभे से रो पड़ा था।
कितनी अच्छी कविताएं लिखते थे वह। एक देशविख्यात महाकवि के सबसे प्रिय शिष्यों में गिने जाते रहे हैं। अब अपने पुत्र की माफिया-राजनीतिक यश-प्रतिष्ठा से काफी आह्लादित रहते हैं। दूर-दूर तक नयी पीढ़ी के लोग जानते हैं कि वो फलाने सिंह के पिता हैं।
जिले के साहित्यकारों को अब कोई आंख नहीं दिखा सकता है। उनके पास सब-कुछ है, बस कविता नहीं है।
Subscribe to:
Posts (Atom)